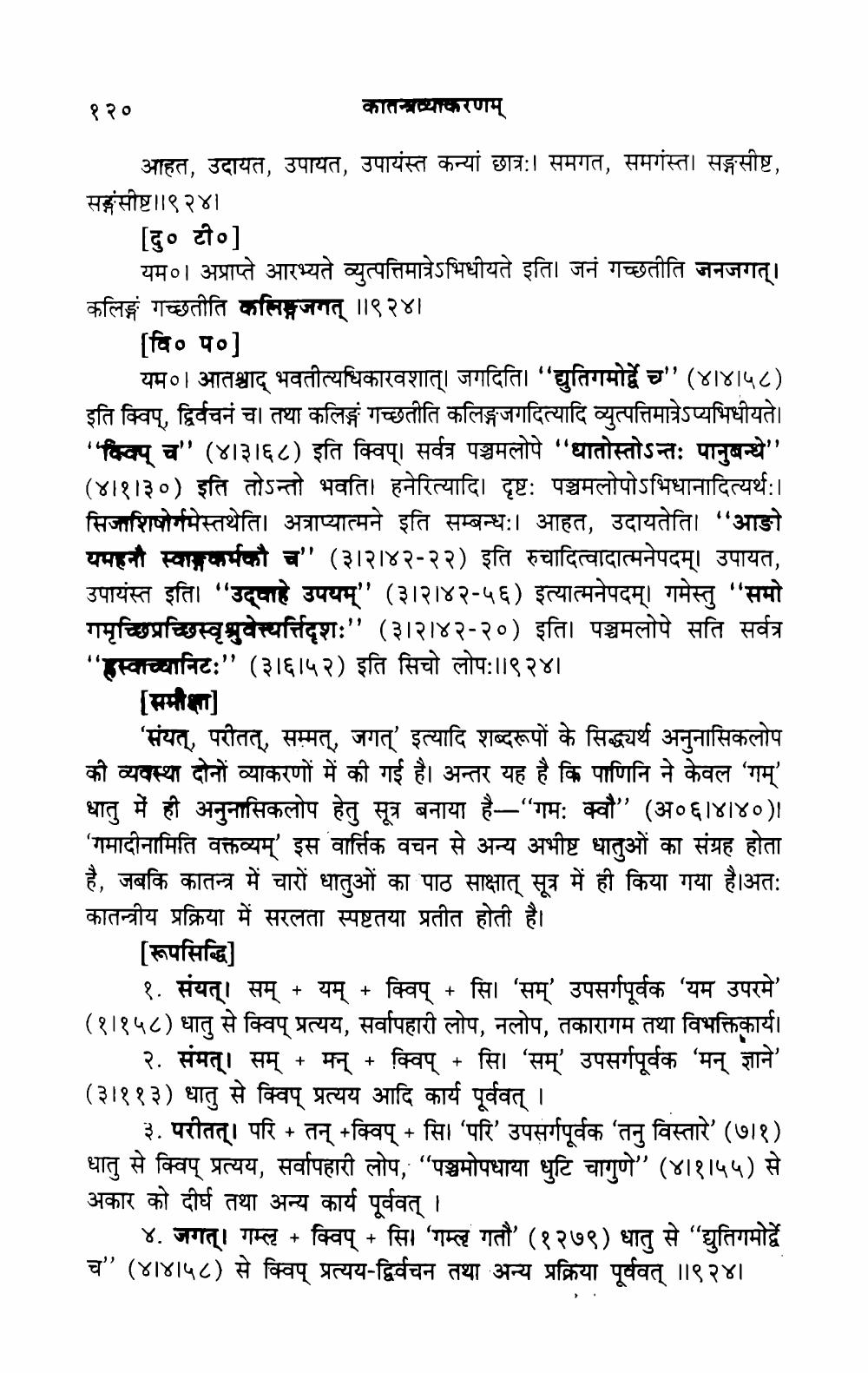________________
१२०
कातन्त्रव्याकरणम्
आहत, उदायत, उपायत, उपायंस्त कन्यां छात्रः। समगत, समगंस्त। सगसीष्ट, सङ्गंसीष्ट।।९२४।
[दु० टी०]
यम०। अप्राप्ते आरभ्यते व्युत्पत्तिमात्रेऽभिधीयते इति। जनं गच्छतीति जनजगत्। कलिङ्गं गच्छतीति कलिङ्गजगत् ।।९२४।
[वि० प०]
यम०। आतश्चाद् भवतीत्यधिकारवशात्। जगदिति। "द्युतिगमोढे च'' (४।४।५८) इति क्विए, द्विर्वचनं च। तथा कलिङ्गं गच्छतीति कलिङ्गजगदित्यादि व्युत्पत्तिमात्रेऽप्यभिधीयते। "विवप् च" (४।३।६८) इति क्विए। सर्वत्र पञ्चमलोपे "धातोस्तोऽन्तः पानुबन्थे" (४।१।३०) इति तोऽन्तो भवति। हनेरित्यादि। दृष्टः पञ्चमलोपोऽभिधानादित्यर्थः। सिजाशिषोर्गमेस्तथेति। अत्राप्यात्मने इति सम्बन्धः। आहत, उदायतेति। "आङो यमहनी स्वाङ्गकर्मको च" (३।२।४२-२२) इति रुचादित्वादात्मनेपदम्। उपायत, उपायंस्त इति। "उदाहे उपयम्" (३।२।४२-५६) इत्यात्मनेपदम्। गमेस्तु "समो गमृच्छिप्रच्छिस्ववेत्थर्त्तिदृशः" (३।२।४२-२०) इति। पञ्चमलोपे सति सर्वत्र "हस्काच्यानिटः" (३।६।५२) इति सिचो लोपः।।९२४।
[समीक्षा _ 'संयत्, परीतत्, सम्मत्, जगत्' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ अनुनासिकलोप की व्यवस्था दोनों व्याकरणों में की गई है। अन्तर यह है कि पाणिनि ने केवल ‘गम्' धातु में ही अनुनासिकलोप हेतु सूत्र बनाया है- “गम: क्वौ” (अ०६।४।४०)। 'गमादीनामिति वक्तव्यम्' इस वार्तिक वचन से अन्य अभीष्ट धातुओं का संग्रह होता है, जबकि कातन्त्र में चारों धातुओं का पाठ साक्षात् सूत्र में ही किया गया है।अत: कातन्त्रीय प्रक्रिया में सरलता स्पष्टतया प्रतीत होती है।
[रूपसिद्धि]
१. संयत्। सम् + यम् + क्विप् + सि। 'सम्' उपसर्गपूर्वक ‘यम उपरमे' (१।१५८) धातु से क्विप् प्रत्यय, सर्वापहारी लोप, नलोप, तकारागम तथा विभक्तिकार्य।
२. संमत्। सम् + मन् + क्विप् + सि। 'सम्' उपसर्गपूर्वक 'मन् ज्ञाने' (३।११३) धातु से क्विप् प्रत्यय आदि कार्य पूर्ववत् ।
३. परीतत्। परि + तन् +क्विप् + सि। 'परि' उपसर्गपूर्वक 'तनु विस्तारे' (७।१) धातु से क्विप् प्रत्यय, सर्वापहारी लोप, “पञ्चमोपधाया धुटि चागुणे' (४।१।५५) से अकार को दीर्घ तथा अन्य कार्य पूर्ववत् ।
४. जगत्। गम्ल + क्विप् + सि। “गम्लु गतौ' (१२७९) धातु से “द्युतिगमोढे च' (४।४।५८) से क्विप् प्रत्यय-द्विवचन तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ।।९२४।