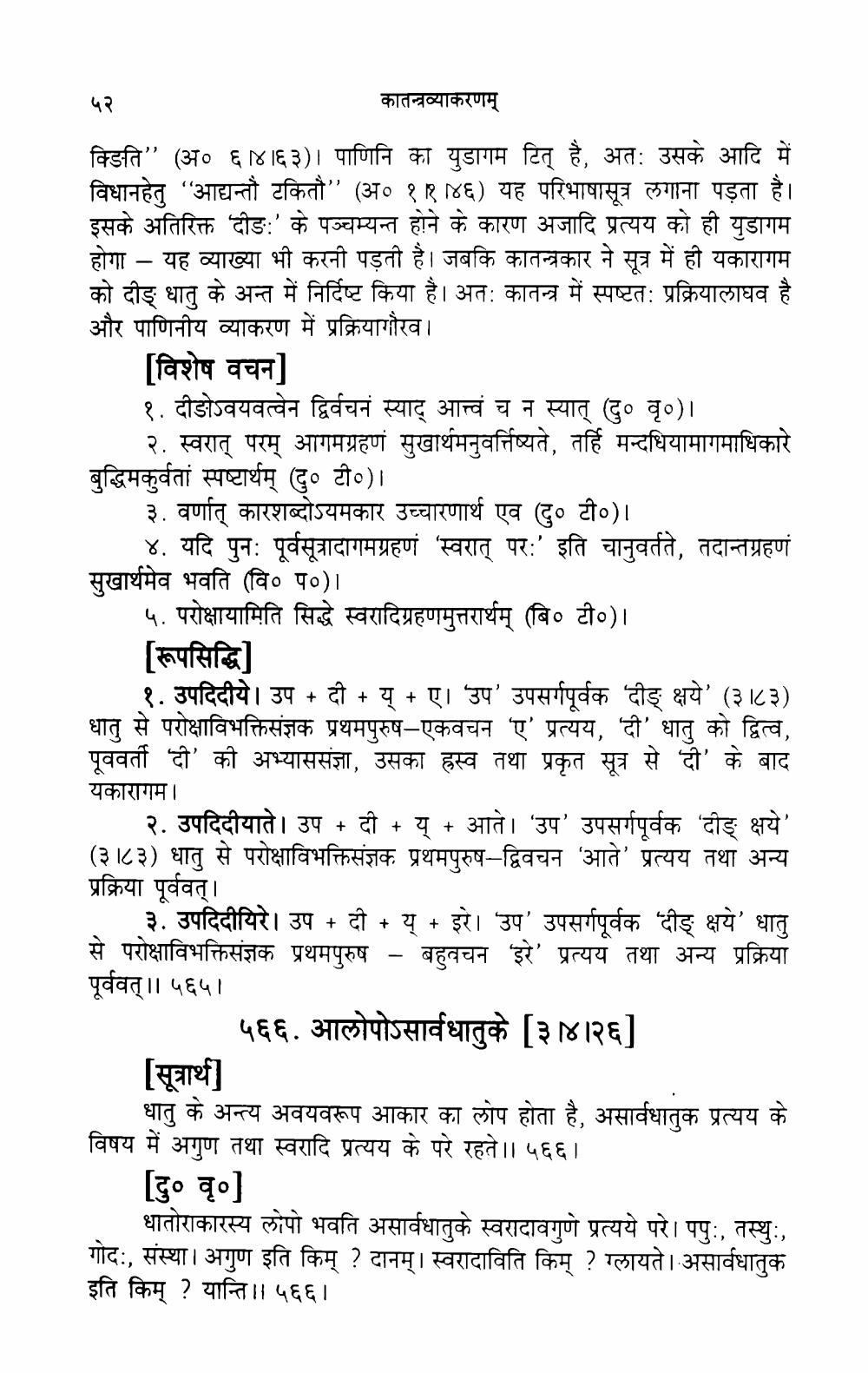________________
कातन्त्रव्याकरणम्
क्ङिति' (अ० ६।४।६३)। पाणिनि का युडागम टित् है, अत: उसके आदि में विधानहेतु “आद्यन्तौ टकितौ'' (अ० ११४६) यह परिभाषासूत्र लगाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दीङः' के पञ्चम्यन्त होने के कारण अजादि प्रत्यय को ही युडागम होगा – यह व्याख्या भी करनी पड़ती है। जबकि कातन्त्रकार ने सूत्र में ही यकारागम को दीङ् धातु के अन्त में निर्दिष्ट किया है। अत: कातन्त्र में स्पष्टत: प्रक्रियालाघव है और पाणिनीय व्याकरण में प्रक्रियागौरव।
[विशेष वचन] १. दीङोऽवयवत्वेन द्विर्वचनं स्याद् आत्त्वं च न स्यात् (दु० वृ०)।
२. स्वरात् परम् आगमग्रहणं सुखार्थमनुवर्तिष्यते, तर्हि मन्दधियामागमाधिकारे बुद्धिमकुर्वतां स्पष्टार्थम् (दु० टी०)।
३. वर्णात् कारशब्दोऽयमकार उच्चारणार्थ एव (दु० टी०)।
४. यदि पुन: पूर्वसूत्रादागमग्रहणं 'स्वरात् परः' इति चानुवर्तते, तदान्तग्रहणं सुखार्थमेव भवति (वि० प०)। ___५. परोक्षायामिति सिद्धे स्वरादिग्रहणमुत्तरार्थम् (बि० टी०)।
[रूपसिद्धि
१. उपदिदीये। उप + दी + य + ए। 'उप' उपसर्गपूर्वक 'दीङ क्षये' (३८३) धातु से परोक्षाविभक्तिसंज्ञक प्रथमपुरुष-एकवचन 'ए' प्रत्यय, 'दी' धातु को द्वित्व, पूववर्ती 'दी' की अभ्याससंज्ञा, उसका ह्रस्व तथा प्रकृत सूत्र से 'दी' के बाद यकारागम।
२. उपदिदीयाते। उप + दी + य् + आते। 'उप' उपसर्गपर्वक 'दीङ क्षये' (३८३) धातु से परोक्षाविभक्तिसंज्ञक प्रथमपुरुष-द्विवचन 'आते' प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत्।
३. उपदिदीयिरे। उप + दी + य् + इरे। 'उप' उपसर्गपूर्वक 'दीङ् क्षये' धातु से परोक्षाविभक्तिसंज्ञक प्रथमपुरुष - बहवचन 'इरे' प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ।। ५६५।
५६६. आलोपोऽसार्वधातुके [३।४।२६] [सूत्रार्थ]
धातु के अन्त्य अवयवरूप आकार का लोप होता है, असार्वधातुक प्रत्यय के विषय में अगुण तथा स्वरादि प्रत्यय के परे रहते।। ५६६।
[दु० वृ०]
धातोराकारस्य लोपो भवति असार्वधातुके स्वरादावगुणे प्रत्यये परे। पपुः, तस्थुः, गोदः, संस्था। अगुण इति किम् ? दानम्। स्वरादाविति किम् ? ग्लायते। असार्वधातुक इति किम् ? यान्ति।। ५६६।