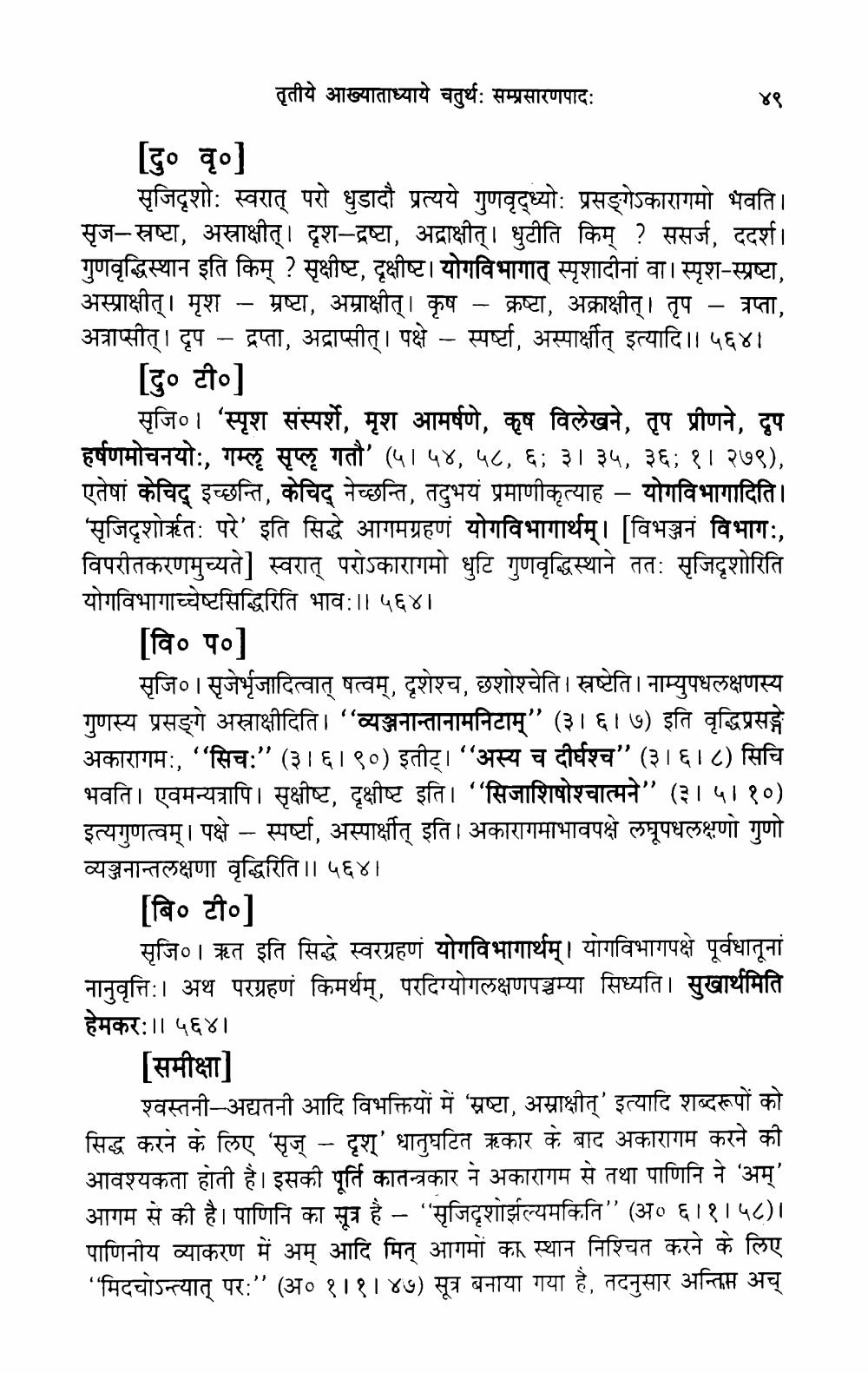________________
४९
तृतीये आख्याताध्याये चतुर्थः सम्प्रसारणपादः [दु० वृ०]
सृजिदृशोः स्वरात् परो धुडादौ प्रत्यये गुणवृद्ध्योः प्रसङ्गेऽकारागमो भवति। सृज-स्रष्टा, अस्राक्षीत्। दृश-द्रष्टा, अद्राक्षीत्। धुटीति किम् ? ससर्ज, ददर्श। गुणवृद्धिस्थान इति किम् ? सूक्षीष्ट, दृक्षीष्ट। योगविभागात स्पृशादीनां वा। स्पृश-स्प्रष्टा, अस्पाक्षीत्। मृश - म्रष्टा, अम्राक्षीत्। कृष – क्रष्टा, अक्राक्षीत्। तृप – त्रप्ता, अत्राप्सीत् । दृप - द्रप्ता, अद्राप्सीत्। पक्षे - स्पा, अस्पार्षीत् इत्यादि।। ५६४।
[दु० टी०]
सृजि० । 'स्पृश संस्पर्श, मृश आमर्षणे, कृष विलेखने, तृप प्रीणने, दुप हर्षणमोचनयोः, गम्ल सृल गतौ' (५। ५४, ५८, ६; ३। ३५, ३६; १। २७९), एतेषां केचिद् इच्छन्ति, केचिद् नेच्छन्ति, तदुभयं प्रमाणीकृत्याह – योगविभागादिति। ‘सृजिदृशोर्ऋतः परे' इति सिद्धे आगमग्रहणं योगविभागार्थम्। [विभञ्जनं विभागः, विपरीतकरणमुच्यते] स्वरात् परोऽकारागमो धुटि गुणवृद्धिस्थाने ततः सृजिदृशोरिति योगविभागाच्चेष्टसिद्धिरिति भावः।। ५६४।
[वि० प०]
सृजि० । सृजे जादित्वात् षत्वम्, दृशेश्च, छशोश्चेति। स्रष्टेति। नाम्युपधलक्षणस्य गुणस्य प्रसङ्गे अस्राक्षीदिति। "व्यञ्जनान्तानामनिटाम्" (३। ६। ७) इति वृद्धिप्रसङ्गे अकारागमः, “सिच:" (३।६। ९०) इतीट। “अस्य च दीर्घश्च" (३। ६। ८) सिचि भवति। एवमन्यत्रापि। सूक्षीष्ट, दृक्षीष्ट इति। “सिजाशिषोश्चात्मने" (३। ५। १०) इत्यगुणत्वम्। पक्षे - स्पा, अस्पार्षीत् इति। अकारागमाभावपक्षे लघूपधलक्षणो गुणो व्यञ्जनान्तलक्षणा वृद्धिरिति।। ५६४।
[बि० टी०]
सृजि० । ऋत इति सिद्धे स्वरग्रहणं योगविभागार्थम्। योगविभागपक्षे पूर्वधातूनां नानुवृत्तिः। अथ परग्रहणं किमर्थम्, परदिग्योगलक्षणपञ्चम्या सिध्यति। सुखार्थमिति हेमकरः।। ५६४।
[समीक्षा
श्वस्तनी-अद्यतनी आदि विभक्तियों में 'स्रष्टा, अनाक्षीत्' इत्यादि शब्दरूपों को सिद्ध करने के लिए 'सृज् - दृश्' धातुघटित ऋकार के बाद अकारागम करने की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति कातन्त्रकार ने अकारागम से तथा पाणिनि ने 'अम्' आगम से की है। पाणिनि का सूत्र है - "सृजिदृशोझल्यमकिति'' (अ०६।१। ५८)। पाणिनीय व्याकरण में अम् आदि मित् आगमों का स्थान निश्चित करने के लिए "मिदचोऽन्त्यात् परः'' (अ० १ । १। ४७) सूत्र बनाया गया है, तदनुसार अन्तिम अच्