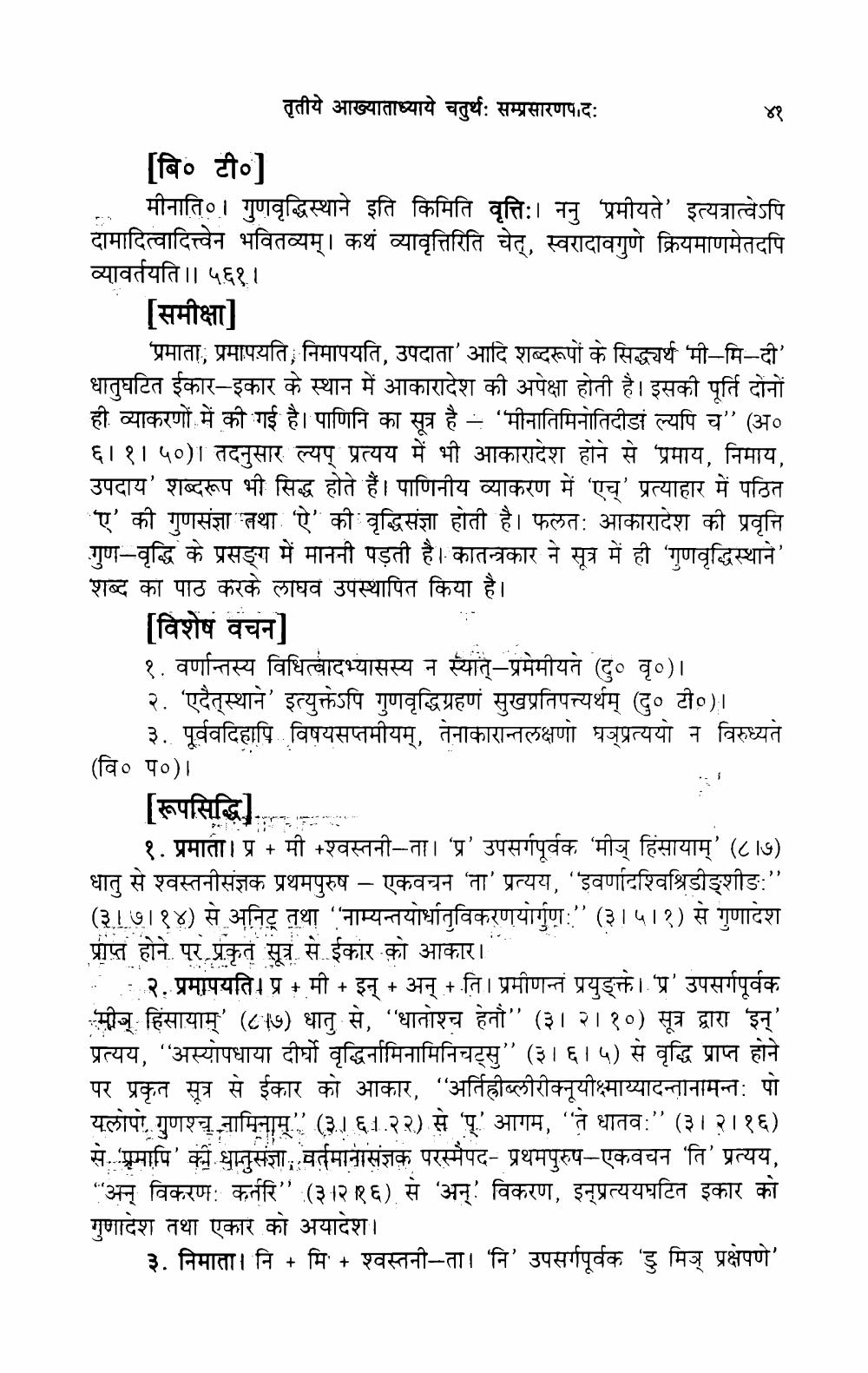________________
तृतीये आख्याताध्याये चतुर्थः सम्प्रसारणपाद:
[बि० टी०]
मीनाति० । गुणवृद्धिस्थाने इति किमिति वृत्तिः। ननु ‘प्रमीयते' इत्यत्रात्वेऽपि दामादित्वादित्त्वेन भवितव्यम्। कथं व्यावृत्तिरिति चेत्, स्वरादावगुणे क्रियमाणमेतदपि व्यावर्तयति।। ५६१।
[समीक्षा]
'प्रमाता; प्रमापयति, निमापयति, उपदाता' आदि शब्दरूपों के सिद्धयर्थ 'मी-मि-दी' धातुघटित ईकार-इकार के स्थान में आकारादेश की अपेक्षा होती है। इसकी पूर्ति दोनों ही व्याकरणों में की गई है। पाणिनि का सूत्र है - “मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च' (अ० ६।१। ५०)। तदनुसार ल्यप् प्रत्यय में भी आकारादेश होने से 'प्रमाय, निमाय, उपदाय' शब्दरूप भी सिद्ध होते हैं। पाणिनीय व्याकरण में 'एच' प्रत्याहार में पठित “ए' की गुणसंज्ञा लथा. 'ऐ' की वृद्धिसंज्ञा होती है। फलत: आकारादेश की प्रवृत्ति गुण-वृद्धि के प्रसङ्ग में माननी पड़ती है। कातन्त्रकार ने सूत्र में ही ‘गुणवृद्धिस्थाने' शब्द का पाठ करके लाघव उपस्थापित किया है।
[विशेष वचन १. वर्णान्तस्य विधित्वादभ्यासस्य न स्यात्-प्रमेमीयते (दु० वृ०)। २. “एदैत्स्थाने' इत्युक्तेऽपि गुणवृद्धिग्रहणं सुखप्रतिपत्त्यर्थम् (दु० टी०)।
३. पूर्ववदिहापि विषयसप्तमीयम्, तेनाकारान्तलक्षणो घञ्प्रत्ययो न विरुध्यते (वि० प०)।
[रूपसिद्धि
१. प्रमाता। प्र + मी +श्वस्तनी-ता। 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'मीञ् हिंसायाम्' (८७) धातु से श्वस्तनीसंज्ञक प्रथमपुरुष – एकवचन 'ता' प्रत्यय, "इवर्णादश्विश्रिडीशीङः'' (३। ७ । १४) से अनिट् तथा “नाम्यन्तयोर्धातुविकरणयोर्गुणः” (३ । ५ । १) से गुणादेश प्राप्त होने पर प्रकृतं सूत्र से ईकार को आकार। ... २. प्रमापयति। प्र + मी + इन् + अन् + ति। प्रमीणन्तं प्रयुङ्क्ते। 'प्र' उपसर्गपूर्वक
मी हिंसायाम्' (८१७) धातु से, "धातोश्च हतो'' (३। २।१०) सूत्र द्वारा 'इन्' प्रत्यय, “अस्योपधाया दीर्घो वृद्धि मिनामिनिचट्सु'' (३। ६। ५) से वृद्धि प्राप्त होने पर प्रकृत सूत्र से ईकार को आकार, “अर्तिह्रीब्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यादन्तानामन्तः पो यलोपो. गुणश्च नामिनाम्' (३।६।.२२) से 'प्.' आगम, "ते धातवः' (३। २ । १६) स. प्रमापि' की धातुसंज्ञा. वर्तमानासंज्ञक परस्मैपद- प्रथमपुरुप-एकवचन 'ति' प्रत्यय, "अन् विकरण: कतरि" (३।२१६) से 'अन्' विकरण, इन्प्रत्ययघटित इकार को गुणादेश तथा एकार को अयादेश।
३. निमाता। नि + मि. + श्वस्तनी-ता। 'नि' उपसर्गपूर्वक 'डु मिञ् प्रक्षेपणे'