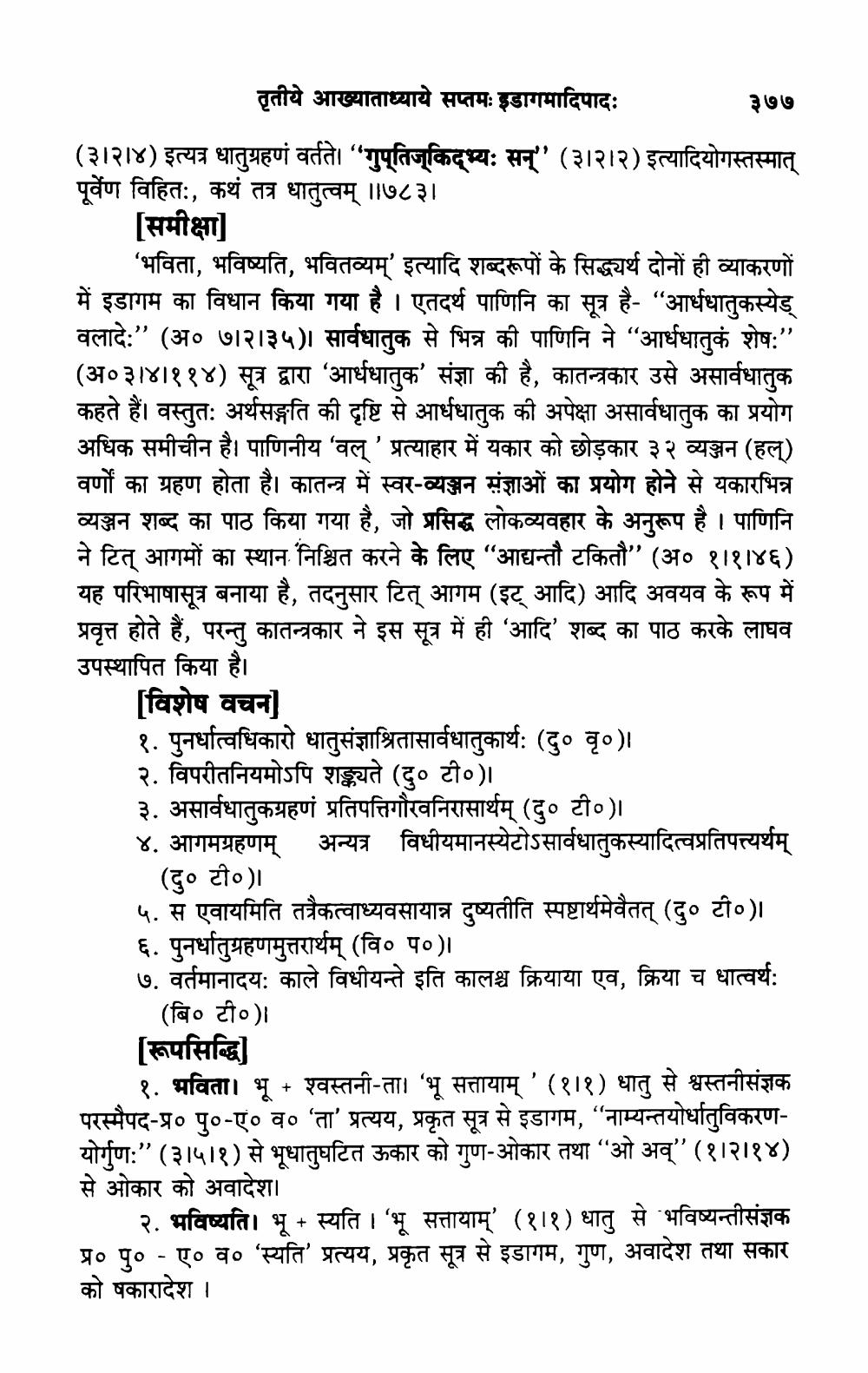________________
तृतीये आख्याताध्याये सप्तमः इडागमादिपादः
,
(३।२।४) इत्यत्र धातुग्रहणं वर्तते । “गुप्तिज्किद्भ्यः सन् " ( ३।२।२) इत्यादियोगस्तस्मात् पूर्वेण विहितः, कथं तत्र धातुत्वम् ॥७८३।
[समीक्षा]
३७७
'भविता, भविष्यति, भवितव्यम्' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ दोनों ही व्याकरणों में इडागम का विधान किया गया है । एतदर्थ पाणिनि का सूत्र है- " आर्धधातुकस्येड् वलादेः” (अ० ७।२।३५ ) | सार्वधातुक से भिन्न की पाणिनि ने “आर्धधातुकं शेषः " (अ०३।४।११४) सूत्र द्वारा 'आर्धधातुक' संज्ञा की है, कातन्त्रकार उसे असार्वधातुक कहते हैं। वस्तुतः अर्थसङ्गति की दृष्टि से आर्धधातुक की अपेक्षा असार्वधातुक का प्रयोग अधिक समीचीन है। पाणिनीय 'वल्' प्रत्याहार में यकार को छोड़कार ३२ व्यञ्जन (हल् ) वर्णों का ग्रहण होता है । कातन्त्र में स्वर - व्यञ्जन संज्ञाओं का प्रयोग होने से यकारभिन्न व्यञ्जन शब्द का पाठ किया गया है, जो प्रसिद्ध लोकव्यवहार के अनुरूप है । पाणिनि ने टित् आगमों का स्थान निश्चित करने के लिए “आद्यन्तौ टकितौ” (अ० १|१|४६ ) यह परिभाषासूत्र बनाया है, तदनुसार टित् आगम (इट् आदि) आदि अवयव के रूप में प्रवृत्त होते हैं, परन्तु कातन्त्रकार ने इस सूत्र में ही 'आदि' शब्द का पाठ करके लाघव उपस्थापित किया है।
[विशेष वचन ]
१. पुनर्धात्वधिकारो धातुसंज्ञाश्रितासार्वधातुकार्थः (दु० वृ०)। २. विपरीतनियमोऽपि शङ्क्यते (दु० टी० ) ।
३. असार्वधातुकग्रहणं प्रतिपत्तिगौरवनिरासार्थम् (दु० टी०)। ४. आगमग्रहणम् (दु० टी० ) ।
५. स एवायमिति तत्रैकत्वाध्यवसायान्न दुष्यतीति स्पष्टार्थमेवैतत् (दु० टी० ) । ६. पुनर्धातुग्रहणमुत्तरार्थम् (वि० प० ) ।
७.
वर्तमानादयः काले विधीयन्ते इति कालश्च क्रियाया एव, क्रिया च धात्वर्थ: (बि० टी० ) ।
[रूपसिद्धि]
१. भविता । भू + श्वस्तनी - ता । 'भू सत्तायाम् ' (१।१) धातु से श्वस्तनीसंज्ञक परस्मैपद-प्र० पु०-एं० व० 'ता' प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से इडागम, “नाम्यन्तयोर्धातुविकरणयोर्गुण: " ( ३।५।१) से भूधातुघटित ऊकार को गुण ओकार तथा “ओ अव्” (१।२।१४) से ओकार को अवादेश ।
अन्यत्र विधीयमानस्येटोऽसार्वधातुकस्यादित्वप्रतिपत्त्यर्थम्
२. भविष्यति । भू + स्यति । 'भू सत्तायाम् ' (१/१) धातु से भविष्यन्तीसंज्ञक प्र० पु० ए० व० 'स्यति' प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से इडागम, गुण, अवादेश तथा सकार को कारादेश ।