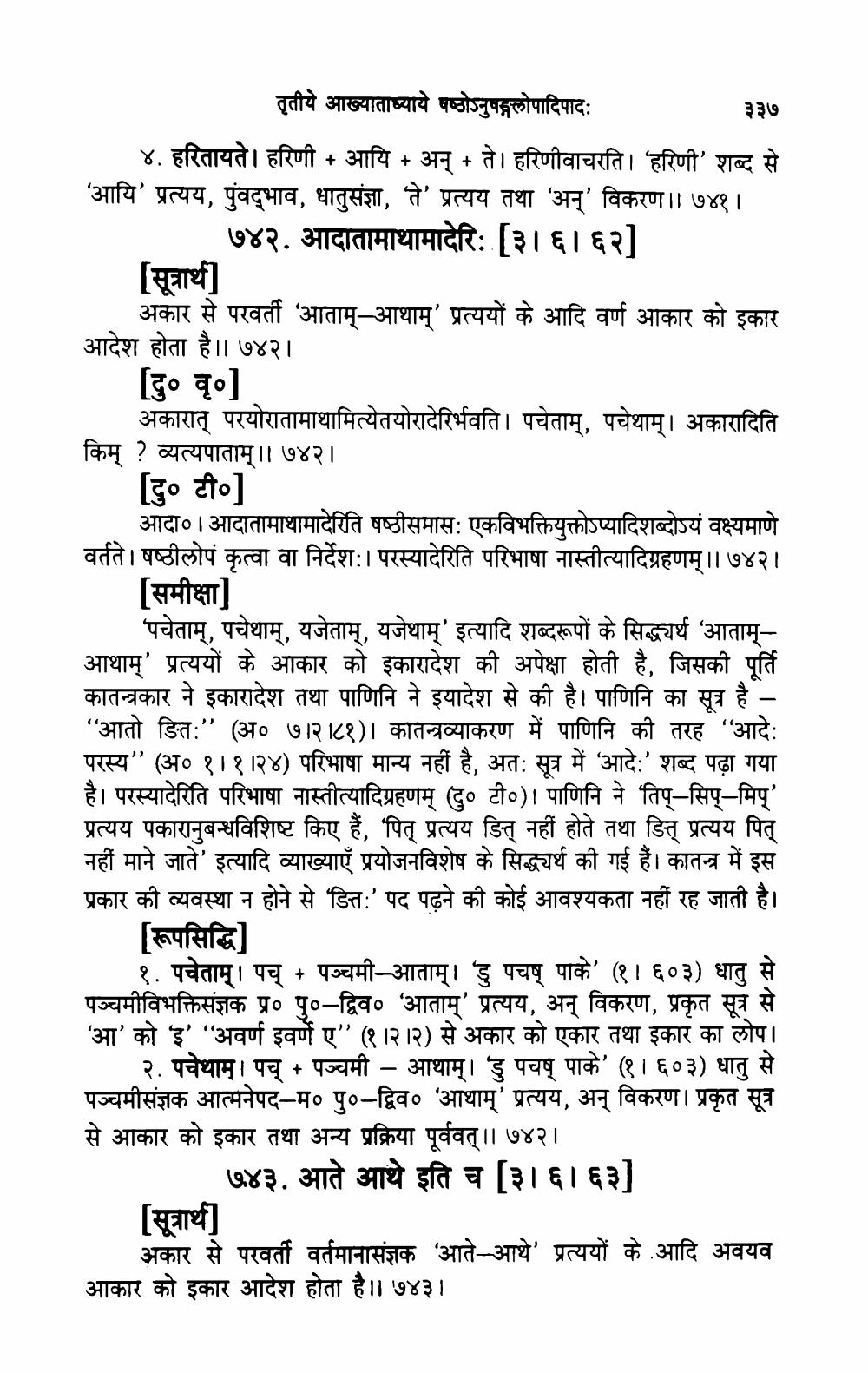________________
तृतीये आख्याताध्याये षष्ठोऽनुषङ्गलोपादिपादः
३३७ ४. हरितायते। हरिणी + आयि + अन् + ते। हरिणीवाचरति। ‘हरिणी' शब्द से 'आयि' प्रत्यय, पुंवद्भाव, धातुसंज्ञा, 'ते' प्रत्यय तथा 'अन्' विकरण।। ७४१ ।
७४२. आदातामाथामादेरिः [३। ६। ६२] [सूत्रार्थ]
अकार से परवर्ती 'आताम्-आथाम्' प्रत्ययों के आदि वर्ण आकार को इकार आदेश होता है।। ७४२।
[दु० वृ०]
अकारात् परयोरातामाथामित्येतयोरादेरिर्भवति। पचेताम्, पचेथाम्। अकारादिति किम् ? व्यत्यपाताम्।। ७४२।
[दु० टी०]
आदा० । आदातामाथामादेरिति षष्ठीसमास: एकविभक्तियुक्तोऽप्यादिशब्दोऽयं वक्ष्यमाणे वर्तते। षष्ठीलोपं कृत्वा वा निर्देश:। परस्यादेरिति परिभाषा नास्तीत्यादिग्रहणम्।। ७४२ ।
[समीक्षा]
‘पचेताम, पचेथाम, यजेताम, यजेथाम्' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ 'आतामआथाम्' प्रत्ययों के आकार को इकारादेश की अपेक्षा होती है, जिसकी पूर्ति कातन्त्रकार ने इकारादेश तथा पाणिनि ने इयादेश से की है। पाणिनि का सूत्र है - "आतो डित:" (अ० ७।२८१)। कातन्त्रव्याकरण में पाणिनि की तरह “आदे: परस्य" (अ० १।१।२४) परिभाषा मान्य नहीं है, अत: सूत्र में 'आदे:' शब्द पढ़ा गया है। परस्यादेरिति परिभाषा नास्तीत्यादिग्रहणम् (टु० टी०)। पाणिनि ने 'तिप्-सिप्-मिप्' प्रत्यय पकारानुबन्धविशिष्ट किए हैं, 'पित् प्रत्यय डित् नहीं होते तथा डित् प्रत्यय पित् नहीं माने जाते' इत्यादि व्याख्याएँ प्रयोजनविशेष के सिद्धयर्थ की गई हैं। कातन्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था न होने से 'डित:' पद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।
[रूपसिद्धि]
१. पचेताम्। पच् + पञ्चमी-आताम्। 'डु पचष् पाके' (१। ६०३) धातु से पञ्चमीविभक्तिसंज्ञक प्र० पु०-द्विव० 'आताम्' प्रत्यय, अन् विकरण, प्रकृत सूत्र से 'आ' को 'इ' “अवर्ण इवणे ए" (१।२।२) से अकार को एकार तथा इकार का लोप।
२. पचेथाम्। पच् + पञ्चमी – आथाम्। 'डु पचष् पाके' (१ । ६०३) धातु से पञ्चमीसंज्ञक आत्मनेपद-म० पु०-द्विव० 'आथाम्' प्रत्यय, अन् विकरण। प्रकृत सूत्र से आकार को इकार तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ।। ७४२।
७४३. आते आथे इति च [३।६।६३] [सूत्रार्थ
अकार से परवर्ती वर्तमानासंज्ञक 'आते-आथे' प्रत्ययों के आदि अवयव आकार को इकार आदेश होता है।। ७४३।