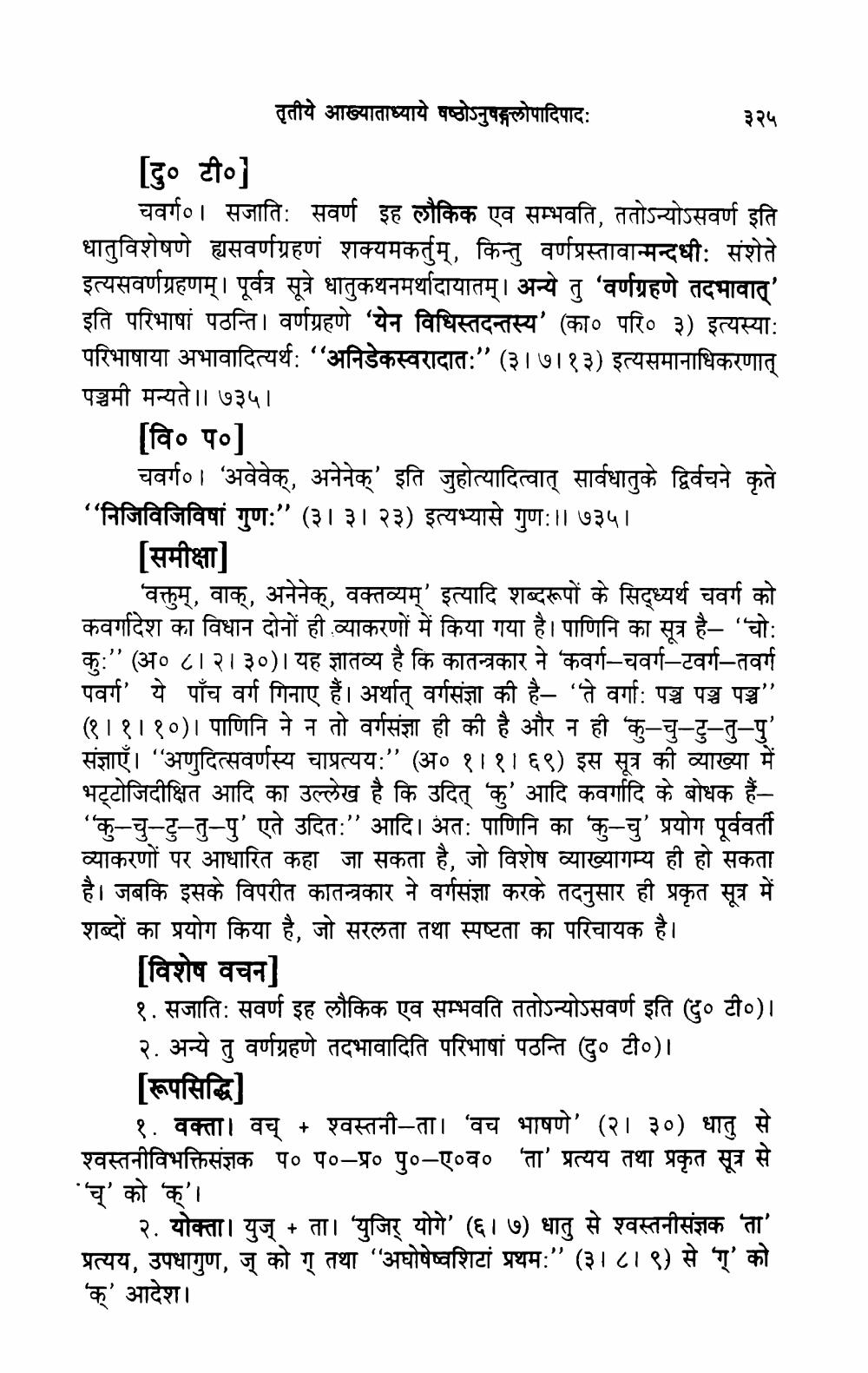________________
३२५
तृतीये आख्याताध्याये षष्ठोऽनुषङ्गलोपादिपाद: [दु० टी०]
चवर्ग०। सजाति: सवर्ण इह लौकिक एव सम्भवति, ततोऽन्योऽसवर्ण इति धातुविशेषणे ह्यसवर्णग्रहणं शक्यमकर्तुम्, किन्तु वर्णप्रस्तावान्मन्दधीः संशेते इत्यसवर्णग्रहणम्। पूर्वत्र सूत्रे धातुकथनमादायातम्। अन्ये तु 'वर्णग्रहणे तदभावात्' इति परिभाषां पठन्ति। वर्णग्रहणे 'येन विधिस्तदन्तस्य' (का० परि० ३) इत्यस्याः परिभाषाया अभावादित्यर्थ: “अनिडेकस्वरादात:" (३ । ७। १३) इत्यसमानाधिकरणात् पञ्चमी मन्यते।। ७३५।
[वि० प०]
चवर्ग०। 'अवेवेक्, अनेनेक्' इति जुहोत्यादित्वात् सार्वधातुके द्विवचने कृते "निजिविजिविषां गुणः" (३ । ३। २३) इत्यभ्यासे गुणः।। ७३५ ।
[समीक्षा]
'वक्तम्, वाक्, अनेनेक, वक्तव्यम्' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ चवर्ग को कवर्गादेश का विधान दोनों ही व्याकरणों में किया गया है। पाणिनि का सूत्र है- “चो: कुः" (अ० ८।२।३०)। यह ज्ञातव्य है कि कातन्त्रकार ने ‘कवर्ग-चवर्ग-टवर्ग-तवर्ग पवर्ग' ये पाँच वर्ग गिनाए हैं। अर्थात् वर्गसंज्ञा की है- “ते वर्गाः पञ्च पञ्च पञ्च" (१ । १। १०)। पाणिनि ने न तो वर्गसंज्ञा ही की है और न ही 'कु-चु-टु-तु-पु' संज्ञाएँ। “अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः” (अ० १।१।६९) इस सूत्र की व्याख्या में भट्टोजिदीक्षित आदि का उल्लेख है कि उदित् 'कु' आदि कवर्गादि के बोधक हैं"कु-चु-टु-तु-पु' एते उदित:" आदि। अत: पाणिनि का 'कु-चु' प्रयोग पूर्ववर्ती व्याकरणों पर आधारित कहा जा सकता है, जो विशेष व्याख्यागम्य ही हो सकता है। जबकि इसके विपरीत कातन्त्रकार ने वर्गसंज्ञा करके तदनुसार ही प्रकृत सूत्र में शब्दों का प्रयोग किया है, जो सरलता तथा स्पष्टता का परिचायक है।
[विशेष वचन] १. सजाति: सवर्ण इह लौकिक एव सम्भवति ततोऽन्योऽसवर्ण इति (९० टी०)। २. अन्ये तु वर्णग्रहणे तदभावादिति परिभाषां पठन्ति (दु० टी०)। [रूपसिद्धि
१. वक्ता। वच् + श्वस्तनी-ता। 'वच भाषणे' (२। ३०) धातु से श्वस्तनीविभक्तिसंज्ञक प० प०-प्र० पु०-ए०व० 'ता' प्रत्यय तथा प्रकृत सूत्र से 'च' को 'क्'।
२. योक्ता। युज् + ता। 'युजिर् योगे' (६। ७) धातु से श्वस्तनीसंज्ञक 'ता' प्रत्यय, उपधागुण, ज् को ग् तथा "अघोषेष्वशिटां प्रथमः' (३। ८। ९) से 'ग्' को 'क्' आदेश।