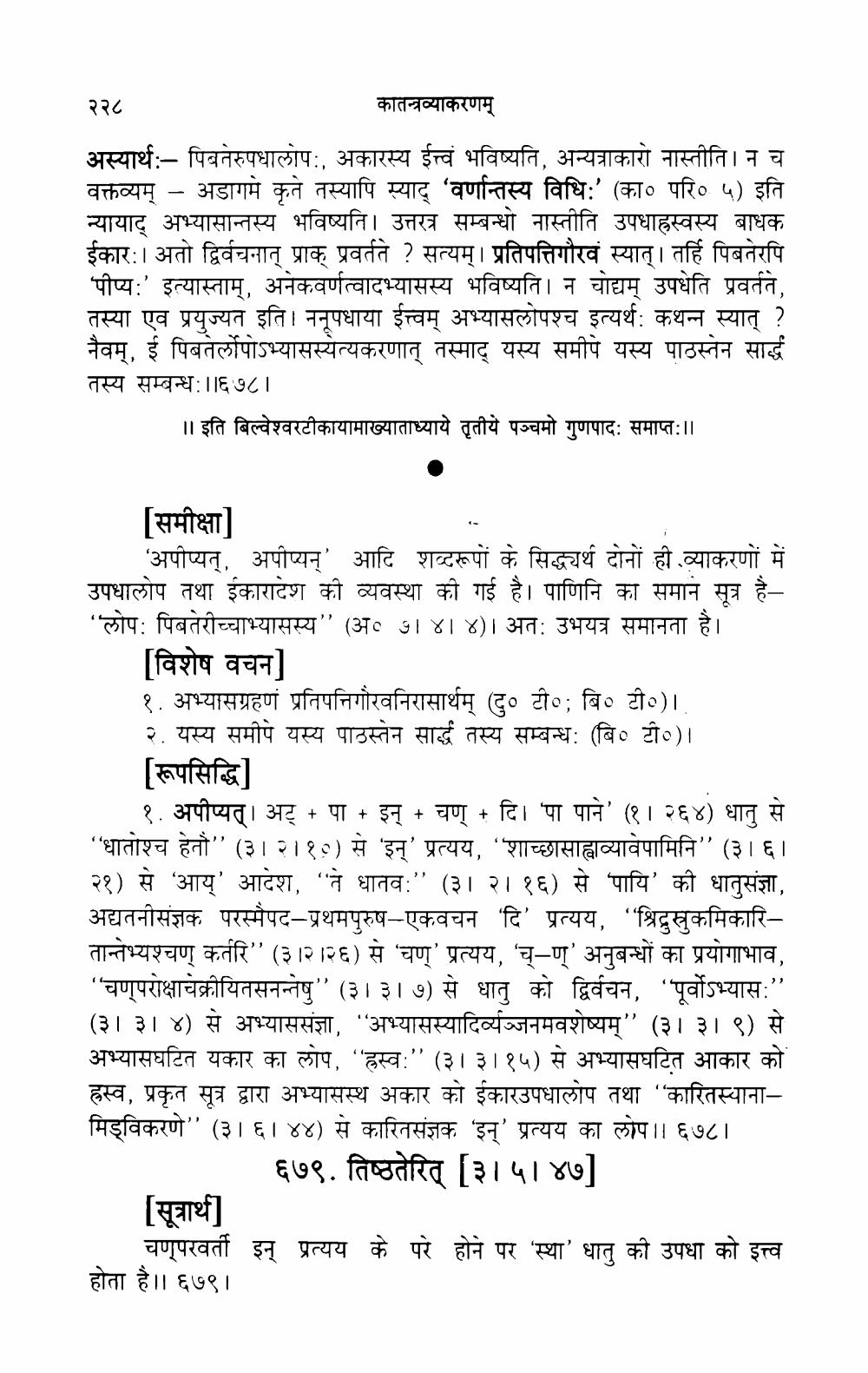________________
२२८
कातन्त्रव्याकरणम् अस्यार्थ:- पिबतेरुपधालोपः, अकारस्य ईत्त्वं भविष्यति, अन्यत्राकारो नास्तीति। न च वक्तव्यम् - अडागमे कृते तस्यापि स्याद् ‘वर्णान्तस्य विधि:' (का० परि० ५) इति न्यायाद् अभ्यासान्तस्य भविष्यति। उत्तरत्र सम्बन्धो नास्तीति उपधाह्रस्वस्य बाधक ईकारः। अतो द्विवचनात् प्राक प्रवर्तते ? सत्यम्। प्रतिपत्तिगौरवं स्यात् । तर्हि पिबतेरपि 'पीप्य:' इत्यास्ताम्, अनेकवर्णत्वादभ्यासस्य भविष्यति। न चोद्यम् उपधेति प्रवर्तते, तस्या एव प्रयुज्यत इति। ननूपधाया ईत्त्वम् अभ्यासलोपश्च इत्यर्थ: कथन्न स्यात् ? नैवम् , ई पिबतेर्लोपोऽभ्यासस्येत्यकरणात् तस्माद् यस्य समीपे यस्य पाठस्तेन सार्द्ध तस्य सम्बन्ध: ।।६७८।
॥ इति बिल्वेश्वरटीकायामाख्याताध्याये तृतीये पञ्चमो गुणपादः समाप्तः।।
[समीक्षा]
'अपीप्यत्, अपीप्यन्' आदि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ दोनों ही व्याकरणों में उपधालोप तथा इंकारादेश की व्यवस्था की गई है। पाणिनि का समान सूत्र है"लोप: पिबतेरीच्चाभ्यासस्य'' (अ० ७।४। ४)। अत: उभयत्र समानता है।
[विशेष वचन] १. अभ्यासग्रहणं प्रतिपत्तिगौरवनिरासार्थम् (टु० टी०; बि० टी०)। २. यस्य समीपे यस्य पाठस्तेन सार्द्ध तस्य सम्बन्ध: (बि० टी०)। [रूपसिद्धि]
१. अपीप्यत्। अट् + पा + इन् + चण् + दि। 'पा पाने' (१ । २६४) धातु से "धातोश्च हेतो'' (३। २ । १०) से 'इन्' प्रत्यय, “शाच्छासाह्वाव्यावेपामिनि'' (३। ६ । २१) से 'आय' आदेश, “ते धातवः' (३। २। १६) से 'पायि' की धातुसंज्ञा, अद्यतनीसंज्ञक परस्मैपद-प्रथमपुरुष एकवचन "दि' प्रत्यय, “श्रिद्रुकमिकारितान्तेभ्यश्चण् कर्तरि' (३।२।२६) से ‘चण्' प्रत्यय, 'च्–ण' अनुबन्धों का प्रयोगाभाव, "चण्परोक्षाचक्रीयितसनन्तेषु'' (३। ३ । ७) से धातु को द्विवचन, “पूर्वोऽभ्यास:" (३। ३। ४) से अभ्याससंज्ञा, "अभ्यासस्यादिळञ्जनमवशेष्यम्'' (३। ३। ९) से अभ्यासघटित यकार का लोप, "ह्रस्वः'' (३।३।१५) से अभ्यासघटित आकार को ह्रस्व, प्रकृत सूत्र द्वारा अभ्यासस्थ अकार को ईकारउपधालोप तथा “कारितस्थानामिड्विकरणे'' (३। ६। ४४) से कारितसंज्ञक 'इन्' प्रत्यय का लोप।। ६७८।
६७९. तिष्ठतेरित् [३। ५। ४७] [सूत्रार्थ]
चण्परवर्ती इन् प्रत्यय के परे होने पर 'स्था' धातु की उपधा को इत्त्व होता है।। ६७९।