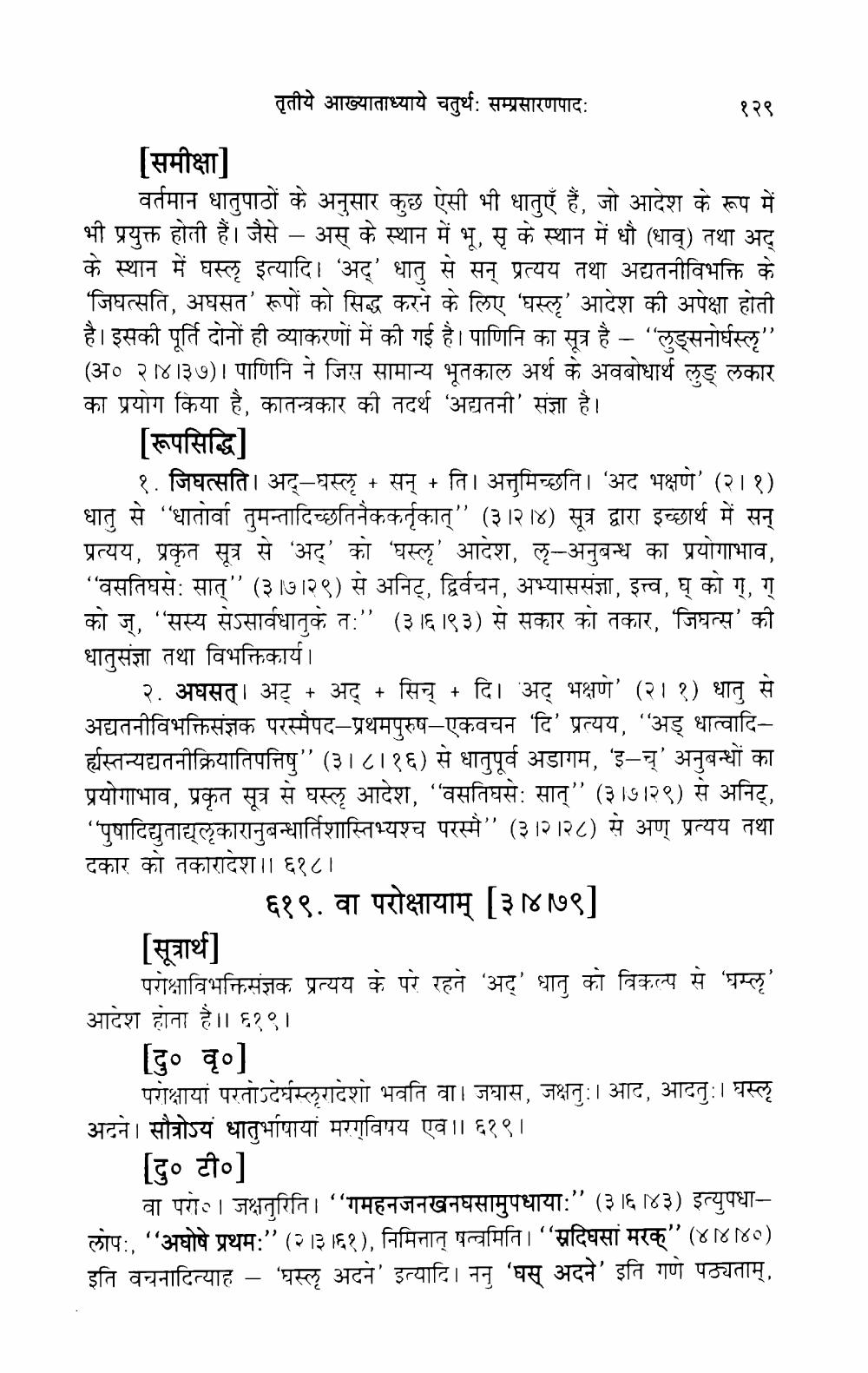________________
तृतीये आख्याताध्याये चतुर्थः सम्प्रसारणपाद:
१२९
[समीक्षा]
वर्तमान धातपाठों के अनुसार कुछ ऐसी भी धातुएँ हैं, जो आदेश के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। जैसे - अस् के स्थान में भू, सू के स्थान में धौ (धाव्) तथा अद् के स्थान में घस्ल इत्यादि। ‘अद्' धातु से सन् प्रत्यय तथा अद्यतनीविभक्ति के 'जिघत्सति, अघसत' रूपों को सिद्ध करने के लिए 'घस्लु' आदेश की अपेक्षा होती है। इसकी पूर्ति दोनों ही व्याकरणों में की गई है। पाणिनि का सूत्र है – “लुङ्सनोर्घस्लु' (अ० २।४।३७)। पाणिनि ने जिस सामान्य भूतकाल अर्थ के अवबोधार्थ लुङ् लकार का प्रयोग किया है, कातन्त्रकार की तदर्थ 'अद्यतनी' संज्ञा है।
[रूपसिद्धि]
१. जिघत्सति। अद्-घस्ल + सन् + ति। अत्तुमिच्छनि। 'अद भक्षणे' (२ । १) धातु से “धातोर्वा तुमन्तादिच्छतिनैककर्तृकात्'' (३।२।४) सूत्र द्वारा इच्छार्थ में सन् प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से 'अद्' को 'घस्ल' आदेश, ल-अनुबन्ध का प्रयोगाभाव, "वसतिघसे: सात्' (३।७।२९) से अनिट, द्विर्वचन, अभ्याससंज्ञा, इत्त्व, घ् को ग, ग् को ज, “सस्य सेऽसार्वधातुके त:" (३।६।९३) से सकार का तकार, जिघत्स' की धातुसंज्ञा तथा विभक्तिकार्य।
२. अघसत्। अट् + अद् + सिच् + दि। अद् भक्षणे' (२। १) धातु से अद्यतनीविभक्तिसंज्ञक परस्मैपद-प्रथमपुरुष–एकवचन 'दि' प्रत्यय, “अड् धात्वादिस्तिन्यद्यतनीक्रियातिपत्तिषु' (३। ८ । १६) से धातुपूर्व अडागम, 'इ–च्' अनुबन्धों का प्रयोगाभाव, प्रकृत सूत्र से घस्लू आदेश, “वसतिघसेः सात्'' (३।७।२९) से अनिट्, “पुषादिद्युताबूलुकारानुबन्धार्तिशास्तिभ्यश्च परस्मै'' (३।२।२८) से अण् प्रत्यय तथा दकार को तकारादेश।। ६१८ ।
६१९. वा परोक्षायाम् [३।४।७९] [सूत्रार्थ]
परोक्षाविभक्तिसंज्ञक प्रत्यय के परे रहते 'अट्' धातु को विकल्प से 'घम्ल' आदेश होता है।। ६१९।
[दु० वृ०]
परोक्षायां परतोऽदेर्घस्लरादेशो भवति वा। जघास, जक्षतुः । आद, आदतुः। घस्ल अदने। सौत्रोऽयं धातु षायां मरग्विषय एव।। ६१९ ।
[दु० टी०]
वा परो । जक्षतुरिति। “गमहनजनखनघसामुपधायाः" (३।६।४३) इत्युपधालोपः, “अघोषे प्रथम:' (२।३।६१), निमित्तात् षत्वमिति। "सदिघसां मरक" (४।४।४०) इति वचनादित्याह – 'घस्ल अदने' इत्यादि। ननु ‘घस् अदने' इति गणे पठ्यताम्,