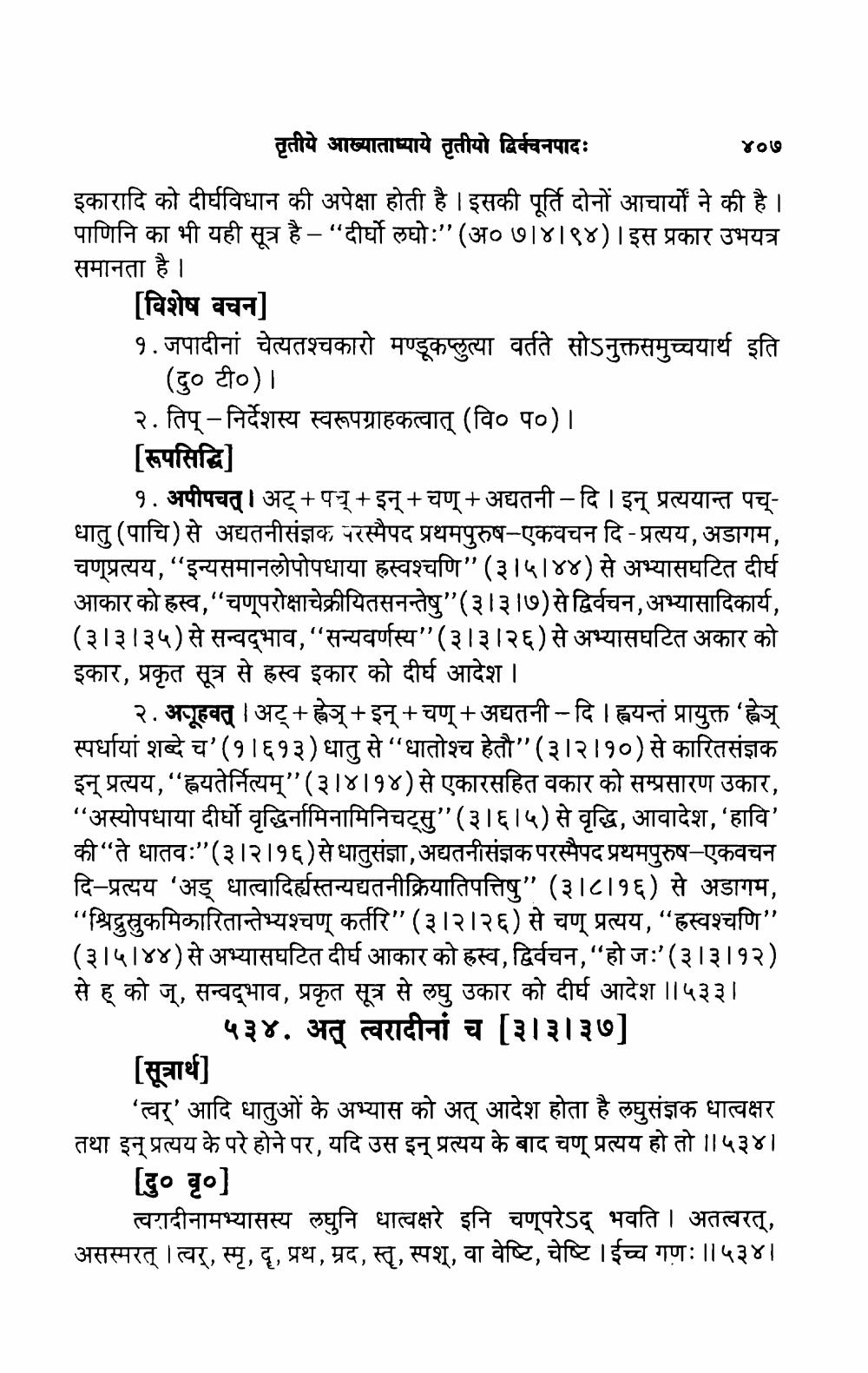________________
तृतीये आख्याताध्याये तृतीयो बिचनपादः
४०७ इकारादि को दीर्घविधान की अपेक्षा होती है | इसकी पूर्ति दोनों आचार्यों ने की है । पाणिनि का भी यही सूत्र है - "दी? लघोः" (अ०७।४।९४) । इस प्रकार उभयत्र समानता है।
[विशेष वचन] १. जपादीनां चेत्यतश्चकारो मण्डूकप्लुत्या वर्तते सोऽनुक्तसमुच्चयार्थ इति
(दु० टी०)। २. तिप् – निर्देशस्य स्वरूपग्राहकत्वात् (वि० प०)। [रूपसिद्धि
१. अपीपचत् । अट् + पच् + इन् + चण् + अद्यतनी - दि । इन् प्रत्ययान्त पच्धातु (पाचि) से अद्यतनीसंज्ञक परस्मैपद प्रथमपुरुष-एकवचन दि-प्रत्यय, अडागम, चण्प्रत्यय, “इन्यसमानलोपोपधाया ह्रस्वश्चणि" (३।५।४४) से अभ्यासघटित दीर्घ आकार को ह्रस्व, “चण्परोक्षाचेक्रीयितसनन्तेषु"(३१३१७)से द्विर्वचन,अभ्यासादिकार्य, (३।३।३५) से सन्वद्भाव, “सन्यवर्णस्य" (३।३।२६) से अभ्यासघटित अकार को इकार, प्रकृत सूत्र से ह्रस्व इकार को दीर्घ आदेश ।
२. अचूहवत् । अट् + ह्वेञ् + इन् + चण् + अद्यतनी-दि । ह्वयन्तं प्रायुक्त 'ह्वेञ् स्पर्धायां शब्दे च' (१।६१३) धातु से “धातोश्च हेतौ" (३।२।१०) से कारितसंज्ञक इन् प्रत्यय, "ह्वयतेर्नित्यम्" (३।४।१४) से एकारसहित वकार को सम्प्रसारण उकार, “अस्योपधाया दीर्घो वृद्धिर्नामिनामिनिचट्सु" (३।६।५) से वृद्धि, आवादेश, ‘हावि' की "ते धातवः"(३।२।१६)से धातुसंज्ञा, अद्यतनीसंज्ञक परस्मैपद प्रथमपुरुष-एकवचन दि-प्रत्यय 'अड़ धात्वादिस्तिन्यद्यतनीक्रियातिपत्तिषु" (३।८।१६) से अडागम, "श्रिद्रुस्रुकमिकारितान्तेभ्यश्चण् कर्तरि" (३।२।२६) से चण प्रत्यय, “हस्वश्चणि" (३।५।४४) से अभ्यासघटित दीर्घ आकार को ह्रस्व, द्विर्वचन, "हो जः' (३।३।१२) से ह को ज्, सन्वद्भाव, प्रकृत सूत्र से लघु उकार को दीर्घ आदेश ।। ५३३।
५३४. अत् त्वरादीनां च [३।३।३७] [सूत्रार्थ]
'त्वर' आदि धातुओं के अभ्यास को अत् आदेश होता है लघुसंज्ञक धात्वक्षर तथा इन् प्रत्यय के परे होने पर, यदि उस इन् प्रत्यय के बाद चण् प्रत्यय हो तो ।। ५३४।
[दु० वृ०]
त्वरादीनामभ्यासस्य लघुनि धात्वक्षरे इनि चण्परेऽद् भवति । अतत्वरत्, असस्मरत् । त्वर्, स्मृ, दृ, प्रथ, म्रद, स्तृ, स्पश्, वा वेष्टि, चेष्टि । ईच्च गणः ।। ५३४ ।