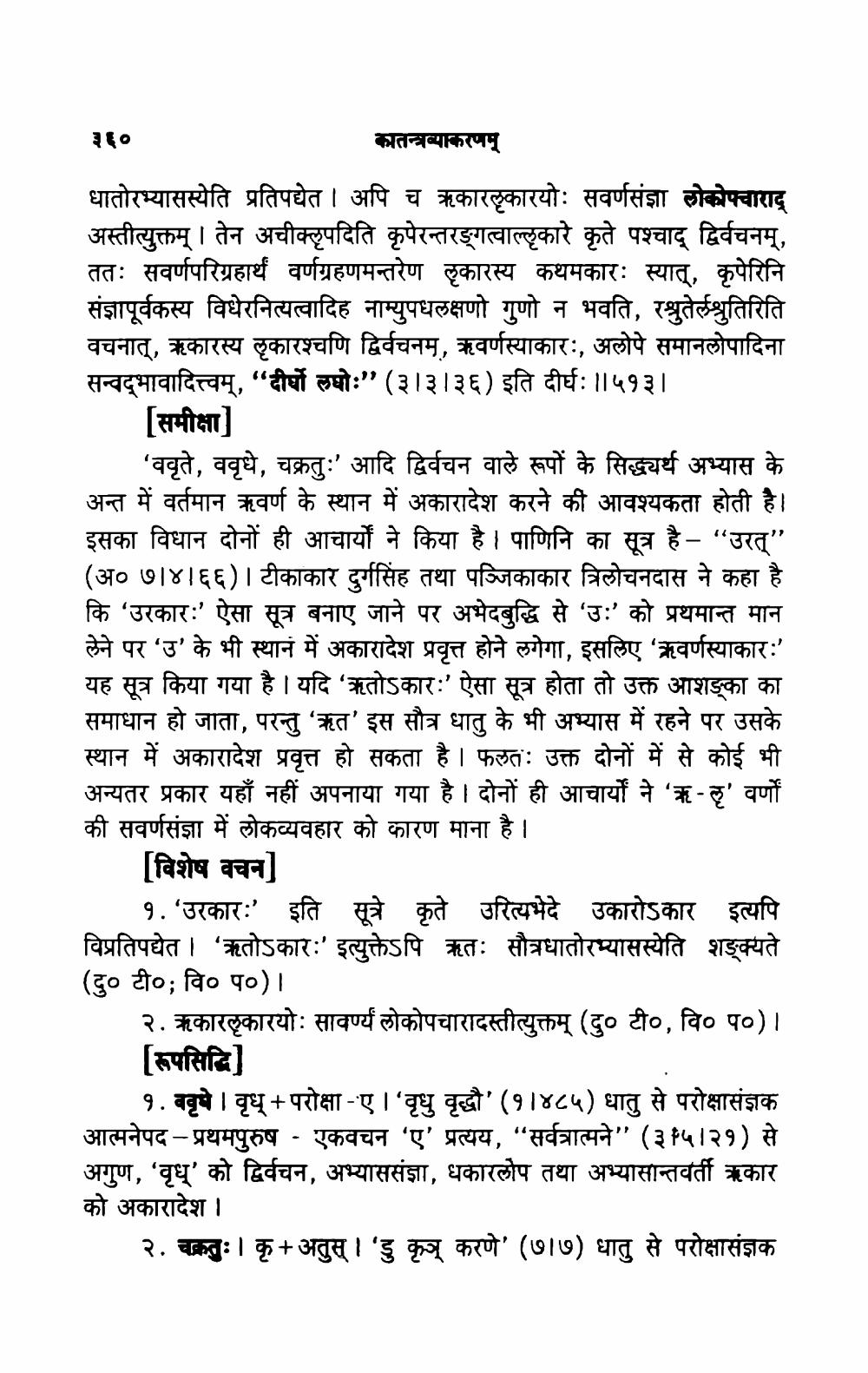________________
३६०
कातन्त्रव्याकरणम्
धातोरभ्यासस्येति प्रतिपद्येत । अपि च ऋकारटुकारयोः सवर्णसंज्ञा लोकोपचाराद् अस्तीत्युक्तम् । तेन अचीक्लृपदिति कृपेरन्तरङ्गत्वाल्लुकारे कृते पश्चाद् द्विवचनम्, ततः सवर्णपरिग्रहार्थं वर्णग्रहणमन्तरेण लकारस्य कथमकारः स्यात, कपेरिनि संज्ञापूर्वकस्य विधेरनित्यत्वादिह नाम्युपधलक्षणो गुणो न भवति, रश्रुतेर्लश्रुतिरिति वचनात्, ऋकारस्य लुकारश्चणि द्विवचनम, ऋवर्णस्याकारः, अलोपे समानलोपादिना सन्वद्भावादित्त्वम्, “दीर्घा लघोः" (३।३।३६) इति दीर्घः ।।५१३ |
[समीक्षा]
'ववृते, ववृधे, चक्रतुः' आदि द्विवचन वाले रूपों के सिद्ध्यर्थ अभ्यास के अन्त में वर्तमान ऋवर्ण के स्थान में अकारादेश करने की आवश्यकता होती है। इसका विधान दोनों ही आचार्यों ने किया है। पाणिनि का सूत्र है- “उरत्" (अ० ७।४।६६)। टीकाकार दुर्गसिंह तथा पञ्जिकाकार त्रिलोचनदास ने कहा है कि 'उरकारः' ऐसा सूत्र बनाए जाने पर अभेदबुद्धि से 'उः' को प्रथमान्त मान लेने पर 'उ' के भी स्थान में अकारादेश प्रवृत्त होने लगेगा, इसलिए 'ऋवर्णस्याकारः' यह सूत्र किया गया है । यदि 'ऋतोऽकारः' ऐसा सूत्र होता तो उक्त आशङ्का का समाधान हो जाता, परन्तु 'ऋत' इस सौत्र धातु के भी अभ्यास में रहने पर उसके स्थान में अकारादेश प्रवृत्त हो सकता है। फलतः उक्त दोनों में से कोई भी अन्यतर प्रकार यहाँ नहीं अपनाया गया है। दोनों ही आचार्यों ने 'क्र-तृ' वर्गों की सवर्णसंज्ञा में लोकव्यवहार को कारण माना है।
[विशेष वचन]
१. 'उरकारः' इति सूत्रे कृते उरित्यभेदे उकारोऽकार इत्यपि विप्रतिपद्येत । 'ऋतोऽकारः' इत्युक्तेऽपि ऋतः सौत्रधातोरभ्यासस्येति शक्यते (दु० टी०; वि० प०)।
२. ऋकारटुकारयोः सावर्ण्य लोकोपचारादस्तीत्युक्तम् (दु० टी०, वि० प०)। [रूपसिदि]
१. बवृषे । वृध् + परोक्षा-ए । 'वृधु वृद्धौ' (१।४८५) धातु से परोक्षासंज्ञक आत्मनेपद-प्रथमपुरुष - एकवचन 'ए' प्रत्यय, "सर्वत्रात्मने" (३१५/२१) से अगुण, 'वृध्' को द्विर्वचन, अभ्याससंज्ञा, धकारलोप तथा अभ्यासान्तवर्ती ऋकार को अकारादेश।
२. चक्रतुः। कृ + अतुस् । 'डु कृञ् करणे' (७।७) धातु से परोक्षासंज्ञक