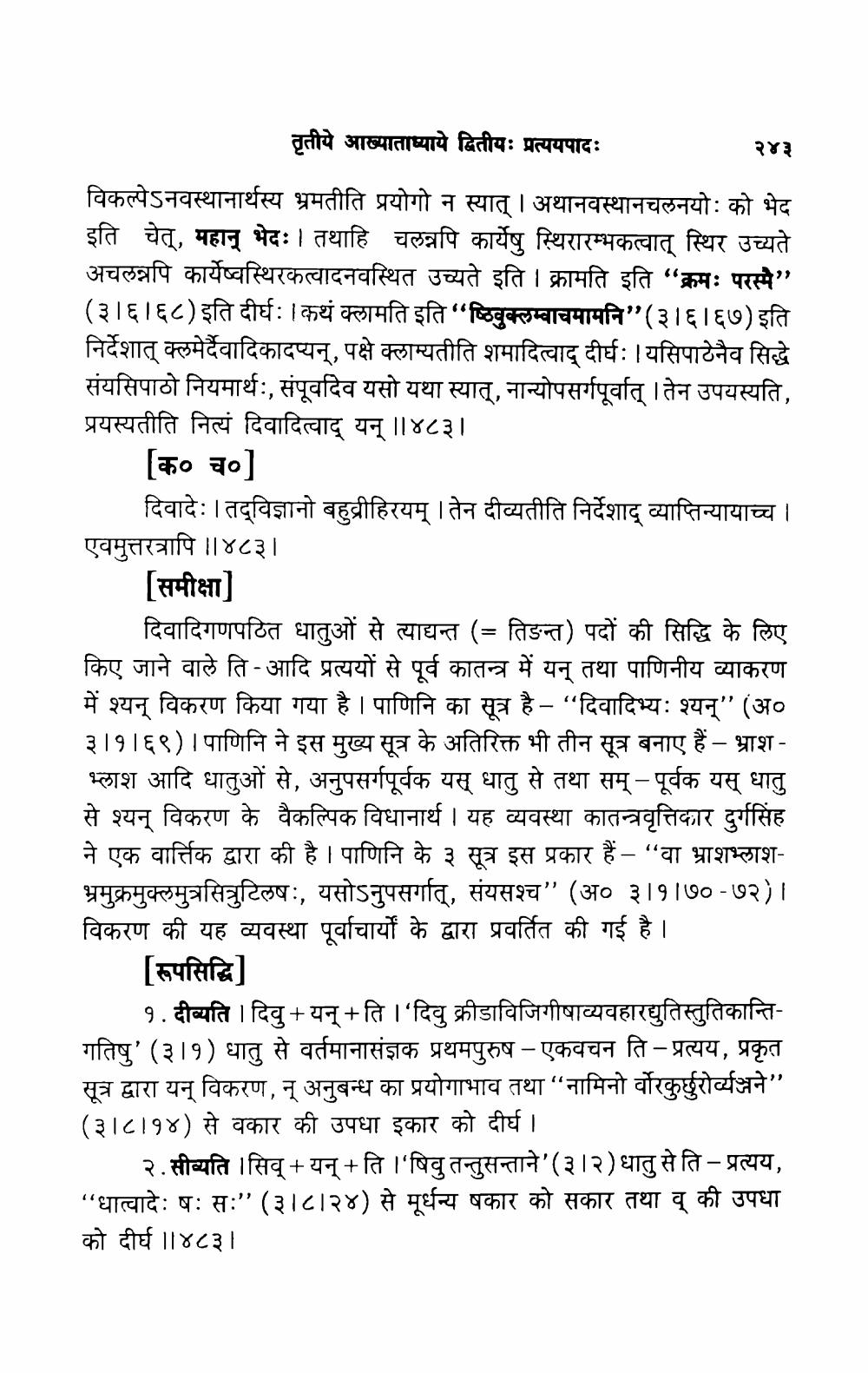________________
तृतीये आख्याताध्याये द्वितीयः प्रत्ययपादः
२४३ विकल्पेऽनवस्थानार्थस्य भ्रमतीति प्रयोगो न स्यात् । अथानवस्थानचलनयोः को भेद इति चेत्, महान् भेदः । तथाहि चलन्नपि कार्येषु स्थिरारम्भकत्वात् स्थिर उच्यते अचलन्नपि कार्येष्वस्थिरकत्वादनवस्थित उच्यते इति । क्रामति इति "क्रमः परस्मै" (३।६।६८) इति दीर्घः । कथं क्लामति इति "ष्ठिवुक्लम्बाचमामनि"(३।६।६७) इति निर्देशात् क्लमेर्देवादिकादप्यन्, पक्षे क्लाम्यतीति शमादित्वाद् दीर्घः । यसिपाठेनैव सिद्धे संयसिपाठो नियमार्थः, संपूवदिव यसो यथा स्यात्, नान्योपसर्गपूर्वात् । तेन उपयस्यति, प्रयस्यतीति नित्यं दिवादित्वाद् यन् ।।४८३ ।
[क० च०]
दिवादेः । तद्विज्ञानो बहुव्रीहिरयम् । तेन दीव्यतीति निर्देशाद् व्याप्तिन्यायाच्च । एवमुत्तरत्रापि ।। ४८३।
[समीक्षा]
दिवादिगणपठित धातुओं से त्याद्यन्त (= तिङन्त) पदों की सिद्धि के लिए किए जाने वाले ति - आदि प्रत्ययों से पूर्व कातन्त्र में यन् तथा पाणिनीय व्याकरण में श्यन् विकरण किया गया है | पाणिनि का सूत्र है - "दिवादिभ्यः श्यन्' (अ० ३।१।६९) । पाणिनि ने इस मुख्य सूत्र के अतिरिक्त भी तीन सूत्र बनाए हैं - भ्राशभ्लाश आदि धातुओं से, अनुपसर्गपूर्वक यस् धातु से तथा सम् – पूर्वक यस् धातु से श्यन् विकरण के वैकल्पिक विधानार्थ । यह व्यवस्था कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गसिंह ने एक वार्त्तिक द्वारा की है | पाणिनि के ३ सूत्र इस प्रकार हैं – “वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः, यसोऽनुपसर्गात्, संयसश्च' (अ० ३।१।७० -७२)। विकरण की यह व्यवस्था पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रवर्तित की गई है ।
[रूपसिद्धि]
१. दीव्यति । दिवु + यन् + ति । 'दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिकान्तिगतिषु' (३।१) धातु से वर्तमानासंज्ञक प्रथमपुरुष – एकवचन ति - प्रत्यय, प्रकृत सूत्र द्वारा यन् विकरण, न् अनुबन्ध का प्रयोगाभाव तथा "नामिनो र्वोरकुर्छरोर्व्यञ्जने" (३।८।१४) से वकार की उपधा इकार को दीर्घ ।
२. सीव्यति ।सिव् + यन् + ति । षिवु तन्तुसन्ताने' (३।२) धातु से ति - प्रत्यय, "धात्वादेः षः सः' (३।८।२४) से मूर्धन्य षकार को सकार तथा व् की उपधा को दीर्घ || ४८३।