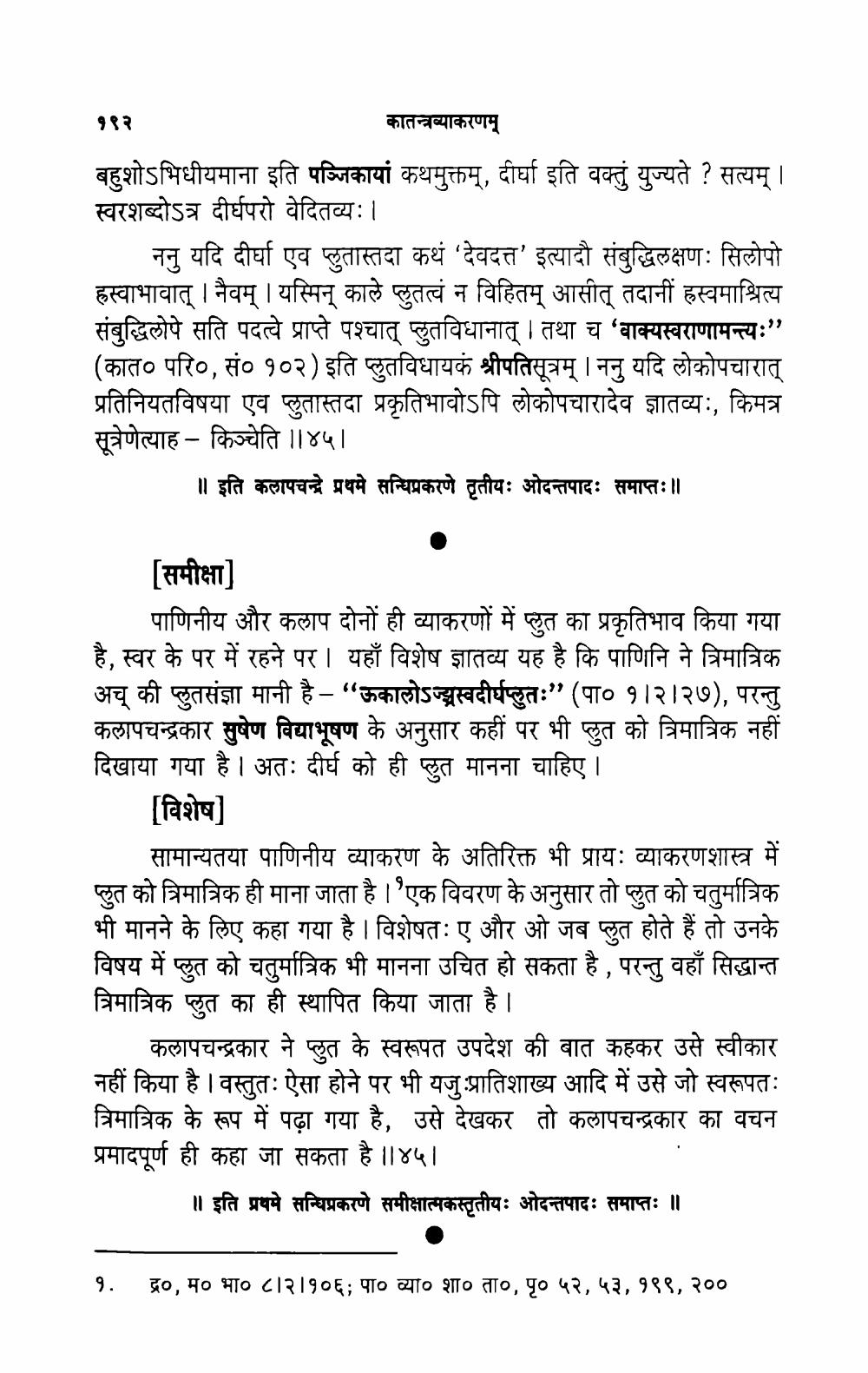________________
१९२
कातन्त्रव्याकरणम् बहुशोऽभिधीयमाना इति पञिकायां कथमुक्तम्, दीर्घा इति वक्तुं युज्यते ? सत्यम् । स्वरशब्दोऽत्र दीर्घपरो वेदितव्यः ।
ननु यदि दीर्घा एव प्लुतास्तदा कथं 'देवदत्त' इत्यादौ संबुद्धिलक्षणः सिलोपो हस्वाभावात् । नैवम् । यस्मिन् काले प्लुतत्वं न विहितम् आसीत् तदानीं ह्रस्वमाश्रित्य संबुद्धिलोपे सति पदत्वे प्राप्ते पश्चात् प्लुतविधानात् । तथा च 'वाक्यस्वराणामन्त्यः" (कात० परि०, सं० १०२) इति प्लुतविधायकं श्रीपतिसूत्रम् । ननु यदि लोकोपचारात् प्रतिनियतविषया एव प्लुतास्तदा प्रकृतिभावोऽपि लोकोपचारादेव ज्ञातव्यः, किमत्र सूत्रेणेत्याह - किञ्चेति ।।४५।
॥ इति कलापचन्द्रे प्रथमे सन्धिप्रकरणे तृतीयः ओदन्तपादः समाप्तः॥
[समीक्षा]
पाणिनीय और कलाप दोनों ही व्याकरणों में प्लुत का प्रकृतिभाव किया गया है, स्वर के पर में रहने पर | यहाँ विशेष ज्ञातव्य यह है कि पाणिनि ने त्रिमात्रिक अच् की प्लुतसंज्ञा मानी है - "ऊकालोऽज्यस्वदीर्घप्लुतः" (पा० १।२।२७), परन्तु कलापचन्द्रकार सुषेण विद्याभूषण के अनुसार कहीं पर भी प्लुत को त्रिमात्रिक नहीं दिखाया गया है । अतः दीर्घ को ही प्लुत मानना चाहिए ।
[विशेष]
सामान्यतया पाणिनीय व्याकरण के अतिरिक्त भी प्रायः व्याकरणशास्त्र में प्लुत को त्रिमात्रिक ही माना जाता है ।' एक विवरण के अनुसार तो प्लुत को चतुर्मात्रिक भी मानने के लिए कहा गया है । विशेषतः ए और ओ जब प्लुत होते हैं तो उनके विषय में प्लुत को चतुर्मात्रिक भी मानना उचित हो सकता है , परन्तु वहाँ सिद्धान्त त्रिमात्रिक प्लुत का ही स्थापित किया जाता है |
कलापचन्द्रकार ने प्लुत के स्वरूपत उपदेश की बात कहकर उसे स्वीकार नहीं किया है । वस्तुतः ऐसा होने पर भी यजुःप्रातिशाख्य आदि में उसे जो स्वरूपतः त्रिमात्रिक के रूप में पढ़ा गया है, उसे देखकर तो कलापचन्द्रकार का वचन प्रमादपूर्ण ही कहा जा सकता है ।। ४५।
॥ इति प्रथमे सन्धिप्रकरणे समीक्षात्मकस्तृतीयः ओदन्तपादः समाप्तः ॥
१.
द्र०, म० भा०८।२।१०६; पा० व्या० शा० ता०, पृ० ५२, ५३, १९९, २००