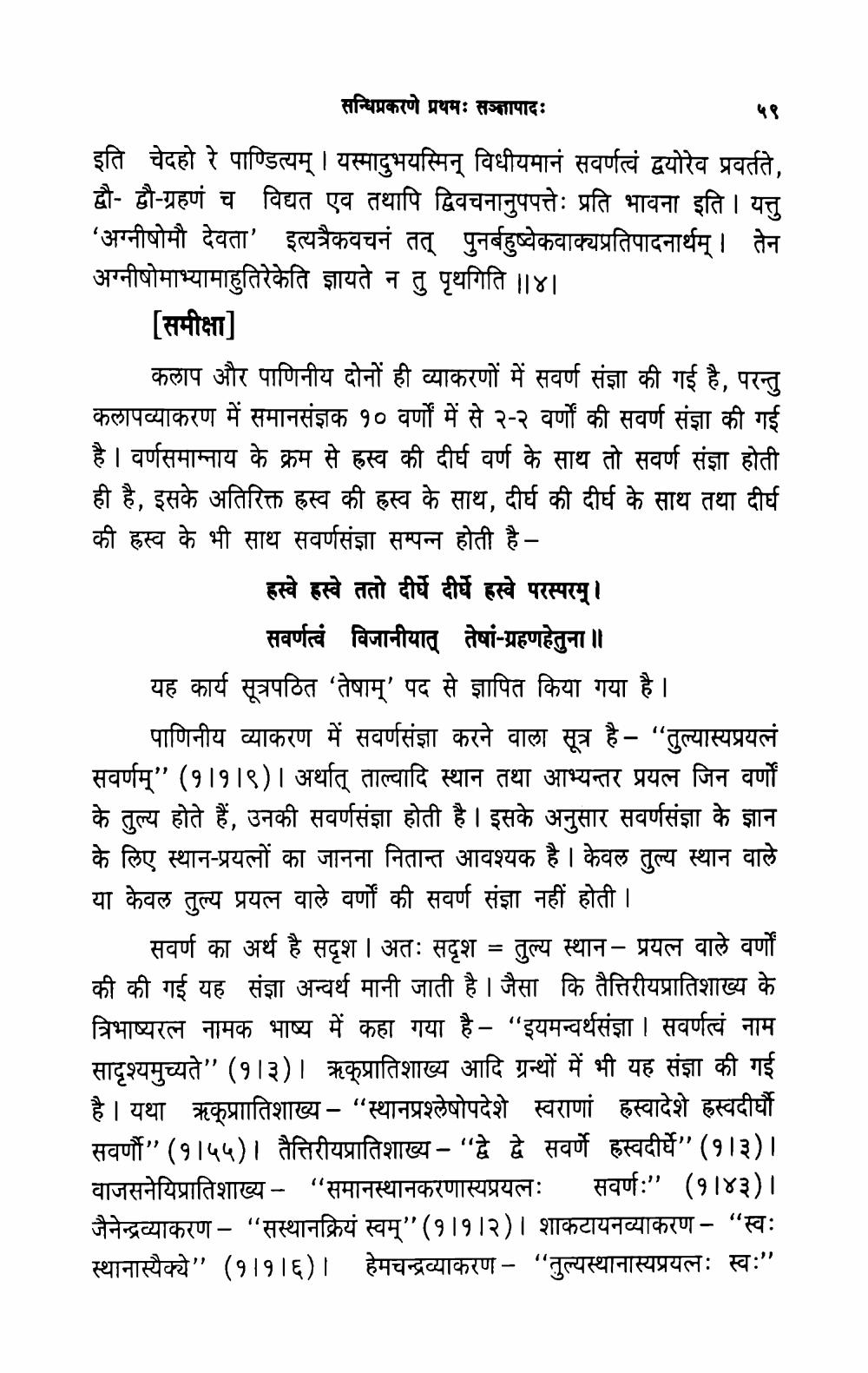________________
सन्धिप्रकरणे प्रथमः सज्ञापादः इति चेदहो रे पाण्डित्यम् । यस्मादुभयस्मिन् विधीयमानं सवर्णत्वं द्वयोरेव प्रवर्तते, द्वौ- द्वौ-ग्रहणं च विद्यत एव तथापि द्विवचनानुपपत्तेः प्रति भावना इति । यत्तु 'अग्नीषोमौ देवता' इत्यत्रैकवचनं तत् पुनर्बहुष्वेकवाक्यप्रतिपादनार्थम् । तेन अग्नीषोमाभ्यामाहुतिरेकेति ज्ञायते न तु पृथगिति ।।४।
[समीक्षा]
कलाप और पाणिनीय दोनों ही व्याकरणों में सवर्ण संज्ञा की गई है, परन्तु कलापव्याकरण में समानसंज्ञक १० वर्गों में से २-२ वर्गों की सवर्ण संज्ञा की गई है । वर्णसमाम्नाय के क्रम से ह्रस्व की दीर्घ वर्ण के साथ तो सवर्ण संज्ञा होती ही है, इसके अतिरिक्त ह्रस्व की ह्रस्व के साथ, दीर्घ की दीर्घ के साथ तथा दीर्घ की ह्रस्व के भी साथ सवर्णसंज्ञा सम्पन्न होती है -
हस्ते हस्वे ततो दीर्घे दीर्घ हस्वे परस्परम् ।
सवर्णत्वं विजानीयात् तेषां-ग्रहणहेतुना ॥ यह कार्य सूत्रपठित 'तेषाम्' पद से ज्ञापित किया गया है |
पाणिनीय व्याकरण में सवर्णसंज्ञा करने वाला सूत्र है- "तुल्यास्यप्रयलं सवर्णम्" (१।१।९)। अर्थात् ताल्वादि स्थान तथा आभ्यन्तर प्रयल जिन वर्णों के तुल्य होते हैं, उनकी सवर्णसंज्ञा होती है । इसके अनुसार सवर्णसंज्ञा के ज्ञान के लिए स्थान-प्रयत्नों का जानना नितान्त आवश्यक है । केवल तुल्य स्थान वाले या केवल तुल्य प्रयत्न वाले वर्गों की सवर्ण संज्ञा नहीं होती ।
सवर्ण का अर्थ है सदृश । अतः सदृश = तुल्य स्थान - प्रयत्न वाले वर्गों की की गई यह संज्ञा अन्वर्थ मानी जाती है । जैसा कि तैत्तिरीयप्रातिशाख्य के त्रिभाष्यरत्न नामक भाष्य में कहा गया है - "इयमन्वर्थसंज्ञा । सवर्णत्वं नाम सादृश्यमुच्यते' (१।३)। ऋप्रातिशाख्य आदि ग्रन्थों में भी यह संज्ञा की गई है । यथा ऋक्प्रातिशाख्य - "स्थानप्रश्लेषोपदेशे स्वराणां ह्रस्वादेशे ह्रस्वदी? सवर्णी" (१।५५)। तैत्तिरीयप्रातिशाख्य - "द्वे द्वे सवर्णे हस्वदीर्घ' (१।३)। वाजसनेयिप्रातिशाख्य - "समानस्थानकरणास्यप्रयत्नः सवर्णः” (१।४३)। जैनेन्द्रव्याकरण - "सस्थानक्रियं स्वम्” (१।१।२)। शाकटायनव्याकरण - "स्वः स्थानास्यैक्ये' (१।१।६)। हेमचन्द्रव्याकरण - "तुल्यस्थानास्यप्रयत्नः स्वः"