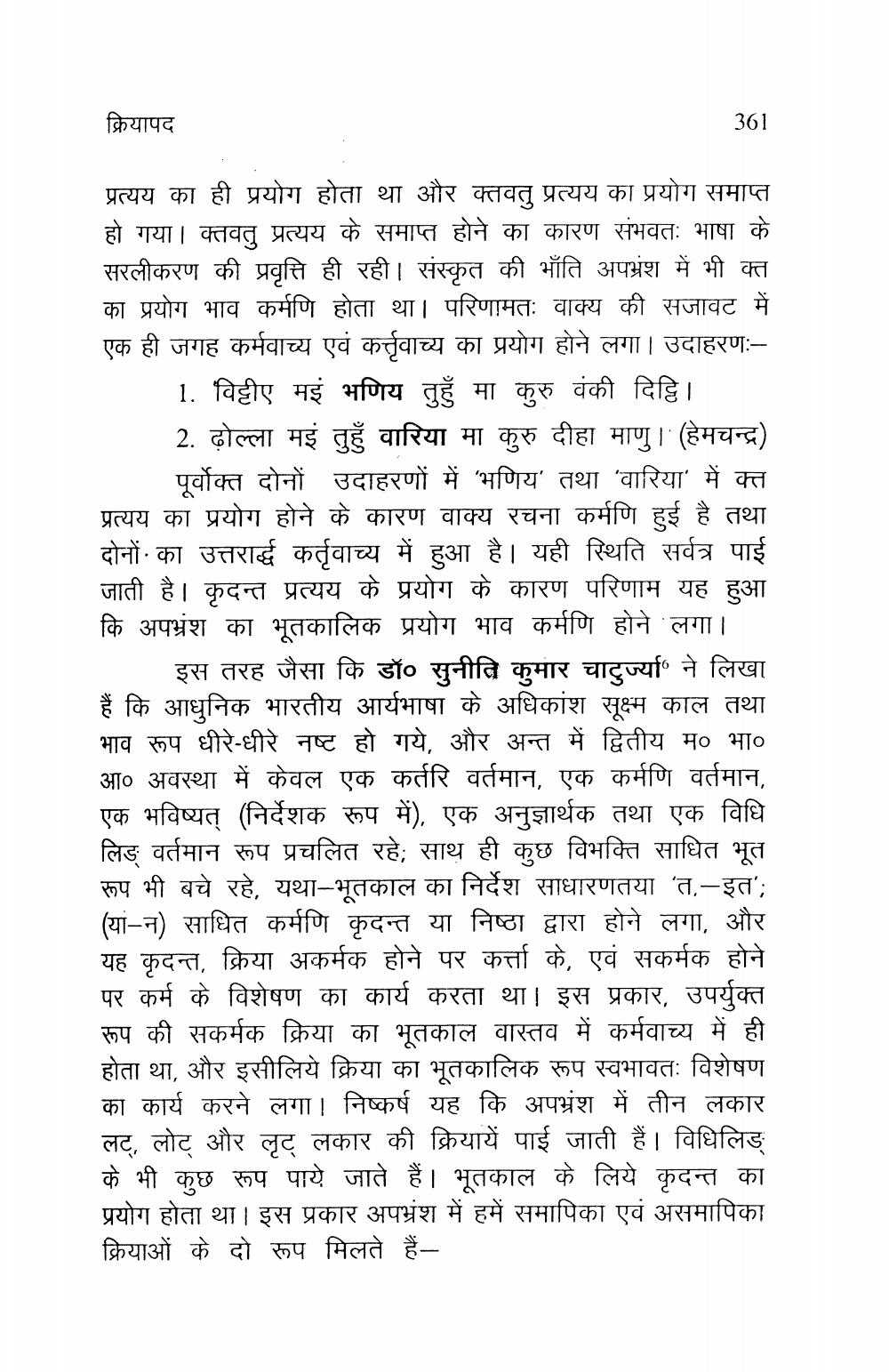________________
क्रियापद
361
प्रत्यय का ही प्रयोग होता था और क्तवतु प्रत्यय का प्रयोग समाप्त हो गया। क्तवतु प्रत्यय के समाप्त होने का कारण संभवतः भाषा के सरलीकरण की प्रवृत्ति ही रही। संस्कृत की भाँति अपभ्रंश में भी क्त का प्रयोग भाव कर्मणि होता था। परिणामतः वाक्य की सजावट में एक ही जगह कर्मवाच्य एवं कर्तृवाच्य का प्रयोग होने लगा। उदाहरण:
1. 'विट्टीए मई भणिय तुहुँ मा कुरु वंकी दिट्ठि। 2. ढोल्ला मई तुहुँ वारिया मा कुरु दीहा माणु। (हेमचन्द्र)
पूर्वोक्त दोनों उदाहरणों में 'भणिय' तथा 'वारिया' में क्त्त प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण वाक्य रचना कर्मणि हुई है तथा दोनों का उत्तरार्द्ध कर्तृवाच्य में हुआ है। यही स्थिति सर्वत्र पाई जाती है। कृदन्त प्रत्यय के प्रयोग के कारण परिणाम यह हुआ कि अपभ्रंश का भूतकालिक प्रयोग भाव कर्मणि होने लगा।
इस तरह जैसा कि डॉ० सुनीति कुमार चाट्ा ने लिखा हैं कि आधुनिक भारतीय आर्यभाषा के अधिकांश सूक्ष्म काल तथा भाव रूप धीरे-धीरे नष्ट हो गये, और अन्त में द्वितीय म० भा० आo अवस्था में केवल एक कर्तरि वर्तमान, एक कर्मणि वर्तमान, एक भविष्यत् (निर्देशक रूप में), एक अनुज्ञार्थक तथा एक विधि लिङ वर्तमान रूप प्रचलित रहे; साथ ही कुछ विभक्ति साधित भूत रूप भी बचे रहे, यथा-भूतकाल का निर्देश साधारणतया 'त,-इत'; (या-न) साधित कर्मणि कृदन्त या निष्ठा द्वारा होने लगा, और यह कृदन्त, क्रिया अकर्मक होने पर कर्त्ता के, एवं सकर्मक होने पर कर्म के विशेषण का कार्य करता था। इस प्रकार, उपर्युक्त रूप की सकर्मक क्रिया का भूतकाल वास्तव में कर्मवाच्य में ही होता था, और इसीलिये क्रिया का भूतकालिक रूप स्वभावतः विशेषण का कार्य करने लगा। निष्कर्ष यह कि अपभ्रंश में तीन लकार लट्, लोट् और लृट् लकार की क्रियायें पाई जाती हैं। विधिलिङ् के भी कुछ रूप पाये जाते हैं। भूतकाल के लिये कृदन्त का प्रयोग होता था। इस प्रकार अपभ्रंश में हमें समापिका एवं असमापिका क्रियाओं के दो रूप मिलते हैं