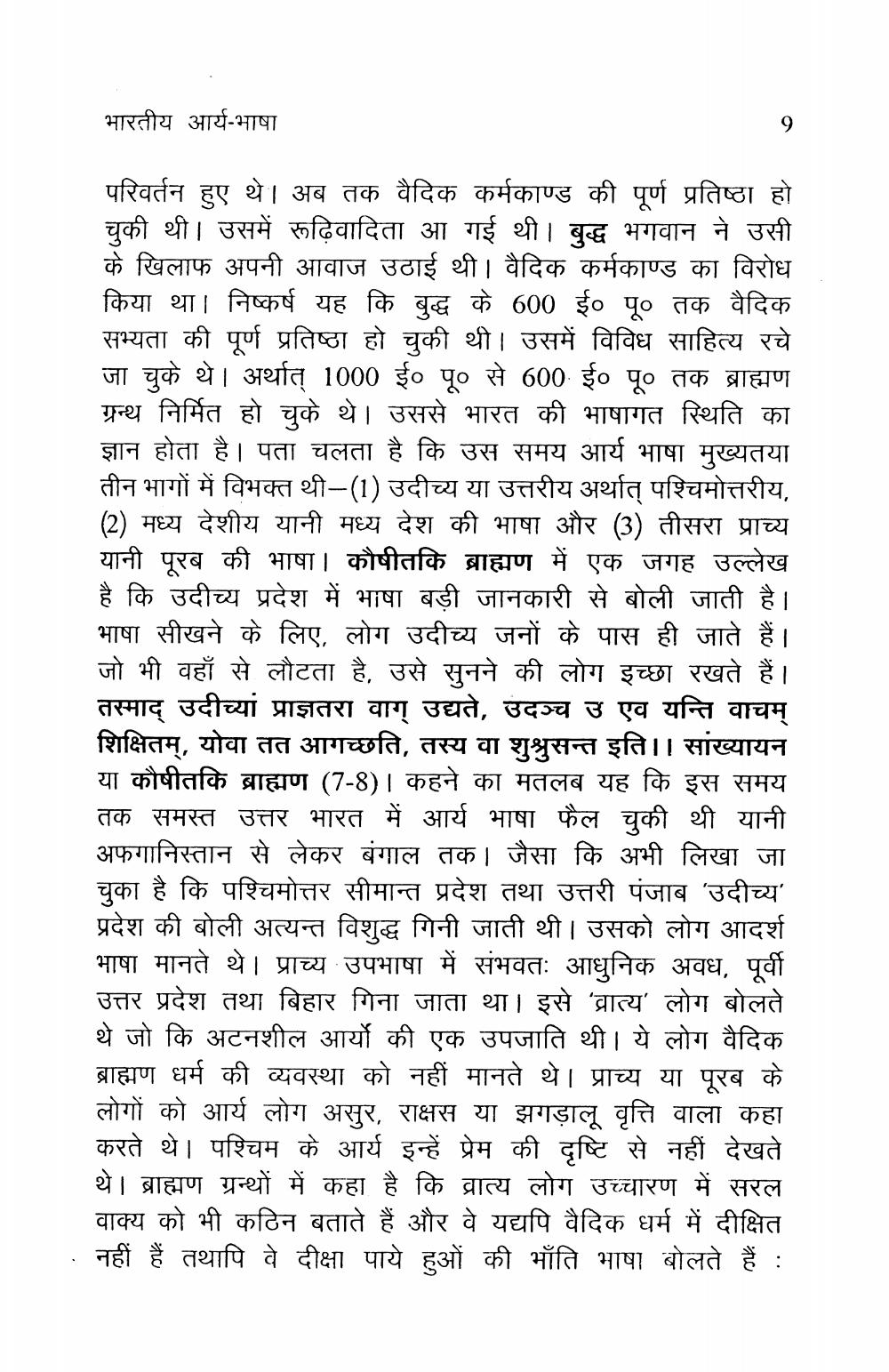________________
भारतीय आर्य-भाषा
परिवर्तन हुए थे। अब तक वैदिक कर्मकाण्ड की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसमें रूढ़िवादिता आ गई थी। बुद्ध भगवान ने उसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। वैदिक कर्मकाण्ड का विरोध किया था। निष्कर्ष यह कि बुद्ध के 600 ई० पू० तक वैदिक सभ्यता की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसमें विविध साहित्य रचे जा चुके थे। अर्थात् 1000 ई० पू० से 600 ई० पू० तक ब्राह्मण ग्रन्थ निर्मित हो चुके थे। उससे भारत की भाषागत स्थिति का ज्ञान होता है। पता चलता है कि उस समय आर्य भाषा मुख्यतया तीन भागों में विभक्त थी-(1) उदीच्य या उत्तरीय अर्थात् पश्चिमोत्तरीय, (2) मध्य देशीय यानी मध्य देश की भाषा और (3) तीसरा प्राच्य यानी पूरब की भाषा। कौषीतकि ब्राह्मण में एक जगह उल्लेख है कि उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ी जानकारी से बोली जाती है। भाषा सीखने के लिए, लोग उदीच्य जनों के पास ही जाते हैं। जो भी वहाँ से लौटता है, उसे सुनने की लोग इच्छा रखते हैं। तस्माद् उदीच्यां प्राज्ञतरा वाग् उद्यते, उदञ्च उ एव यन्ति वाचम् शिक्षितम्, योवा तत आगच्छति, तस्य वा शुश्रुसन्त इति।। सांख्यायन या कौषीतकि ब्राह्मण (7-8)। कहने का मतलब यह कि इस समय तक समस्त उत्तर भारत में आर्य भाषा फैल चुकी थी यानी अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक। जैसा कि अभी लिखा जा चुका है कि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश तथा उत्तरी पंजाब "उदीच्य' प्रदेश की बोली अत्यन्त विशुद्ध गिनी जाती थी। उसको लोग आदर्श भाषा मानते थे। प्राच्य उपभाषा में संभवतः आधुनिक अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार गिना जाता था। इसे 'व्रात्य' लोग बोलते थे जो कि अटनशील आर्यो की एक उपजाति थी। ये लोग वैदिक ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था को नहीं मानते थे। प्राच्य या पूरब के लोगों को आर्य लोग असुर, राक्षस या झगड़ालू वृत्ति वाला कहा करते थे। पश्चिम के आर्य इन्हें प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते थे। ब्राह्मण ग्रन्थों में कहा है कि व्रात्य लोग उच्चारण में सरल वाक्य को भी कठिन बताते हैं और वे यद्यपि वैदिक धर्म में दीक्षित . नहीं हैं तथापि वे दीक्षा पाये हुओं की भाँति भाषा बोलते हैं :