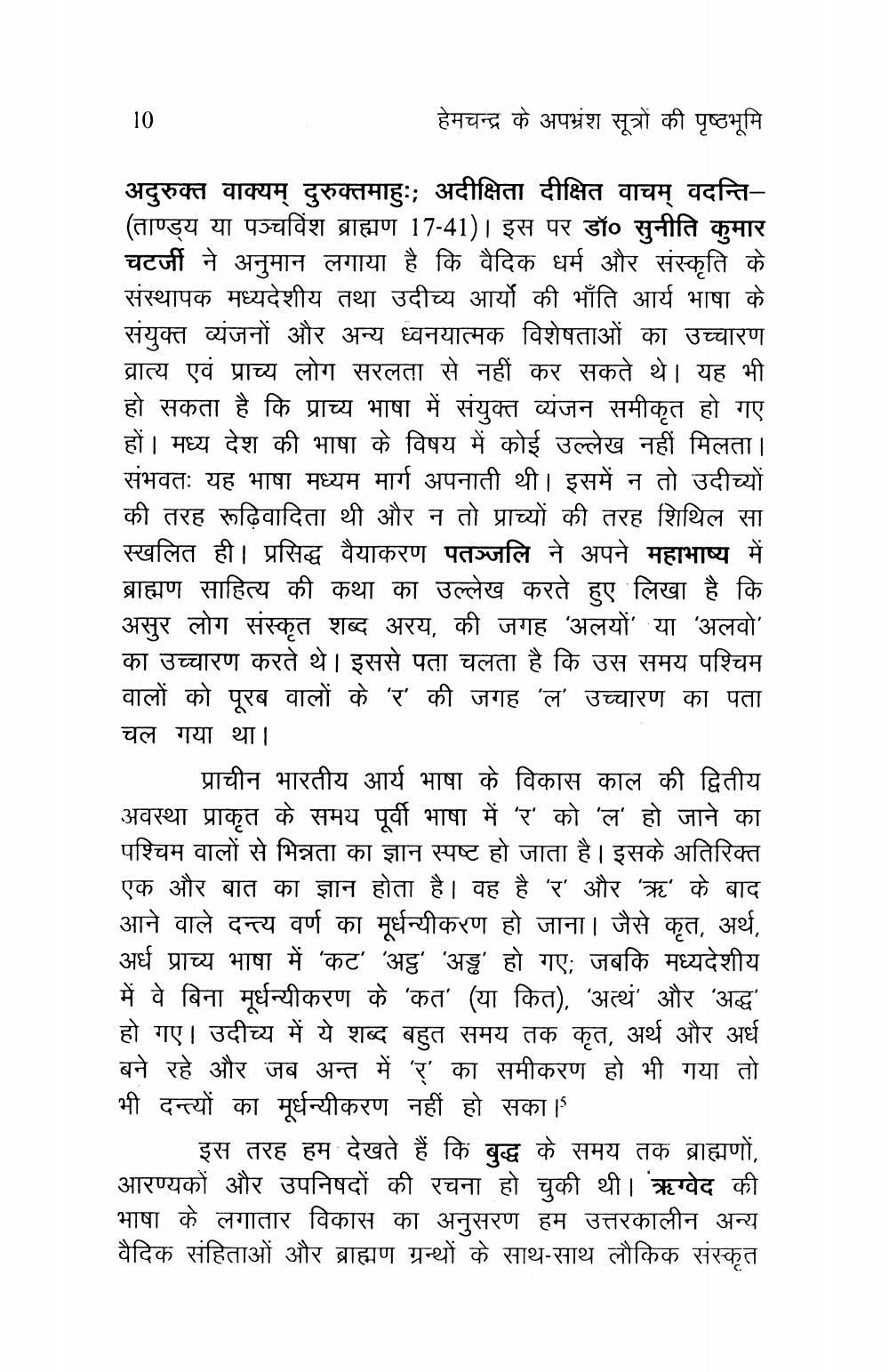________________
10
हेमचन्द्र के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि
अदुरुक्त वाक्यम् दुरुक्तमाहः; अदीक्षिता दीक्षित वाचम् वदन्ति(ताण्ड्य या पञ्चविंश ब्राह्मण 17-41)। इस पर डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी ने अनुमान लगाया है कि वैदिक धर्म और संस्कृति के संस्थापक मध्यदेशीय तथा उदीच्य आर्यों की भाँति आर्य भाषा के संयुक्त व्यंजनों और अन्य ध्वनयात्मक विशेषताओं का उच्चारण व्रात्य एवं प्राच्य लोग सरलता से नहीं कर सकते थे। यह भी हो सकता है कि प्राच्य भाषा में संयुक्त व्यंजन समीकृत हो गए हों। मध्य देश की भाषा के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। संभवतः यह भाषा मध्यम मार्ग अपनाती थी। इसमें न तो उदीच्यों की तरह रूढ़िवादिता थी और न तो प्राच्यों की तरह शिथिल सा स्खलित ही। प्रसिद्ध वैयाकरण पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में ब्राह्मण साहित्य की कथा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि असुर लोग संस्कृत शब्द अरय, की जगह 'अलयों' या 'अलवो' का उच्चारण करते थे। इससे पता चलता है कि उस समय पश्चिम वालों को पूरब वालों के 'र' की जगह 'ल' उच्चारण का पता चल गया था।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के विकास काल की द्वितीय अवस्था प्राकृत के समय पूर्वी भाषा में 'र' को 'ल' हो जाने का पश्चिम वालों से भिन्नता का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात का ज्ञान होता है। वह है 'र' और 'ऋ' के बाद आने वाले दन्त्य वर्ण का मूर्धन्यीकरण हो जाना। जैसे कृत, अर्थ, अर्ध प्राच्य भाषा में 'कट' 'अट्ट' 'अड्ड' हो गए; जबकि मध्यदेशीय में वे बिना मूर्धन्यीकरण के 'कत' (या कित), 'अत्यं' और 'अद्ध' हो गए। उदीच्य में ये शब्द बहुत समय तक कृत, अर्थ और अर्ध बने रहे और जब अन्त में 'र' का समीकरण हो भी गया तो भी दन्त्यों का मूर्धन्यीकरण नहीं हो सका।
इस तरह हम देखते हैं कि बुद्ध के समय तक ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हो चुकी थी। ऋग्वेद की भाषा के लगातार विकास का अनुसरण हम उत्तरकालीन अन्य वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ-साथ लौकिक संस्कृत