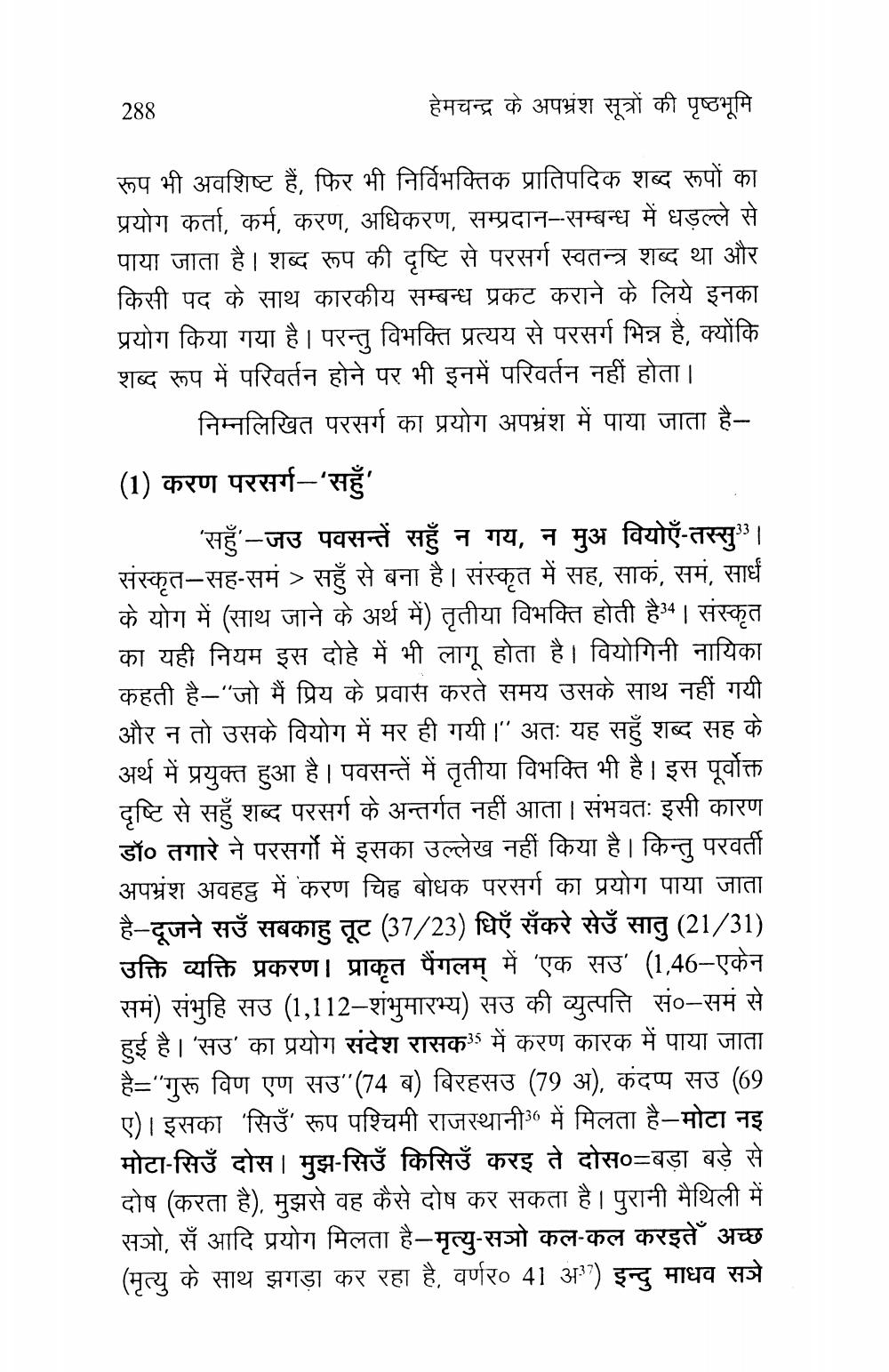________________
288
हेमचन्द्र के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि
रूप भी अवशिष्ट हैं, फिर भी निर्विभक्तिक प्रातिपदिक शब्द रूपों का प्रयोग कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, सम्प्रदान-सम्बन्ध में धड़ल्ले से पाया जाता है। शब्द रूप की दृष्टि से परसर्ग स्वतन्त्र शब्द था और किसी पद के साथ कारकीय सम्बन्ध प्रकट कराने के लिये इनका प्रयोग किया गया है। परन्तु विभक्ति प्रत्यय से परसर्ग भिन्न है, क्योंकि शब्द रूप में परिवर्तन होने पर भी इनमें परिवर्तन नहीं होता।
निम्नलिखित परसर्ग का प्रयोग अपभ्रंश में पाया जाता है(1) करण परसर्ग-'सहुँ'
'सहुँ'-जउ पवसन्तें सहुँ न गय, न मुअ वियोएँ-तस्सु। संस्कृत-सह-समं > सहुँ से बना है। संस्कृत में सह, साकं, समं, सार्धं के योग में (साथ जाने के अर्थ में) तृतीया विभक्ति होती है | संस्कृत का यही नियम इस दोहे में भी लागू होता है। वियोगिनी नायिका कहती है-"जो मैं प्रिय के प्रवास करते समय उसके साथ नहीं गयी
और न तो उसके वियोग में मर ही गयी। अतः यह सहुँ शब्द सह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पवसन्ते में तृतीया विभक्ति भी है। इस पूर्वोक्त दृष्टि से सहुँ शब्द परसर्ग के अन्तर्गत नहीं आता। संभवतः इसी कारण डॉ० तगारे ने परसर्गों में इसका उल्लेख नहीं किया है। किन्तु परवर्ती अपभ्रंश अवहट्ट में करण चिह बोधक परसर्ग का प्रयोग पाया जाता है-दूजने सउँ सबकाहु तूट (37/23) धिएँ सँकरे सेउँ सातु (21/31) उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्राकृत पैंगलम् में ‘एक सउ' (1,46-एकेन सम) संभुहि सउ (1,112-शंभुमारभ्य) सउ की व्युत्पत्ति सं०-समं से हुई है। ‘सउ' का प्रयोग संदेश रासक में करण कारक में पाया जाता है="गुरू विण एण सउ" (74 ब) बिरहसउ (79 अ), कंदप्प सउ (69 ए)। इसका 'सिउँ' रूप पश्चिमी राजस्थानी में मिलता है-मोटा नइ मोटा-सिउँ दोस। मुझ-सिउँ किसिउँ करइ ते दोस०=बड़ा बड़े से दोष (करता है), मुझसे वह कैसे दोष कर सकता है। पुरानी मैथिली में सञो, सँ आदि प्रयोग मिलता है-मृत्यु-सञो कल-कल करइतें अच्छ (मृत्यु के साथ झगड़ा कर रहा है, वर्णर० 41 अ7) इन्दु माधव सत्रे