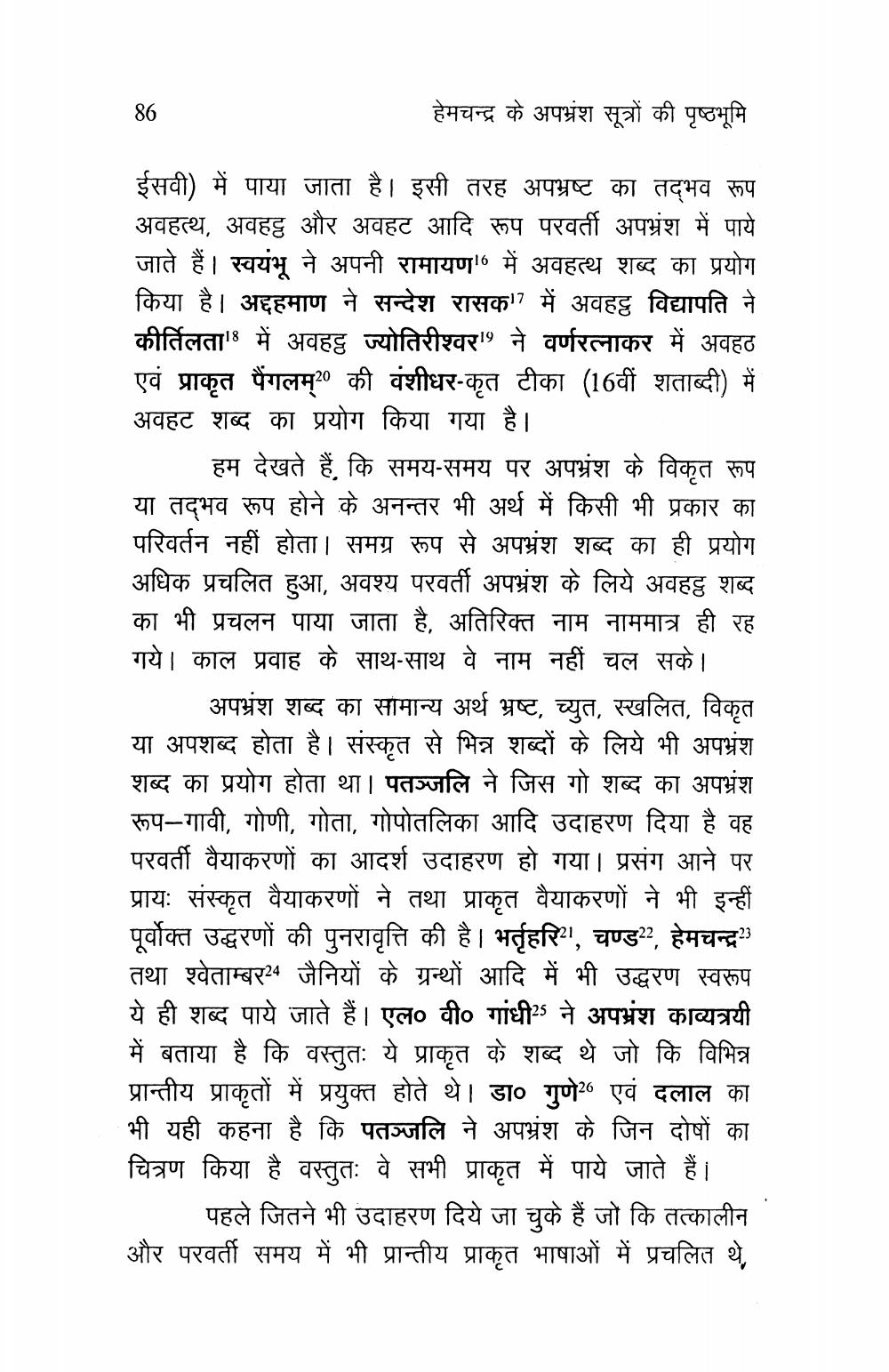________________
हेमचन्द्र के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि
ईसवी) में पाया जाता है। इसी तरह अपभ्रष्ट का तद्भव रूप अवहत्थ, अवहट्ट और अवहट आदि रूप परवर्ती अपभ्रंश में पाये जाते हैं। स्वयंभू ने अपनी रामायण में अवहत्थ शब्द का प्रयोग किया है। अद्दहमाण ने सन्देश रासक'7 में अवहट्ट विद्यापति ने कीर्तिलता' में अवहट्ठ ज्योतिरीश्वर ने वर्णरत्नाकर में अवहठ एवं प्राकृत पैंगलम्20 की वंशीधर-कृत टीका (16वीं शताब्दी) में अवहट शब्द का प्रयोग किया गया है।
हम देखते हैं, कि समय-समय पर अपभ्रंश के विकृत रूप या तद्भव रूप होने के अनन्तर भी अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। समग्र रूप से अपभ्रंश शब्द का ही प्रयोग अधिक प्रचलित हुआ, अवश्य परवर्ती अपभ्रंश के लिये अवहट्ठ शब्द का भी प्रचलन पाया जाता है, अतिरिक्त नाम नाममात्र ही रह गये। काल प्रवाह के साथ-साथ वे नाम नहीं चल सके।
अपभ्रंश शब्द का सामान्य अर्थ भ्रष्ट, च्युत, स्खलित, विकृत या अपशब्द होता है। संस्कृत से भिन्न शब्दों के लिये भी अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। पतञ्जलि ने जिस गो शब्द का अपभ्रंश रूप-गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि उदाहरण दिया है वह परवर्ती वैयाकरणों का आदर्श उदाहरण हो गया। प्रसंग आने पर प्रायः संस्कृत वैयाकरणों ने तथा प्राकृत वैयाकरणों ने भी इन्हीं पूर्वोक्त उद्धरणों की पुनरावृत्ति की है। भर्तृहरिण, चण्ड22, हेमचन्द्र तथा श्वेताम्बर24 जैनियों के ग्रन्थों आदि में भी उद्धरण स्वरूप ये ही शब्द पाये जाते हैं। एल० वी० गांधी25 ने अपभ्रंश काव्यत्रयी में बताया है कि वस्तुतः ये प्राकृत के शब्द थे जो कि विभिन्न प्रान्तीय प्राकृतों में प्रयुक्त होते थे। डा० गुणे26 एवं दलाल का भी यही कहना है कि पतञ्जलि ने अपभ्रंश के जिन दोषों का चित्रण किया है वस्तुतः वे सभी प्राकृत में पाये जाते हैं।
पहले जितने भी उदाहरण दिये जा चुके हैं जो कि तत्कालीन और परवर्ती समय में भी प्रान्तीय प्राकृत भाषाओं में प्रचलित थे,