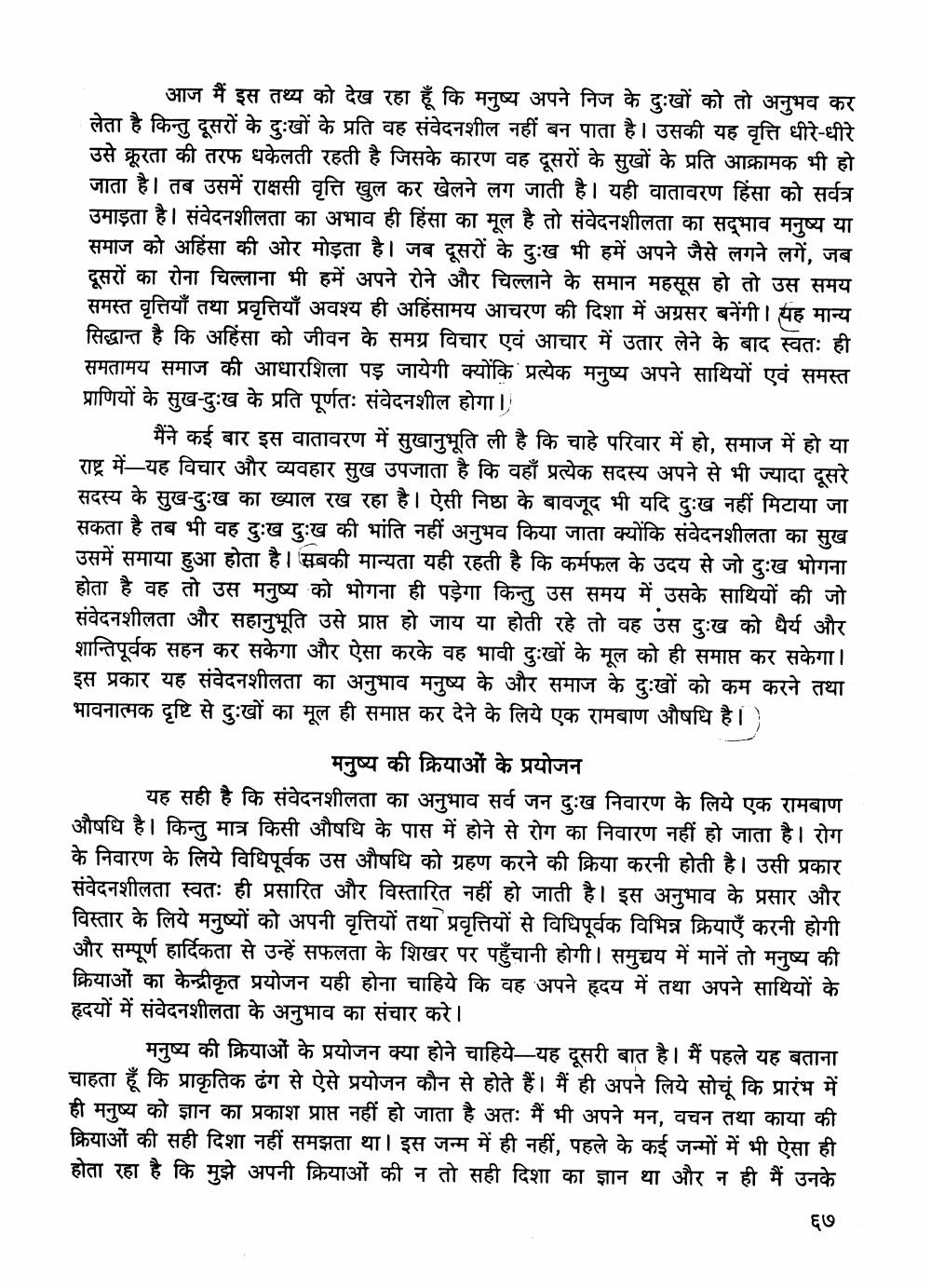________________
आज मैं इस तथ्य को देख रहा हूँ कि मनुष्य अपने निज के दुःखों को तो अनुभव कर ता है किन्तु दूसरों के दुःखों के प्रति वह संवेदनशील नहीं बन पाता है । उसकी यह वृत्ति धीरे-धीरे उसे क्रूरता की तरफ धकेलती रहती है जिसके कारण वह दूसरों के सुखों के प्रति आक्रामक भी हो जाता है। तब उसमें राक्षसी वृत्ति खुल कर खेलने लग जाती है। यही वातावरण हिंसा को सर्वत्र उमाड़ता है। संवेदनशीलता का अभाव ही हिंसा का मूल है तो संवेदनशीलता का सद्भाव मनुष्य या समाज को अहिंसा की ओर मोड़ता है। जब दूसरों के दुःख भी हमें अपने जैसे लगने लगें, जब दूसरों का रोना चिल्लाना भी हमें अपने रोने और चिल्लाने के समान महसूस हो तो उस समय समस्त वृत्तियाँ तथा प्रवृत्तियाँ अवश्य ही अहिंसामय आचरण की दिशा में अग्रसर बनेंगी। यह मान्य सिद्धान्त है कि अहिंसा को जीवन के समग्र विचार एवं आचार में उतार लेने के बाद स्वतः ही समतामय समाज की आधारशिला पड़ जायेगी क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने साथियों एवं समस्त प्राणियों के सुख-दुःख के प्रति पूर्णतः संवेदनशील होगा ।
मैंने कई बार इस वातावरण में सुखानुभूति ली है कि चाहे परिवार में हो, समाज में हो या राष्ट्र में - यह विचार और व्यवहार सुख उपजाता है कि वहाँ प्रत्येक सदस्य अपने से भी ज्यादा दूसरे सदस्य के सुख-दुःख का ख्याल रख रहा है। ऐसी निष्ठा के बावजूद भी यदि दुःख नहीं मिटाया जा सकता है तब भी वह दुःख दुःख की भांति नहीं अनुभव किया जाता क्योंकि संवेदनशीलता का सुख उसमें समाया हुआ होता है। सबकी मान्यता यही रहती है कि कर्मफल के उदय से जो दुःख भोगना होता है वह तो उस मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा किन्तु उस समय में उसके साथियों की जो संवेदनशीलता और सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाय या होती रहे तो वह उस दुःख को धैर्य और शान्तिपूर्वक सहन कर सकेगा और ऐसा करके वह भावी दुःखों के मूल को ही समाप्त कर सकेगा । इस प्रकार यह संवेदनशीलता का अनुभाव मनुष्य के और समाज के दुःखों को कम करने तथा भावनात्मक दृष्टि से दुःखों का मूल ही समाप्त कर देने के लिये एक रामबाण औषधि है ।
मनुष्य की क्रियाओं के प्रयोजन
यह सही है कि संवेदनशीलता का अनुभाव सर्व जन दुःख निवारण के लिये एक रामबाण औषधि है । किन्तु मात्र किसी औषधि के पास में होने से रोग का निवारण नहीं हो जाता है। रोग के निवारण के लिये विधिपूर्वक उस औषधि को ग्रहण करने की क्रिया करनी होती है । उसी प्रकार संवेदनशीलता स्वतः ही प्रसारित और विस्तारित नहीं हो जाती है । इस अनुभाव के प्रसार और विस्तार के लिये मनुष्यों को अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों से विधिपूर्वक विभिन्न क्रियाएँ करनी होगी और सम्पूर्ण हार्दिकता से उन्हें सफलता के शिखर पर पहुँचानी होगी । समुच्चय में मानें तो मनुष्य की क्रियाओं का केन्द्रीकृत प्रयोजन यही होना चाहिये कि वह अपने हृदय तथा अपने साथियों के हृदयों में संवेदनशीलता के अनुभाव का संचार करे ।
मनुष्य की क्रियाओं के प्रयोजन क्या होने चाहिये - यह दूसरी बात है । मैं पहले यह बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक ढंग से ऐसे प्रयोजन कौन से होते हैं। मैं ही अपने लिये सोचूं कि प्रारंभ में ही मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हो जाता है अतः मैं भी अपने मन, वचन तथा काया की क्रियाओं की सही दिशा नहीं समझता था । इस जन्म में ही नहीं, पहले के कई जन्मों में भी ऐसा ही होता रहा है कि मुझे अपनी क्रियाओं की न तो सही दिशा का ज्ञान
था और न ही मैं उनके
६७