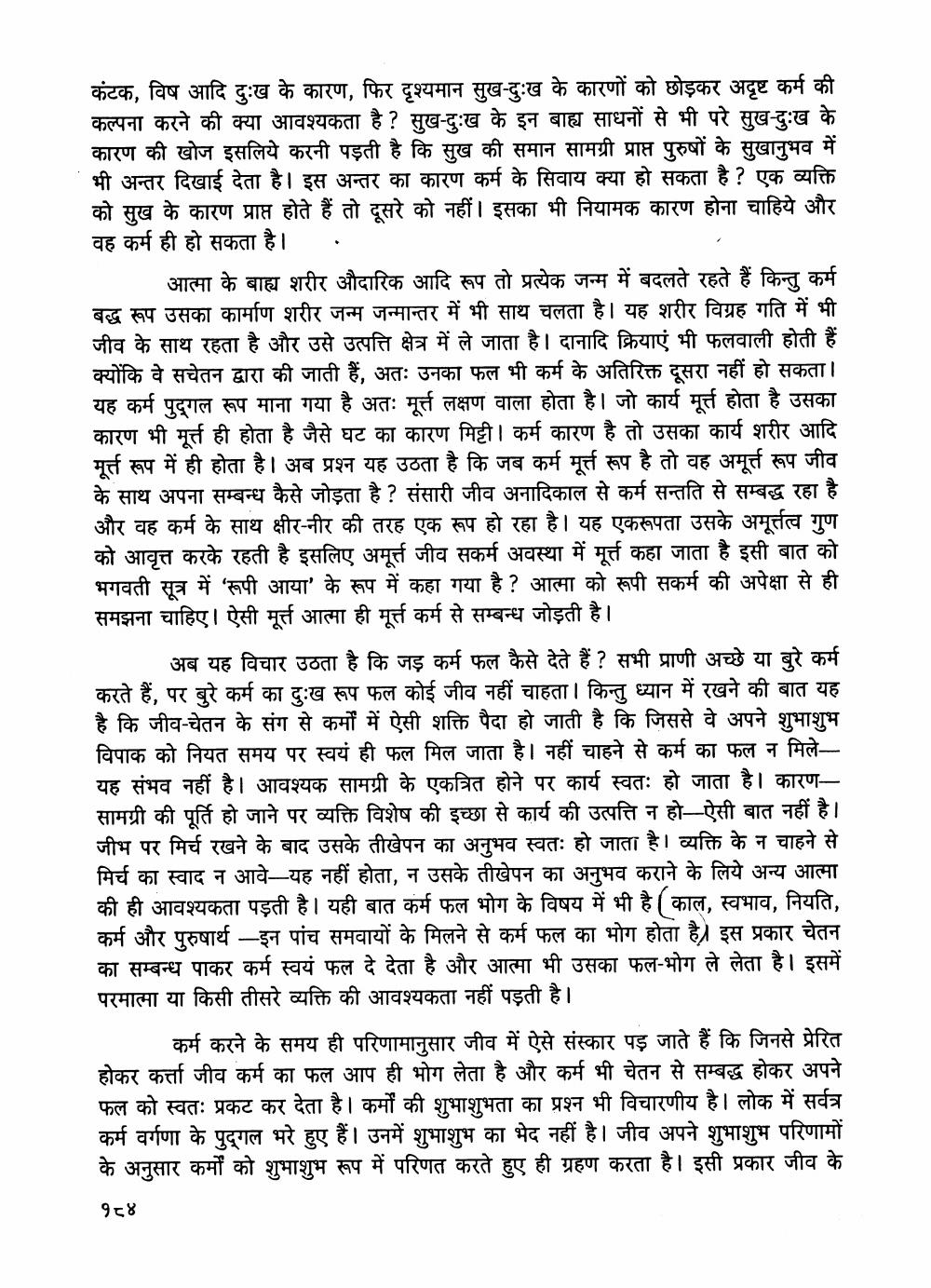________________
कंटक, विष आदि दुःख के कारण, फिर दृश्यमान सुख - दुःख के कारणों को छोड़कर अदृष्ट कर्म की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? सुख-दुःख के इन बाह्य साधनों से भी परे सुख-दुःख के कारण की खोज इसलिये करनी पड़ती है कि सुख की समान सामग्री प्राप्त पुरुषों के सुखानुभव में भी अन्तर दिखाई देता है। इस अन्तर का कारण कर्म के सिवाय क्या हो सकता है ? एक व्यक्ति को सुख के कारण प्राप्त होते हैं तो दूसरे को नहीं। इसका भी नियामक कारण होना चाहिये और वह कर्म ही हो सकता है।
आत्मा के बाह्य शरीर औदारिक आदि रूप तो प्रत्येक जन्म में बदलते रहते हैं किन्तु कर्म बद्ध रूप उसका कार्माण शरीर जन्म जन्मान्तर में भी साथ चलता है। यह शरीर विग्रह गति में भी जीव के साथ रहता है और उसे उत्पत्ति क्षेत्र में ले जाता है। दानादि क्रियाएं भी फलवाली होती हैं क्योंकि वे सचेतन द्वारा की जाती हैं, अतः उनका फल भी कर्म के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता । यह कर्म पुद्गल रूप माना गया है अतः मूर्त्त लक्षण वाला होता है। जो कार्य मूर्त्त होता है उसका कारण भी मूर्त ही होता है जैसे घट का कारण मिट्टी । कर्म कारण है तो उसका कार्य शरीर आदि मूर्त रूप में ही होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कर्म मूर्त रूप है तो वह अमूर्त रूप जीव के साथ अपना सम्बन्ध कैसे जोड़ता है ? संसारी जीव अनादिकाल से कर्म सन्तति से सम्बद्ध रहा है और वह कर्म के साथ क्षीर-नीर की तरह एक रूप हो रहा है। यह एकरूपता उसके अमूर्त्तत्व गुण को आवृत्त करके रहती है इसलिए अमूर्त जीव सकर्म अवस्था में मूर्त कहा जाता है इसी बात को भगवती सूत्र में 'रूपी आया' के रूप में कहा गया है ? आत्मा को रूपी सकर्म की अपेक्षा से ही समझना चाहिए। ऐसी मूर्त आत्मा ही मूर्त्त कर्म से सम्बन्ध जोड़ती है ।
अब यह विचार उठता है कि जड़ कर्म फल कैसे देते हैं ? सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, पर बुरे कर्म का दुःख रूप फल कोई जीव नहीं चाहता । किन्तु ध्यान में रखने की बात यह है कि जीव-चेतन के संग से कर्मों में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वे अपने शुभाशुभ विपाक को नियत समय पर स्वयं ही फल मिल जाता है। नहीं चाहने से कर्म का फल न मिले— यह संभव नहीं है। आवश्यक सामग्री के एकत्रित होने पर कार्य स्वतः हो जाता है। कारणसामग्री की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति विशेष की इच्छा से कार्य की उत्पत्ति न हो-ऐसी बात नहीं है । जीभ पर मिर्च रखने के बाद उसके तीखेपन का अनुभव स्वतः हो जाता है। व्यक्ति के न चाहने से मिर्च का स्वाद न आवे - यह नहीं होता, न उसके तीखेपन का अनुभव कराने के लिये अन्य आत्मा की ही आवश्यकता पड़ती है। यही बात कर्म फल भोग के विषय में भी है (काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ – इन पांच समवायों के मिलने से कर्म फल का भोग होता है। इस प्रकार चेतन का सम्बन्ध पाकर कर्म स्वयं फल दे देता है और आत्मा भी उसका फल भोग ले लेता है। इसमें परमात्मा या किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।
कर्म करने के समय ही परिणामानुसार जीव में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कर्त्ता जीव कर्म का फल आप ही भोग लेता है और कर्म भी चेतन से सम्बद्ध होकर अपने फल को स्वतः प्रकट कर देता है। कर्मों की शुभाशुभता का प्रश्न भी विचारणीय है । लोक में सर्वत्र कर्म वर्गणा के पुद्गल भरे हुए हैं । उनमें शुभाशुभ का भेद नहीं है। जीव अपने शुभाशुभ परिणामों के अनुसार कर्मों को शुभाशुभ रूप में परिणत करते हुए ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार जीव के
१८४