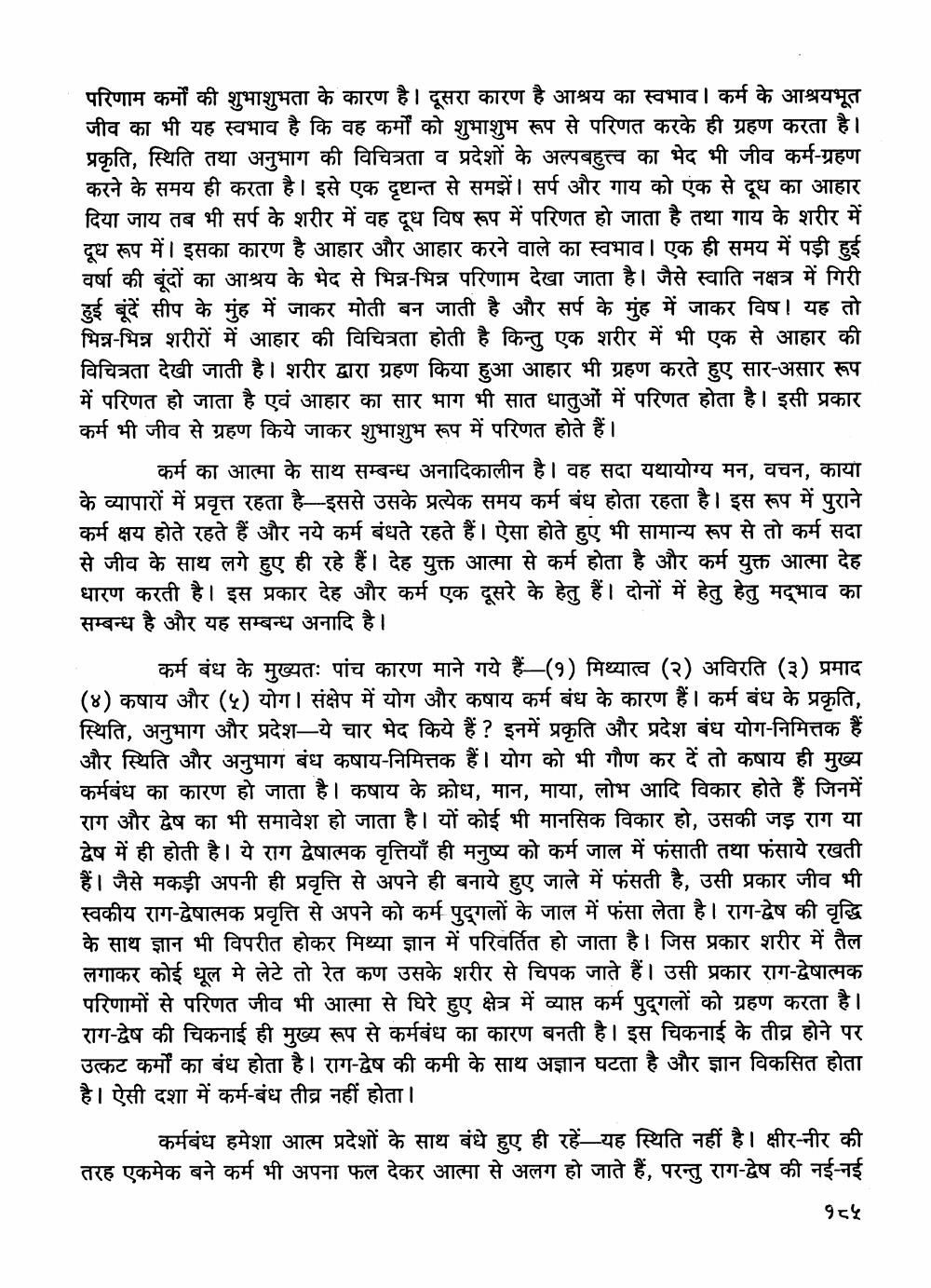________________
परिणाम कर्मों की शभाशभता के कारण है। दसरा कारण है आश्रय का स्वभाव । कर्म के आश्रयभत
का भी यह स्वभाव है कि वह कर्मों को शभाशभ रूप से परिणत करके ही ग्रहण करता है। प्रकृति, स्थिति तथा अनुभाग की विचित्रता व प्रदेशों के अल्पबहुत्त्व का भेद भी जीव कर्म-ग्रहण करने के समय ही करता है। इसे एक दृष्टान्त से समझें। सर्प और गाय को एक से दूध का आहार दिया जाय तब भी सर्प के शरीर में वह दूध विष रूप में परिणत हो जाता है तथा गाय के शरीर में दूध रूप में। इसका कारण है आहार और आहार करने वाले का स्वभाव । एक ही समय में पड़ी हुई वर्षा की बूंदों का आश्रय के भेद से भिन्न-भिन्न परिणाम देखा जाता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंदें सीप के मुंह में जाकर मोती बन जाती है और सर्प के मुंह में जाकर विष । यह तो भिन्न-भिन्न शरीरों में आहार की विचित्रता होती है किन्तु एक शरीर में भी एक से आहार की विचित्रता देखी जाती है। शरीर द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार भी ग्रहण करते हुए सार-असार रूप में परिणत हो जाता है एवं आहार का सार भाग भी सात धातुओं में परिणत होता है। इसी प्रकार कर्म भी जीव से ग्रहण किये जाकर शुभाशुभ रूप में परिणत होते हैं।
कर्म का आत्मा के साथ सम्बन्ध अनादिकालीन है। वह सदा यथायोग्य मन, वचन, काया के व्यापारों में प्रवृत्त रहता है—इससे उसके प्रत्येक समय कर्म बंध होता रहता है। इस रूप में पुराने कर्म क्षय होते रहते हैं और नये कर्म बंधते रहते हैं। ऐसा होते हुए भी सामान्य रूप से तो कर्म सदा से जीव के साथ लगे हुए ही रहे हैं। देह युक्त आत्मा से कर्म होता है और कर्म युक्त आत्मा देह धारण करती है। इस प्रकार देह और कर्म एक दूसरे के हेतु हैं। दोनों में हेतु हेतु मद्भाव का सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध अनादि है।
कर्म बंध के मुख्यतः पांच कारण माने गये हैं (१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय और (५) योग । संक्षेप में योग और कषाय कर्म बंध के कारण हैं। कर्म बंध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश—ये चार भेद किये हैं? इनमें प्रकृति और प्रदेश बंध योग-निमित्तक हैं
और स्थिति और अनुभाग बंध कषाय-निमित्तक हैं। योग को भी गौण कर दें तो कषाय ही मुख्य कर्मबंध का कारण हो जाता है। कषाय के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार होते हैं जिनमें राग और द्वेष का भी समावेश हो जाता है। यों कोई भी मानसिक विकार हो, उसकी जड़ राग या द्वेष में ही होती है। ये राग द्वेषात्मक वृत्तियाँ ही मनुष्य को कर्म जाल में फंसाती तथा फंसाये रखती हैं। जैसे मकड़ी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने ही बनाये हुए जाले में फंसती है, उसी प्रकार जीव भी स्वकीय राग-द्वेषात्मक प्रवृत्ति से अपने को कर्म पुद्गलों के जाल में फंसा लेता है। राग-द्वेष की वृद्धि के साथ ज्ञान भी विपरीत होकर मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार शरीर में तैल लगाकर कोई धूल मे लेटे तो रेत कण उसके शरीर से चिपक जाते हैं। उसी प्रकार राग-द्वेषात्मक परिणामों से परिणत जीव भी आत्मा से घिरे हुए क्षेत्र में व्याप्त कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है। राग-द्वेष की चिकनाई ही मुख्य रूप से कर्मबंध का कारण बनती है। इस चिकनाई के तीव्र होने पर उत्कट कर्मों का बंध होता है। राग-द्वेष की कमी के साथ अज्ञान घटता है और ज्ञान विकसित होता है। ऐसी दशा में कर्म-बंध तीव्र नहीं होता।
कर्मबंध हमेशा आत्म प्रदेशों के साथ बंधे हुए ही रहें यह स्थिति नहीं है। क्षीर-नीर की तरह एकमेक बने कर्म भी अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं, परन्तु राग-द्वेष की नई-नई
१८५