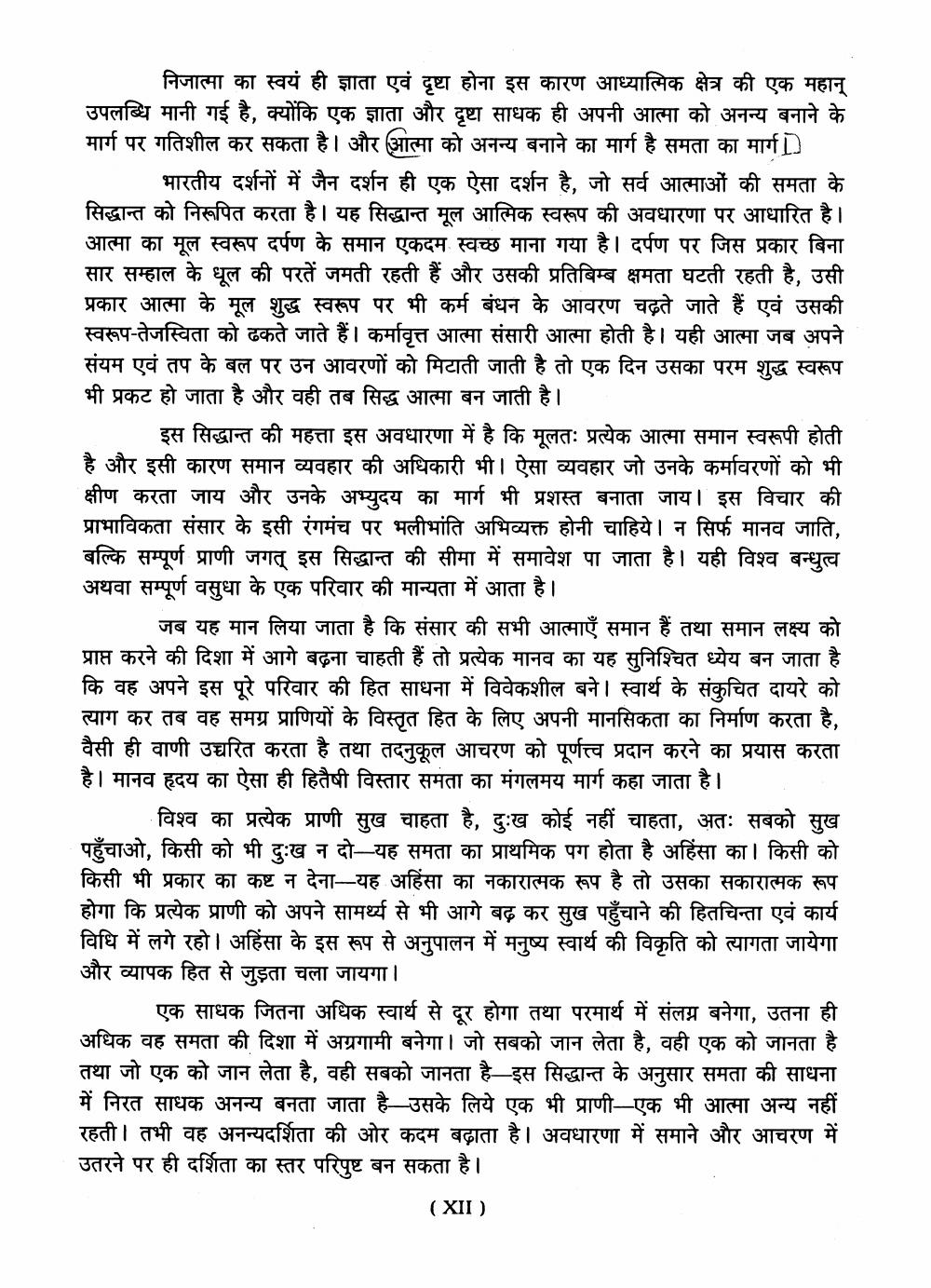________________
निजात्मा का स्वयं ही ज्ञाता एवं दृष्टा होना इस कारण आध्यात्मिक क्षेत्र की एक महान् उपलब्धि मानी गई है, क्योंकि एक ज्ञाता और दृष्टा साधक ही अपनी आत्मा को अनन्य बनाने के मार्ग पर गतिशील कर सकता है। और आत्मा को अनन्य बनाने का मार्ग है समता का मार्ग
भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है, जो सर्व आत्माओं की समता के सिद्धान्त को निरूपित करता है। यह सिद्धान्त मूल आत्मिक स्वरूप की अवधारणा पर आधारित है। आत्मा का मूल स्वरूप दर्पण के समान एकदम स्वच्छ माना गया है। दर्पण पर जिस प्रकार बिना सार सम्हाल के धूल की परतें जमती रहती हैं और उसकी प्रतिबिम्ब क्षमता घटती रहती है, उसी प्रकार आत्मा के मूल शुद्ध स्वरूप पर भी कर्म बंधन के आवरण चढ़ते जाते हैं एवं उसकी स्वरूप-तेजस्विता को ढकते जाते हैं। कर्मावृत्त आत्मा संसारी आत्मा होती है। यही आत्मा जब अपने संयम एवं तप के बल पर उन आवरणों को मिटाती जाती है तो एक दिन उसका परम शुद्ध स्वरूप भी प्रकट हो जाता है और वही तब सिद्ध आत्मा बन जाती है।
इस सिद्धान्त की महत्ता इस अवधारणा में है कि मूलतः प्रत्येक आत्मा समान स्वरूपी होती है और इसी कारण समान व्यवहार की अधिकारी भी। ऐसा व्यवहार जो उनके कर्मावरणों को भी क्षीण करता जाय और उनके अभ्युदय का मार्ग भी प्रशस्त बनाता जाय। इस विचार की प्राभाविकता संसार के इसी रंगमंच पर भलीभांति अभिव्यक्त होनी चाहिये। न सिर्फ मानव जाति, बल्कि सम्पूर्ण प्राणी जगत् इस सिद्धान्त की सीमा में समावेश पा जाता है। यही विश्व बन्धुत्व अथवा सम्पूर्ण वसुधा के एक परिवार की मान्यता में आता है।
जब यह मान लिया जाता है कि संसार की सभी आत्माएँ समान हैं तथा समान लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं तो प्रत्येक मानव का यह सुनिश्चित ध्येय बन जाता है कि वह अपने इस पूरे परिवार की हित साधना में विवेकशील बने । स्वार्थ के संकुचित दायरे को त्याग कर तब वह समग्र प्राणियों के विस्तृत हित के लिए अपनी मानसिकता का निर्माण करता है, वैसी ही वाणी उच्चरित करता है तथा तदनुकूल आचरण को पूर्णत्त्व प्रदान करने का प्रयास करता है। मानव हृदय का ऐसा ही हितैषी विस्तार समता का मंगलमय मार्ग कहा जाता है।
विश्व का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुःख कोई नहीं चाहता, अतः सबको सुख पहुँचाओ, किसी को भी दुःख न दो—यह समता का प्राथमिक पग होता है अहिंसा का। किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना—यह अहिंसा का नकारात्मक रूप है तो उसका सकारात्मक रूप होगा कि प्रत्येक प्राणी को अपने सामर्थ्य से भी आगे बढ़ कर सुख पहुँचाने की हितचिन्ता एवं कार्य विधि में लगे रहो। अहिंसा के इस रूप से अनुपालन में मनुष्य स्वार्थ की विकति को त्यागता जायेगा और व्यापक हित से जुड़ता चला जायगा।
एक साधक जितना अधिक स्वार्थ से दूर होगा तथा परमार्थ में संलग्न बनेगा, उतना ही अधिक वह समता की दिशा में अग्रगामी बनेगा। जो सबको जान लेता है, वही एक को जानता है तथा जो एक को जान लेता है, वही सबको जानता है—इस सिद्धान्त के अनुसार समता की साधना में निरत साधक अनन्य बनता जाता है उसके लिये एक भी प्राणी—एक भी आत्मा अन्य नहीं रहती। तभी वह अनन्यदर्शिता की ओर कदम बढ़ाता है। अवधारणा में समाने और आचरण में उतरने पर ही दर्शिता का स्तर परिपुष्ट बन सकता है।
(XII)