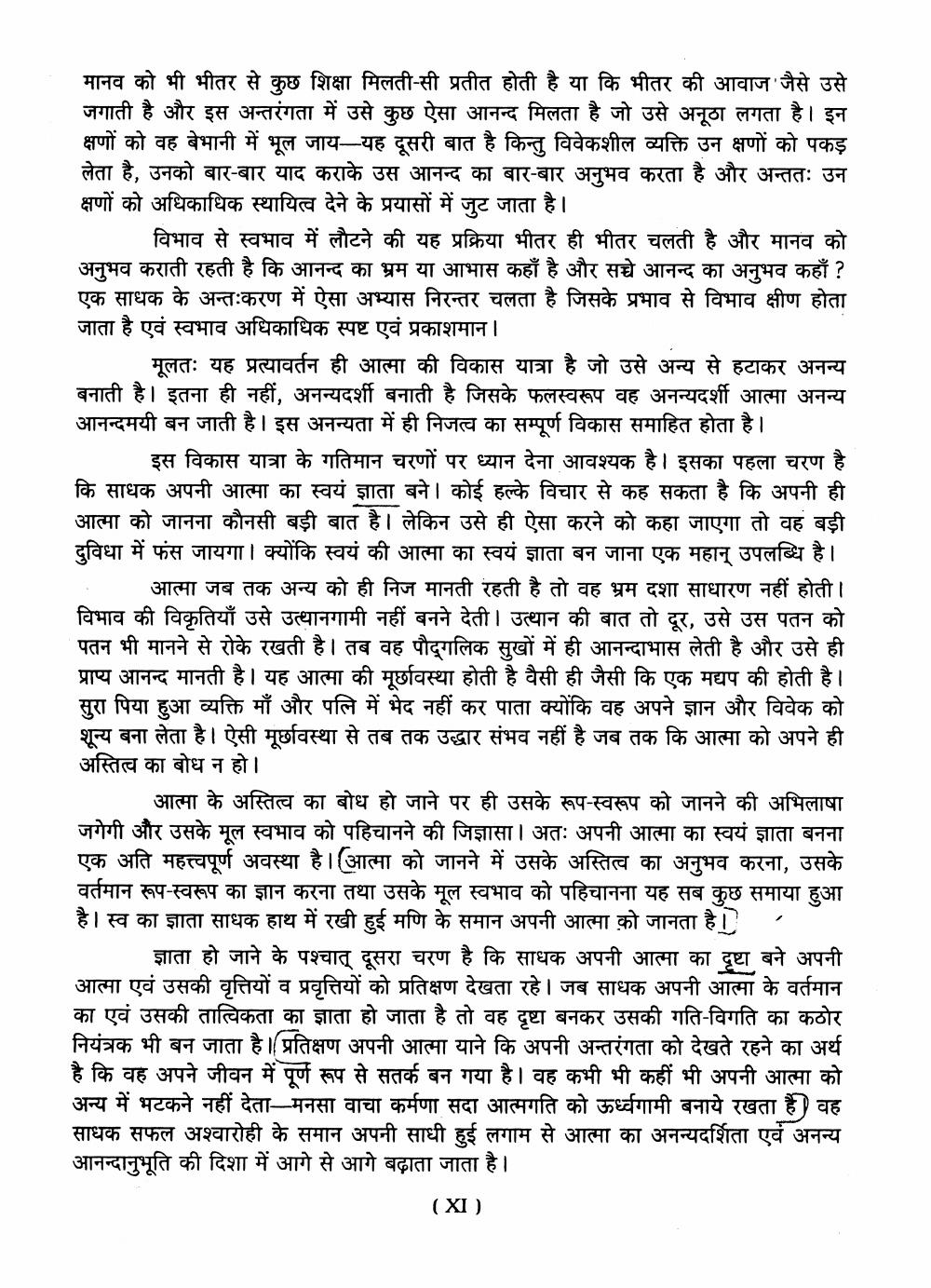________________
मानव को भी भीतर से कुछ शिक्षा मिलती-सी प्रतीत होती है या कि भीतर की आवाज जैसे उसे जगाती है और इस अन्तरंगता में उसे कुछ ऐसा आनन्द मिलता है जो उसे अनूठा लगता है। इन क्षणों को वह बेभानी में भूल जाय - यह दूसरी बात है किन्तु विवेकशील व्यक्ति उन क्षणों को पकड़ लेता है, उनको बार-बार याद कराके उस आनन्द का बार-बार अनुभव करता है और अन्ततः उन क्षणों को अधिकाधिक स्थायित्व देने के प्रयासों में जुट जाता है।
विभाव से स्वभाव में लौटने की यह प्रक्रिया भीतर ही भीतर चलती है और मानव को अनुभव कराती रहती है कि आनन्द का भ्रम या आभास कहाँ है और सच्चे आनन्द का अनुभव कहाँ ? एक साधक के अन्तःकरण में ऐसा अभ्यास निरन्तर चलता है जिसके प्रभाव से विभाव क्षीण होता जाता है एवं स्वभाव अधिकाधिक स्पष्ट एवं प्रकाशमान ।
मूलतः यह प्रत्यावर्तन ही आत्मा की विकास यात्रा है जो उसे अन्य से हटाकर अनन्य बनाती है। इतना ही नहीं, अनन्यदर्शी बनाती है जिसके फलस्वरूप वह अनन्यदर्शी आत्मा अनन्य आनन्दमयी बन जाती है। इस अनन्यता में ही निजत्व का सम्पूर्ण विकास समाहित होता है ।
इस विकास यात्रा के गतिमान चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका पहला चरण है कि साधक अपनी आत्मा का स्वयं ज्ञाता बने । कोई हल्के विचार से कह सकता है कि अपनी ही आत्मा को जानना कौनसी बड़ी बात है । लेकिन उसे ही ऐसा करने को कहा जाएगा तो वह बड़ी दुविधा में फंस जायगा। क्योंकि स्वयं की आत्मा का स्वयं ज्ञाता बन जाना एक महान् उपलब्धि है । आत्मा जब तक अन्य को ही निज मानती रहती है तो वह भ्रम दशा साधारण नहीं होती । विभाव की विकृतियाँ उसे उत्थानगामी नहीं बनने देती । उत्थान की बात तो दूर, उसे उस पतन को पतन भी मानने से रोके रखती है। तब वह पौद्गलिक सुखों में ही आनन्दाभास लेती है और उसे ही प्राप्य आनन्द मानती है। यह आत्मा की मूर्छावस्था होती है वैसी ही जैसी कि एक मद्यप की होती है। सुरा पिया हुआ व्यक्ति माँ और पलि में भेद नहीं कर पाता क्योंकि वह अपने ज्ञान और विवेक को शून्य बना लेता है। ऐसी मूर्छावस्था से तब तक उद्धार संभव नहीं है जब तक कि आत्मा को अपने ही अस्तित्व का बोध न हो ।
आत्मा के अस्तित्व का बोध हो जाने पर ही उसके रूप-स्वरूप को जानने की अभिलाषा जगेगी और उसके मूल स्वभाव को पहिचानने की जिज्ञासा । अतः अपनी आत्मा का स्वयं ज्ञाता बनना एक अति महत्त्वपूर्ण अवस्था है । (आत्मा को जानने में उसके अस्तित्व का अनुभव करना, उसके वर्तमान रूप-स्वरूप का ज्ञान करना तथा उसके मूल स्वभाव को पहिचानना यह सब कुछ समाया हुआ है । स्व का ज्ञाता साधक हाथ में रखी हुई मणि के समान अपनी आत्मा को जानता है।
ज्ञाता हो जाने के पश्चात् दूसरा चरण है कि साधक अपनी आत्मा का दृष्टा बने अपनी आत्मा एवं उसकी वृत्तियों व प्रवृत्तियों को प्रतिक्षण देखता रहे। जब साधक अपनी आत्मा के वर्तमान का एवं उसकी तात्विकता का ज्ञाता हो जाता है तो वह दृष्टा बनकर उसकी गति-विगति का कठोर नियंत्रक भी बन जाता है । प्रतिक्षण अपनी आत्मा याने कि अपनी अन्तरंगता को देखते रहने का अर्थ है कि वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से सतर्क बन गया है। वह कभी भी कहीं भी अपनी आत्मा को अन्य में भटकने नहीं देता - मनसा वाचा कर्मणा सदा आत्मगति को ऊर्ध्वगामी बनाये रखता है। वह साधक सफल अश्वारोही के समान अपनी साधी हुई लगाम से आत्मा का अनन्यदर्शिता एवं अनन्य आनन्दानुभूति की दिशा में आगे से आगे बढ़ाता जाता है।
(XI)