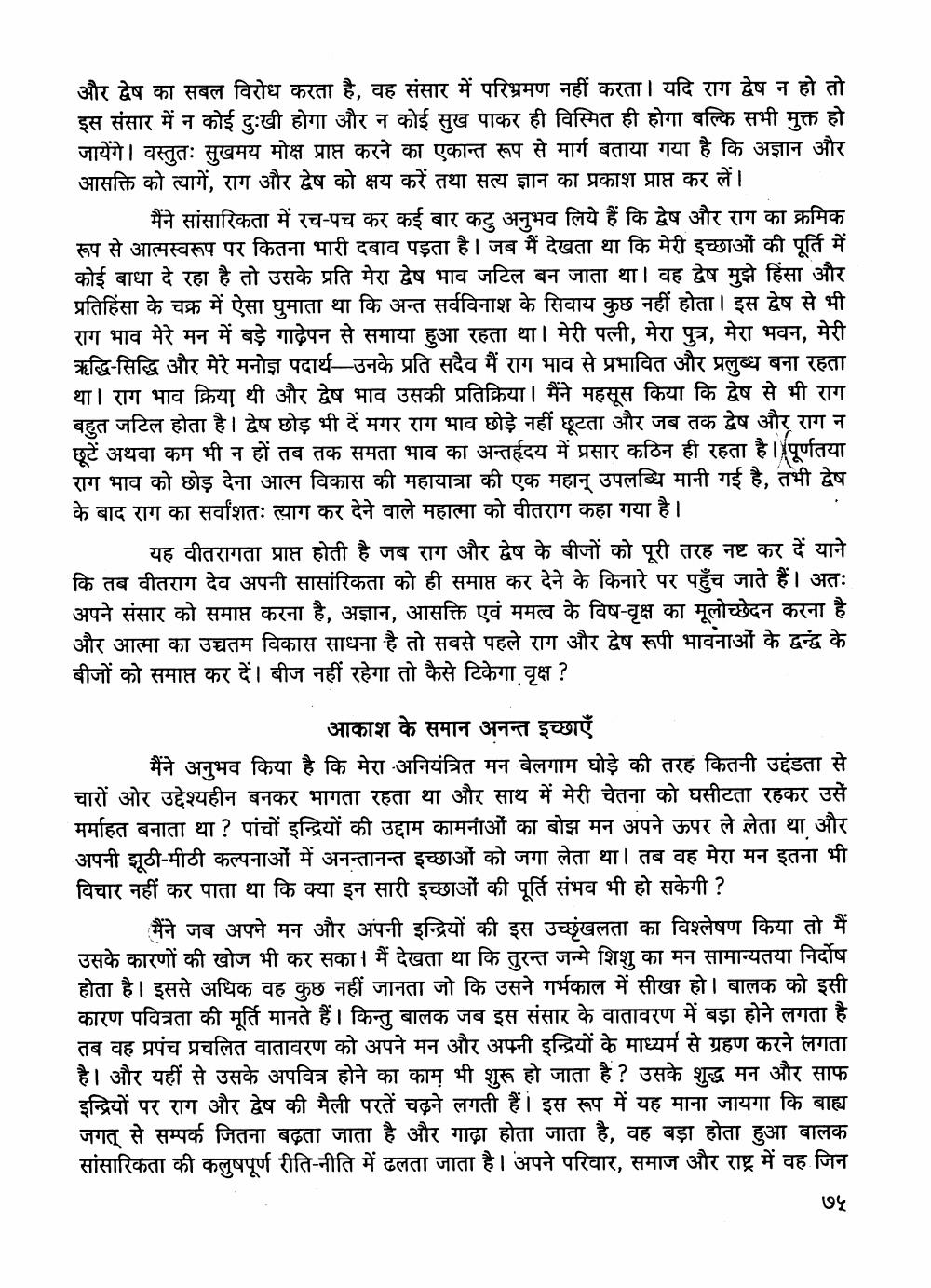________________
और द्वेष का सबल विरोध करता है, वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता। यदि राग द्वेष न हो तो इस संसार में न कोई दुःखी होगा और न कोई सुख पाकर ही विस्मित ही होगा बल्कि सभी मुक्त हो जायेंगे । वस्तुतः सुखमय मोक्ष प्राप्त करने का एकान्त रूप से मार्ग बताया गया है कि अज्ञान और आसक्ति को त्यागें, राग और द्वेष को क्षय करें तथा सत्य ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लें ।
मैंने सांसारिकता में रच-पच कर कई बार कटु अनुभव लिये हैं कि द्वेष और राग का क्रमिक रूप से आत्मस्वरूप पर कितना भारी दबाव पड़ता है। जब मैं देखता था कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति में कोई बाधा दे रहा है तो उसके प्रति मेरा द्वेष भाव जटिल बन जाता था। वह द्वेष मुझे हिंसा और प्रतिहिंसा के चक्र में ऐसा घुमाता था कि अन्त सर्वविनाश के सिवाय कुछ नहीं होता । इस द्वेष से भी राग भाव मेरे मन में बड़े गाढ़ेपन से समाया हुआ रहता था। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा भवन, मेरी ऋद्धि-सिद्धि और मेरे मनोज्ञ पदार्थ – उनके प्रति सदैव मैं राग भाव से प्रभावित और प्रलुब्ध बना रहता था। राग भाव क्रिया थी और द्वेष भाव उसकी प्रतिक्रिया । मैंने महसूस किया कि द्वेष से भी राग बहुत जटिल होता है । द्वेष छोड़ भी दें मगर राग भाव छोड़े नहीं छूटता और जब तक द्वेष और राग न छूटें अथवा कम भी न हों तब तक समता भाव का अन्तर्हृदय में प्रसार कठिन ही रहता है। पूर्णतया राग भाव को छोड़ देना आत्म विकास की महायात्रा की एक महान् उपलब्धि मानी गई है, तभी द्वेष के बाद राग का सर्वांशतः त्याग कर देने वाले महात्मा को वीतराग कहा गया है।
यह वीतरागता प्राप्त होती है जब राग और द्वेष के बीजों को पूरी तरह नष्ट कर दें याने कि तब वीतराग देव अपनी सासांरिकता को ही समाप्त कर देने के किनारे पर पहुँच जाते हैं । अतः अपने संसार को समाप्त करना है, अज्ञान, आसक्ति एवं ममत्व के विषवृक्ष का मूलोच्छेदन करना है और आत्मा का उच्चतम विकास साधना है तो सबसे पहले राग और द्वेष रूपी भावनाओं के द्वन्द्व के बीजों को समाप्त कर दें। बीज नहीं रहेगा तो कैसे टिकेगा वृक्ष ?
आकाश के समान अनन्त इच्छाएँ
मैंने अनुभव किया है कि मेरा अनियंत्रित मन बेलगाम घोड़े की तरह कितनी उद्दंडता से चारों ओर उद्देश्यहीन बनकर भागता रहता था और साथ में मेरी चेतना को घसीटता रहकर उसे मर्माहत बनाता था ? पांचों इन्द्रियों की उद्दाम कामनाओं का बोझ मन अपने ऊपर ले लेता था और अपनी झूठी-मीठी कल्पनाओं में अनन्तानन्त इच्छाओं को जगा लेता था। तब वह मेरा मन इतना भी विचार नहीं कर पाता था कि क्या इन सारी इच्छाओं की पूर्ति संभव भी हो सकेगी ?
मैंने जब अपने मन और अपनी इन्द्रियों की इस उच्छृंखलता का विश्लेषण किया तो मैं उसके कारणों की खोज भी कर सका। मैं देखता था कि तुरन्त जन्मे शिशु का मन सामान्यतया निर्दोष होता है। इससे अधिक वह कुछ नहीं जानता जो कि उसने गर्भकाल में सीखा हो। बालक को इसी कारण पवित्रता की मूर्ति मानते हैं । किन्तु बालक जब इस संसार के वातावरण में बड़ा होने लगता है तब वह प्रपंच प्रचलित वातावरण को अपने मन और अपनी इन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण करने लगता है। और यहीं से उसके अपवित्र होने का काम भी शुरू हो जाता है ? उसके शुद्ध मन और साफ इन्द्रियों पर राग और द्वेष की मैली परतें चढ़ने लगती हैं। इस रूप में यह माना जायगा कि बाह्य जगत् से सम्पर्क जितना बढ़ता जाता है और गाढ़ा होता जाता है, वह बड़ा होता हुआ बालक सांसारिकता की कलुषपूर्ण रीति-नीति में ढलता जाता है। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र में वह जिन
७५