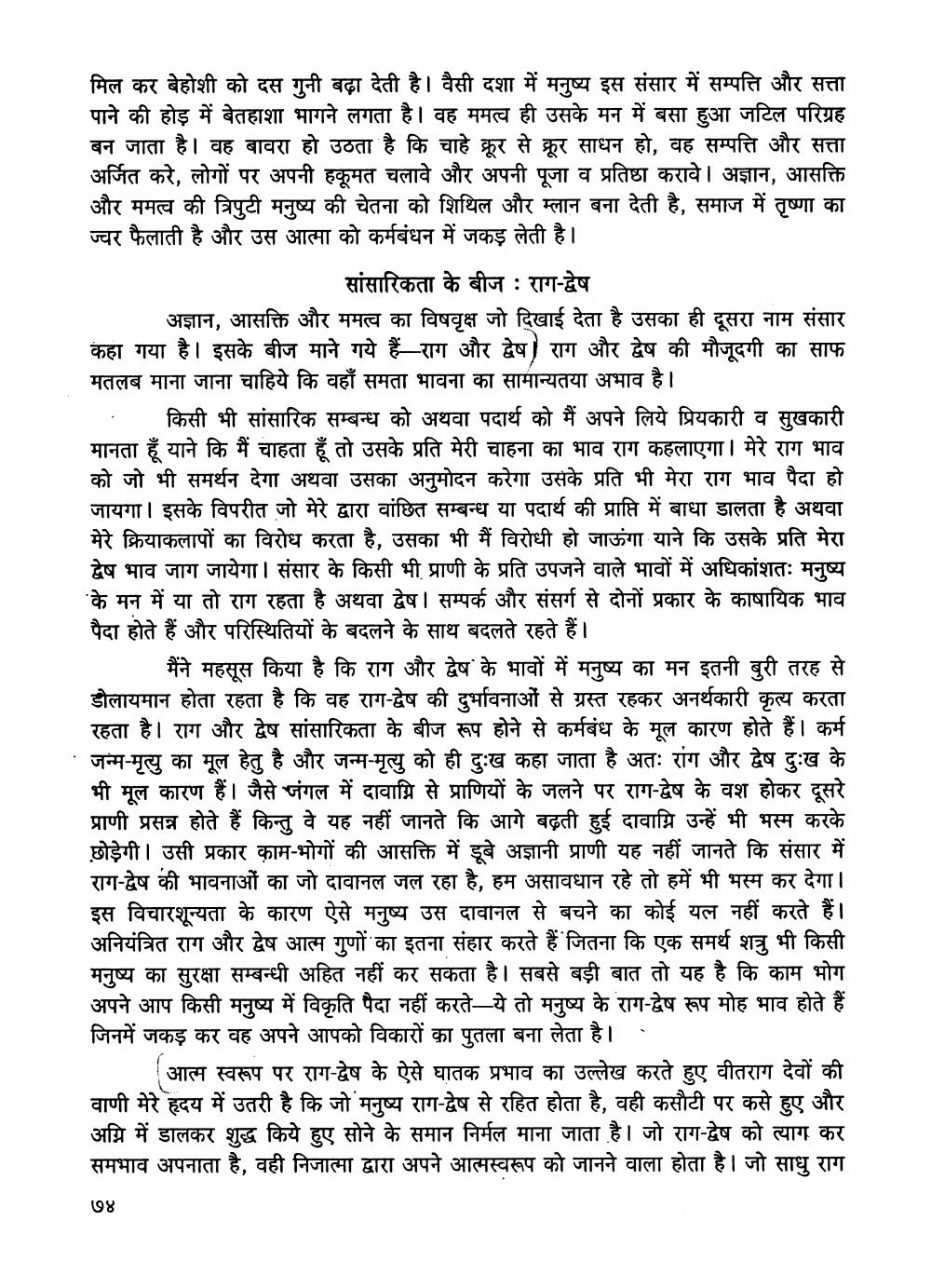________________
मिल कर बेहोशी को दस गुनी बढ़ा देती है। वैसी दशा में मनुष्य इस संसार में सम्पत्ति और सत्ता पाने की होड़ में बेतहाशा भागने लगता है। वह ममत्व ही उसके मन में बसा हुआ जटिल परिग्रह बन जाता है। वह बावरा हो उठता है कि चाहे क्रूर से क्रूर साधन हो, वह सम्पत्ति और सत्ता अर्जित करे, लोगों पर अपनी हकूमत चलावे और अपनी पूजा व प्रतिष्ठा करावे। अज्ञान, आसक्ति और ममत्व की त्रिपुटी मनुष्य की चेतना को शिथिल और म्लान बना देती है, समाज में तृष्णा का ज्वर फैलाती है और उस आत्मा को कर्मबंधन में जकड़ लेती है।
सांसारिकता के बीज : राग-द्वेष अज्ञान, आसक्ति और ममत्व का विषवृक्ष जो दिखाई देता है उसका ही दूसरा नाम संसार कहा गया है। इसके बीज माने गये हैं राग और द्वेष) राग और द्वेष की मौजूदगी का साफ मतलब माना जाना चाहिये कि वहाँ समता भावना का सामान्यतया अभाव है।
- किसी भी सांसारिक सम्बन्ध को अथवा पदार्थ को मैं अपने लिये प्रियकारी व सुखकारी मानता हूँ याने कि मैं चाहता हूँ तो उसके प्रति मेरी चाहना का भाव राग कहलाएगा। मेरे राग भाव को जो भी समर्थन देगा अथवा उसका अनुमोदन करेगा उसके प्रति भी मेरा राग भाव पैदा हो जायगा। इसके विपरीत जो मेरे द्वारा वांछित सम्बन्ध या पदार्थ की प्राप्ति में बाधा डालता है अथवा मेरे क्रियाकलापों का विरोध करता है, उसका भी मैं विरोधी हो जाऊंगा याने कि उसके प्रति मेरा द्वेष भाव जाग जायेगा। संसार के किसी भी प्राणी के प्रति उपजने वाले भावों में अधिकांशतः मनुष्य के मन में या तो राग रहता है अथवा द्वेष । सम्पर्क और संसर्ग से दोनों प्रकार के काषायिक भाव पैदा होते हैं और परिस्थितियों के बदलने के साथ बदलते रहते हैं।
मैंने महसूस किया है कि राग और द्वेष के भावों में मनुष्य का मन इतनी बुरी तरह से डोलायमान होता रहता है कि वह राग-द्वेष की दुर्भावनाओं से ग्रस्त रहकर अनर्थकारी कृत्य करता रहता है। राग और द्वेष सांसारिकता के बीज रूप होने से कर्मबंध के मूल कारण होते हैं। कर्म जन्म-मृत्यु का मूल हेतु है और जन्म-मृत्यु को ही दुःख कहा जाता है अतः रांग और द्वेष दुःख के भी मूल कारण हैं। जैसे जंगल में दावाग्नि से प्राणियों के जलने पर राग-द्वेष के वश होकर दूसरे प्राणी प्रसन्न होते हैं किन्तु वे यह नहीं जानते कि आगे बढ़ती हुई दावाग्नि उन्हें भी भस्म करके छोड़ेगी। उसी प्रकार काम-भोगों की आसक्ति में डूबे अज्ञानी प्राणी यह नहीं जानते कि संसार में राग-द्वेष की भावनाओं का जो दावानल जल रहा है, हम असावधान रहे तो हमें भी भस्म कर देगा। इस विचारशून्यता के कारण ऐसे मनुष्य उस दावानल से बचने का कोई यल नहीं करते हैं। अनियंत्रित राग और द्वेष आत्म गुणों का इतना संहार करते हैं जितना कि एक समर्थ शत्रु भी किसी मनुष्य का सुरक्षा सम्बन्धी अहित नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काम भोग अपने आप किसी मनुष्य में विकृति पैदा नहीं करते—ये तो मनुष्य के राग-द्वेष रूप मोह भाव होते हैं जिनमें जकड़ कर वह अपने आपको विकारों का पुतला बना लेता है। '
आत्म स्वरूप पर राग-द्वेष के ऐसे घातक प्रभाव का उल्लेख करते हुए वीतराग देवों की वाणी मेरे हृदय में उतरी है कि जो मनुष्य राग-द्वेष से रहित होता है, वही कसौटी पर कसे हुए और अग्नि में डालकर शुद्ध किये हुए सोने के समान निर्मल माना जाता है। जो राग-द्वेष को त्याग कर समभाव अपनाता है, वही निजात्मा द्वारा अपने आत्मस्वरूप को जानने वाला होता है। जो साधु राग
७४