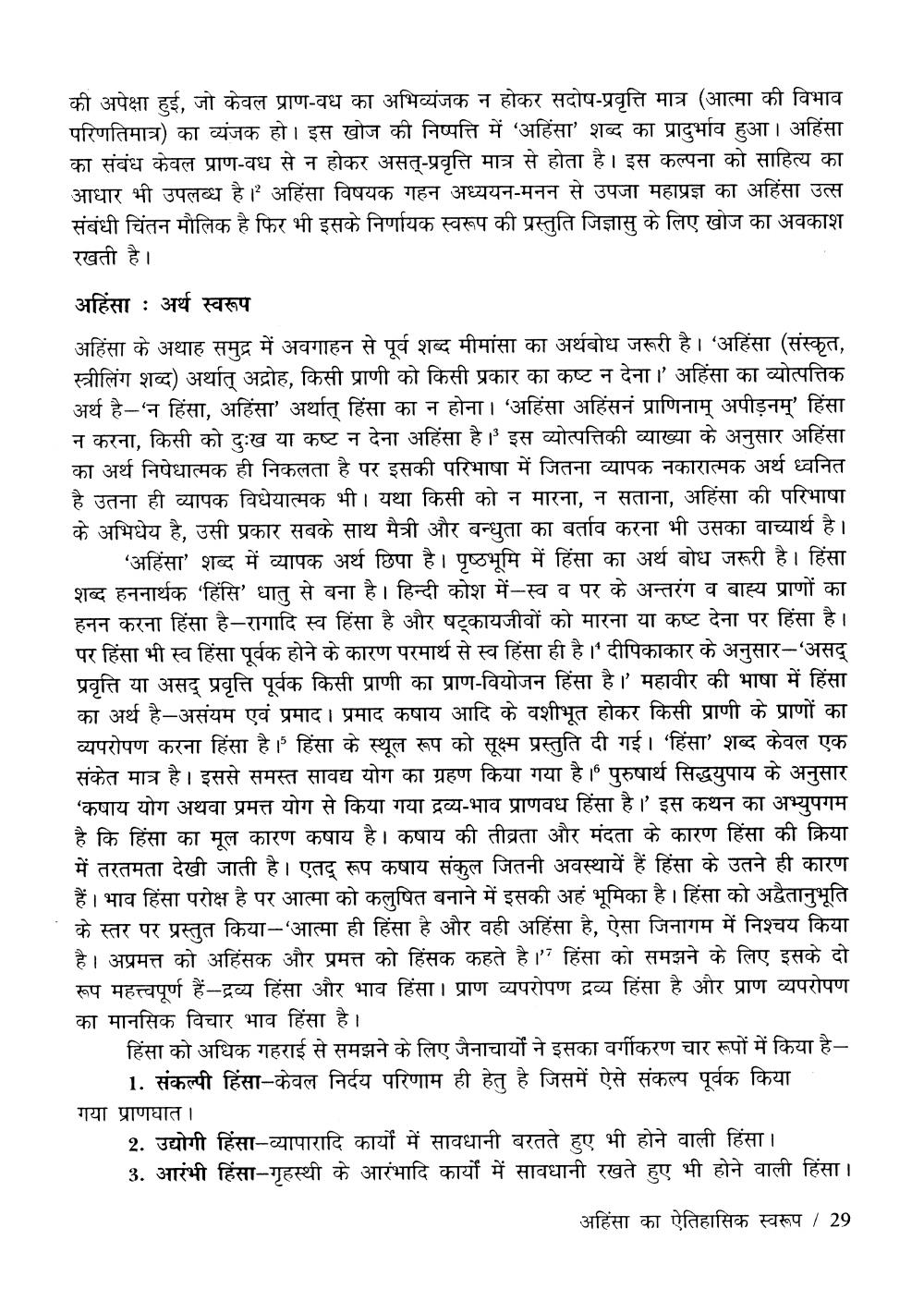________________
की अपेक्षा हुई, जो केवल प्राण-वध का अभिव्यंजक न होकर सदोष-प्रवृत्ति मात्र (आत्मा की विभाव परिणतिमात्र) का व्यंजक हो। इस खोज की निष्पत्ति में 'अहिंसा' शब्द का प्रादुर्भाव हुआ। अहिंसा का संबंध केवल प्राण-वध से न होकर असत्-प्रवृत्ति मात्र से होता है। इस कल्पना को साहित्य का आधार भी उपलब्ध है। अहिंसा विषयक गहन अध्ययन-मनन से उपजा महाप्रज्ञ का अहिंसा उत्स संबंधी चिंतन मौलिक है फिर भी इसके निर्णायक स्वरूप की प्रस्तुति जिज्ञासु के लिए खोज का अवकाश रखती है।
अहिंसा : अर्थ स्वरूप अहिंसा के अथाह समुद्र में अवगाहन से पूर्व शब्द मीमांसा का अर्थबोध जरूरी है। 'अहिंसा (संस्कृत, स्त्रीलिंग शब्द) अर्थात् अद्रोह, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना।' अहिंसा का व्योत्पत्तिक अर्थ है-'न हिंसा, अहिंसा' अर्थात् हिंसा का न होना। 'अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम् अपीड़नम्' हिंसा न करना, किसी को दुःख या कष्ट न देना अहिंसा है। इस व्योत्पत्तिकी व्याख्या के अनुसार अहिंसा का अर्थ निषेधात्मक ही निकलता है पर इसकी परिभाषा में जितना व्यापक नकारात्मक अर्थ ध्वनित है उतना ही व्यापक विधेयात्मक भी। यथा किसी को न मारना, न सताना, अहिंसा की परिभाषा के अभिधेय है, उसी प्रकार सबके साथ मैत्री और बन्धुता का बर्ताव करना भी उसका वाच्यार्थ है।
'अहिंसा' शब्द में व्यापक अर्थ छिपा है। पृष्ठभूमि में हिंसा का अर्थ बोध जरूरी है। हिंसा शब्द हननार्थक 'हिंसि' धातु से बना है। हिन्दी कोश में-स्व व पर के अन्तरंग व बाह्य प्राणों का हनन करना हिंसा है-रागादि स्व हिंसा है और षट्कायजीवों को मारना या कष्ट देना पर हिंसा है। पर हिंसा भी स्व हिंसा पूर्वक होने के कारण परमार्थ से स्व हिंसा ही है।' दीपिकाकार के अनुसार-'असद् प्रवृत्ति या असद् प्रवृत्ति पूर्वक किसी प्राणी का प्राण-वियोजन हिंसा है।' महावीर की भाषा में हिंसा का अर्थ है-असंयम एवं प्रमाद। प्रमाद कषाय आदि के वशीभूत होकर किसी प्राणी के प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा है। हिंसा के स्थूल रूप को सूक्ष्म प्रस्तुति दी गई। 'हिंसा' शब्द केवल एक संकेत मात्र है। इससे समस्त सावध योग का ग्रहण किया गया है। पुरुषार्थ सिद्धयुपाय के अनुसार 'कषाय योग अथवा प्रमत्त योग से किया गया द्रव्य-भाव प्राणवध हिंसा है।' इस कथन का अभ्यपगम है कि हिंसा का मूल कारण कषाय है। कषाय की तीव्रता और मंदता के कारण हिंसा की क्रिया में तरतमता देखी जाती है। एतद् रूप कषाय संकुल जितनी अवस्थायें हैं हिंसा के उतने ही कारण हैं। भाव हिंसा परोक्ष है पर आत्मा को कलुषित बनाने में इसकी अहं भूमिका है। हिंसा को अद्वैतानुभूति के स्तर पर प्रस्तुत किया- 'आत्मा ही हिंसा है और वही अहिंसा है, ऐसा जिनागम में निश्चय किया है। अप्रमत्त को अहिंसक और प्रमत्त को हिंसक कहते है।" हिंसा को समझने के लिए इसके दो रूप महत्त्वपूर्ण हैं-द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। प्राण व्यपरोपण द्रव्य हिंसा है और प्राण व्यपरोपण का मानसिक विचार भाव हिंसा है।
हिंसा को अधिक गहराई से समझने के लिए जैनाचार्यों ने इसका वर्गीकरण चार रूपों में किया है
1. संकल्पी हिंसा-केवल निर्दय परिणाम ही हेतु है जिसमें ऐसे संकल्प पूर्वक किया गया प्राणघात।
2. उद्योगी हिंसा-व्यापारादि कार्यों में सावधानी बरतते हुए भी होने वाली हिंसा। 3. आरंभी हिंसा-गृहस्थी के आरंभादि कार्यों में सावधानी रखते हुए भी होने वाली हिंसा।
अहिंसा का ऐतिहासिक स्वरूप / 29