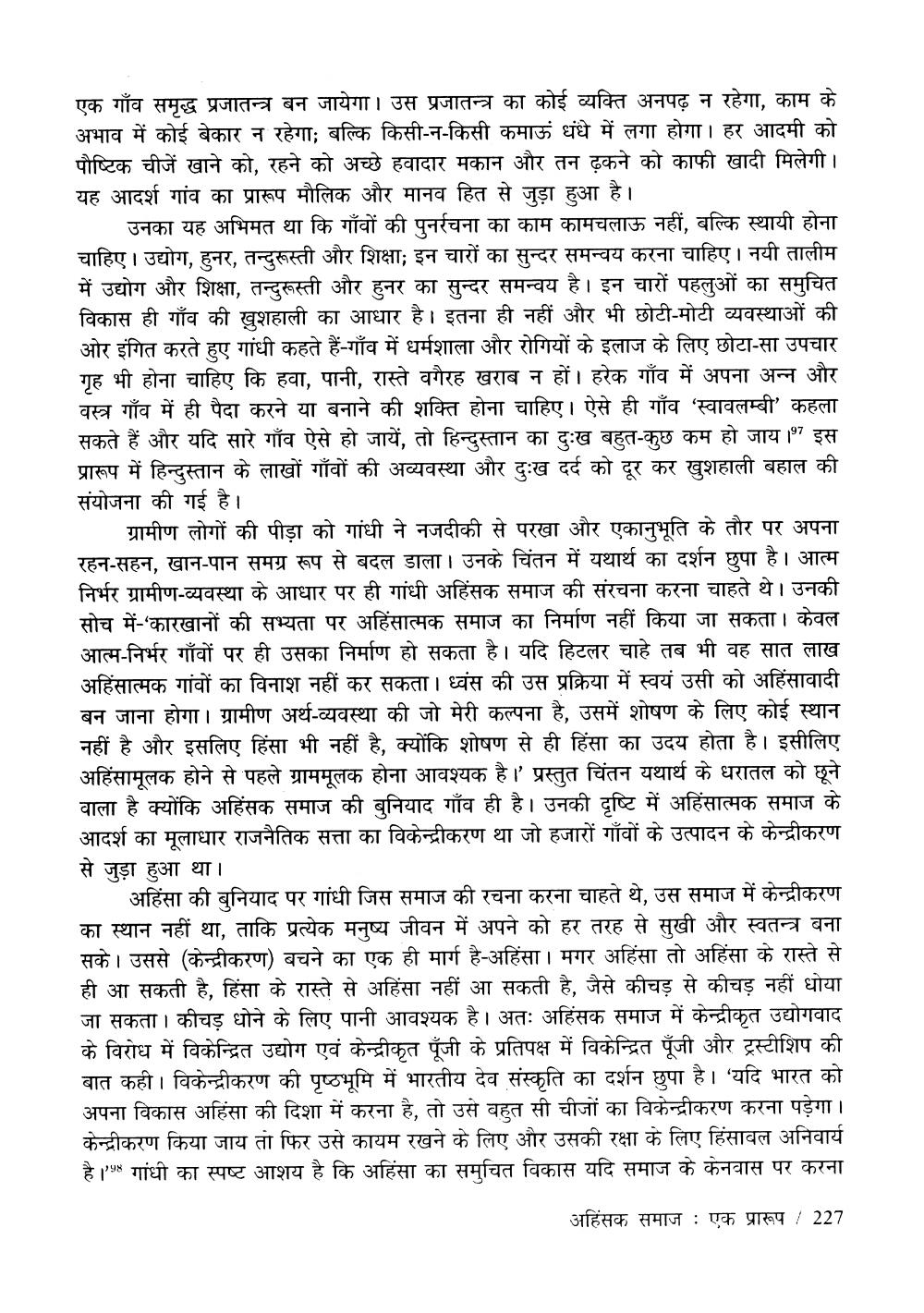________________
एक गाँव समृद्ध प्रजातन्त्र बन जायेगा । उस प्रजातन्त्र का कोई व्यक्ति अनपढ़ न रहेगा, काम के अभाव में कोई बेकार न रहेगा; बल्कि किसी-न-किसी कमाऊं धंधे में लगा होगा। हर आदमी को पौष्टिक चीजें खाने को, रहने को अच्छे हवादार मकान और तन ढकने को काफी खादी मिलेगी । यह आदर्श गांव का प्रारूप मौलिक और मानव हित से जुड़ा हुआ है ।
उनका यह अभिमत था कि गाँवों की पुनर्रचना का काम कामचलाऊ नहीं, बल्कि स्थायी होना चाहिए । उद्योग, हुनर, तन्दुरूस्ती और शिक्षा; इन चारों का सुन्दर समन्वय करना चाहिए । नयी तालीम में उद्योग और शिक्षा, तन्दुरूस्ती और हुनर का सुन्दर समन्वय है । इन चारों पहलुओं का समुचित विकास ही गाँव की खुशहाली का आधार है। इतना ही नहीं और भी छोटी-मोटी व्यवस्थाओं की ओर इंगित करते हुए गांधी कहते हैं - गाँव में धर्मशाला और रोगियों के इलाज के लिए छोटा सा उपचार गृह भी होना चाहिए कि हवा, पानी, रास्ते वगैरह खराब न हों । हरेक गाँव में अपना अन्न और वस्त्र गाँव में ही पैदा करने या बनाने की शक्ति होना चाहिए । ऐसे ही गाँव 'स्वावलम्बी ' कहला सकते हैं और यदि सारे गाँव ऐसे हो जायें, तो हिन्दुस्तान का दुःख बहुत कुछ कम हो जाय ।" इस प्रारूप में हिन्दुस्तान के लाखों गाँवों की अव्यवस्था और दुःख दर्द को दूर कर खुशहाली बहाल की संयोजना की गई है ।
ग्रामीण लोगों की पीड़ा को गांधी ने नजदीकी से परखा और एकानुभूति के तौर पर अपना रहन-सहन, खान-पान समग्र रूप से बदल डाला। उनके चिंतन में यथार्थ का दर्शन छुपा है । आत्म निर्भर ग्रामीण व्यवस्था के आधार पर ही गांधी अहिंसक समाज की संरचना करना चाहते थे । उनकी सोच में- 'कारखानों की सभ्यता पर अहिंसात्मक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। केवल आत्म-निर्भर गाँवों पर ही उसका निर्माण हो सकता है । यदि हिटलर चाहे तब भी वह सात लाख अहिंसात्मक गांवों का विनाश नहीं कर सकता । ध्वंस की उस प्रक्रिया में स्वयं उसी को अहिंसावादी बन जाना होगा। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की जो मेरी कल्पना है, उसमें शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है और इसलिए हिंसा भी नहीं है, क्योंकि शोषण से ही हिंसा का उदय होता है । इसीलिए अहिंसामूलक होने से पहले ग्राममूलक होना आवश्यक है।' प्रस्तुत चिंतन यथार्थ के धरातल को छूने वाला है क्योंकि अहिंसक समाज की बुनियाद गाँव ही है। उनकी दृष्टि में अहिंसात्मक समाज के आदर्श का मूलाधार राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण था जो हजारों गाँवों के उत्पादन के केन्द्रीकरण से जुड़ा हुआ था ।
अहिंसा की बुनियाद पर गांधी जिस समाज की रचना करना चाहते थे, उस समाज में केन्द्रीकरण का स्थान नहीं था, ताकि प्रत्येक मनुष्य जीवन में अपने को हर तरह से सुखी और स्वतन्त्र बना सके। उससे (केन्द्रीकरण) बचने का एक ही मार्ग है-अहिंसा । मगर अहिंसा तो अहिंसा के रास्ते से ही आ सकती है, हिंसा के रास्ते से अहिंसा नहीं आ सकती है, जैसे कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता । कीचड़ धोने के लिए पानी आवश्यक है । अतः अहिंसक समाज में केन्द्रीकृत उद्योगवाद
विरोध में विकेन्द्रित उद्योग एवं केन्द्रीकृत पूँजी के प्रतिपक्ष में विकेन्द्रित पूँजी और ट्रस्टीशिप की बात कही। विकेन्द्रीकरण की पृष्ठभूमि में भारतीय देव संस्कृति का दर्शन छुपा है । 'यदि भारत को अपना विकास अहिंसा की दिशा में करना है, तो उसे बहुत सी चीजों का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा । केन्द्रीकरण किया जाय तो फिर उसे कायम रखने के लिए और उसकी रक्षा के लिए हिंसावल अनिवार्य
8 गांधी का स्पष्ट आशय है कि अहिंसा का समुचित विकास यदि समाज के केनवास पर करना
अहिंसक समाज एक प्रारूप / 227