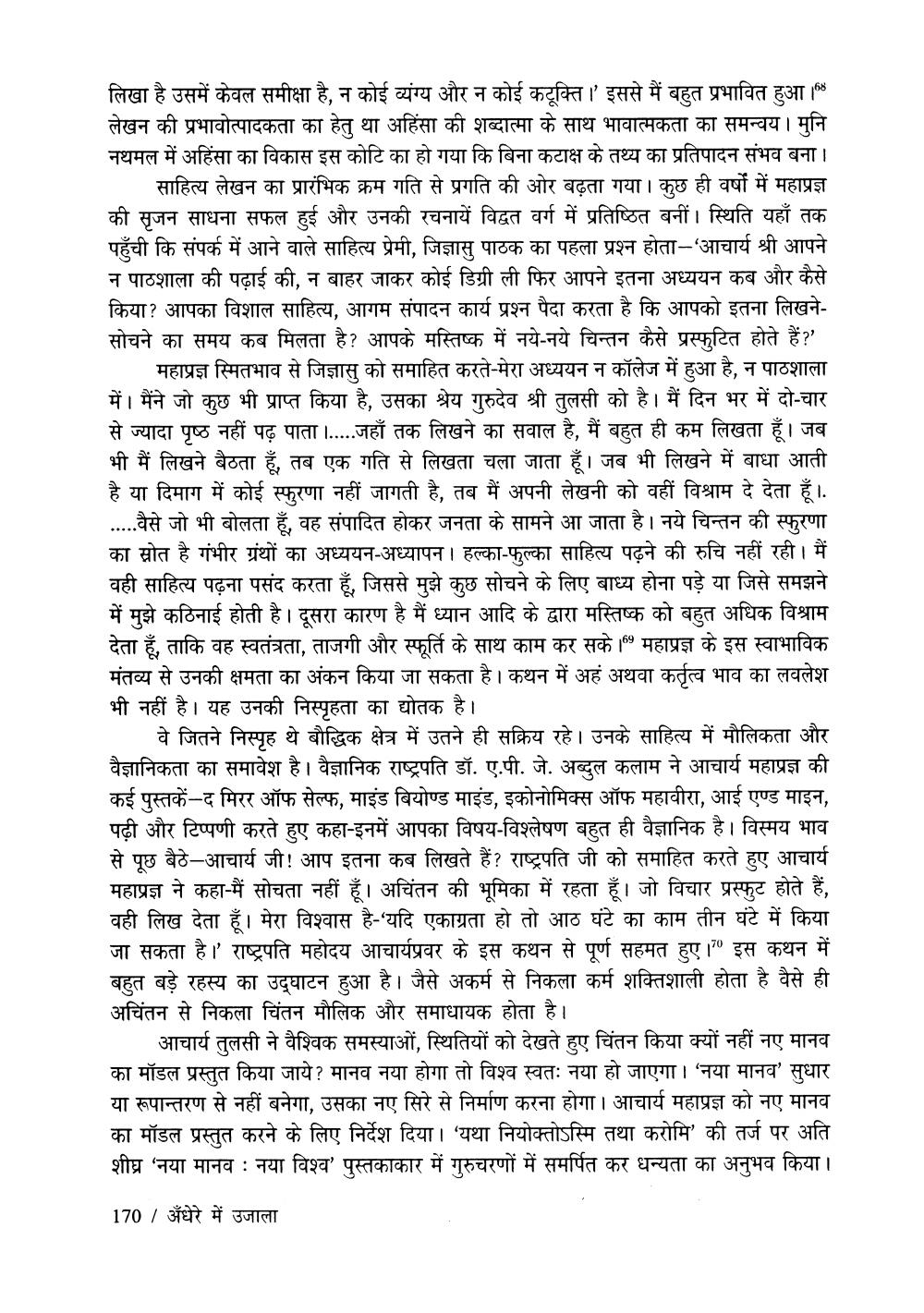________________
लिखा है उसमें केवल समीक्षा है, न कोई व्यंग्य और न कोई कटूक्ति ।' इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेखन की प्रभावोत्पादकता का हेतु था अहिंसा की शब्दात्मा के साथ भावात्मकता का समन्वय । नथमल में अहिंसा का विकास इस कोटि का हो गया कि बिना कटाक्ष के तथ्य का प्रतिपादन संभव बना ।
साहित्य लेखन का प्रारंभिक क्रम गति से प्रगति की ओर बढ़ता गया । कुछ ही वर्षों में महाप्रज्ञ की सृजन साधना सफल हुई और उनकी रचनायें विद्वत वर्ग में प्रतिष्ठित बनीं। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि संपर्क में आने वाले साहित्य प्रेमी, जिज्ञासु पाठक का पहला प्रश्न होता - 'आचार्य श्री आपने न पाठशाला की पढ़ाई की, न बाहर जाकर कोई डिग्री ली फिर आपने इतना अध्ययन कब और कैसे किया ? आपका विशाल साहित्य, आगम संपादन कार्य प्रश्न पैदा करता है कि आपको इतना लिखनेसोचने का समय कब मिलता है? आपके मस्तिष्क में नये-नये चिन्तन कैसे प्रस्फुटित होते हैं ? '
महाप्रज्ञ स्मितभाव से जिज्ञासु को समाहित करते - मेरा अध्ययन न कॉलेज में हुआ है, न पाठशाला * । मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसका श्रेय गुरुदेव श्री तुलसी को है । मैं दिन भर में दो-चार से ज्यादा पृष्ठ नहीं पढ़ पाता ।..... जहाँ तक लिखने का सवाल है, मैं बहुत ही कम लिखता हूँ । जब भी मैं लिखने बैठता हूँ, तब एक गति से लिखता चला जाता हूँ। जब भी लिखने में बाधा आती है या दिमाग में कोई स्फुरणा नहीं जागती है, तब मैं अपनी लेखनी को वहीं विश्राम दे देता हूँ ।. .. वैसे जो भी बोलता हूँ, वह संपादित होकर जनता के सामने आ जाता है। नये चिन्तन की स्फुरणा का स्रोत है गंभीर ग्रंथों का अध्ययन-अध्यापन । हल्का-फुल्का साहित्य पढ़ने की रुचि नहीं रही । मैं वही साहित्य पढ़ना पसंद करता हूँ, जिससे मुझे कुछ सोचने के लिए बाध्य होना पड़े या जिसे समझने में मुझे कठिनाई होती है। दूसरा कारण है मैं ध्यान आदि के द्वारा मस्तिष्क को बहुत अधिक विश्राम देता हूँ, ताकि वह स्वतंत्रता, ताजगी और स्फूर्ति के साथ काम कर सके। 69 महाप्रज्ञ के इस स्वाभाविक मंतव्य से उनकी क्षमता का अंकन किया जा सकता है । कथन 'अहं अथवा कर्तृत्व भाव का लवलेश भी नहीं है । यह उनकी निस्पृहता का द्योतक है।
1
वे जितने निस्पृह थे बौद्धिक क्षेत्र में उतने ही सक्रिय रहे। उनके साहित्य में मौलिकता और वैज्ञानिकता का समावेश है । वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने आचार्य महाप्रज्ञ की कई पुस्तकें—द मिरर ऑफ सेल्फ, माइंड बियोण्ड माइंड, इकोनोमिक्स ऑफ महावीरा, आई एण्ड माइन, पढ़ी और टिप्पणी करते हुए कहा- इनमें आपका विषय-विश्लेषण बहुत ही वैज्ञानिक है । विस्मय भाव से पूछ बैठे - आचार्य जी ! आप इतना कब लिखते हैं? राष्ट्रपति जी को समाहित करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ कहा-मैं सोचता नहीं हूँ। अचिंतन की भूमिका में रहता हूँ। जो विचार प्रस्फुट होते हैं, वही लिख देता हूँ। मेरा विश्वास है- 'यदि एकाग्रता हो तो आठ घंटे का काम तीन घंटे में किया जा सकता है।' राष्ट्रपति महोदय आचार्यप्रवर के इस कथन से पूर्ण सहमत हुए।" इस कथन में बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन हुआ है। जैसे अकर्म से निकला कर्म शक्तिशाली होता है वैसे ही अचिंतन से निकला चिंतन मौलिक और समाधायक होता है ।
आचार्य तुलसी ने वैश्विक समस्याओं, स्थितियों को देखते हुए चिंतन किया क्यों नहीं नए मानव का मॉडल प्रस्तुत किया जाये ? मानव नया होगा तो विश्व स्वतः नया हो जाएगा। 'नया मानव' सुधार या रूपान्तरण से नहीं बनेगा, उसका नए सिरे से निर्माण करना होगा । आचार्य महाप्रज्ञ को नए मानव का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया । 'यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि की तर्ज पर अति शीघ्र 'नया मानव : नया विश्व' पुस्तकाकार में गुरुचरणों में समर्पित कर धन्यता का अनुभव किया । 170 / अँधेरे में उजाला