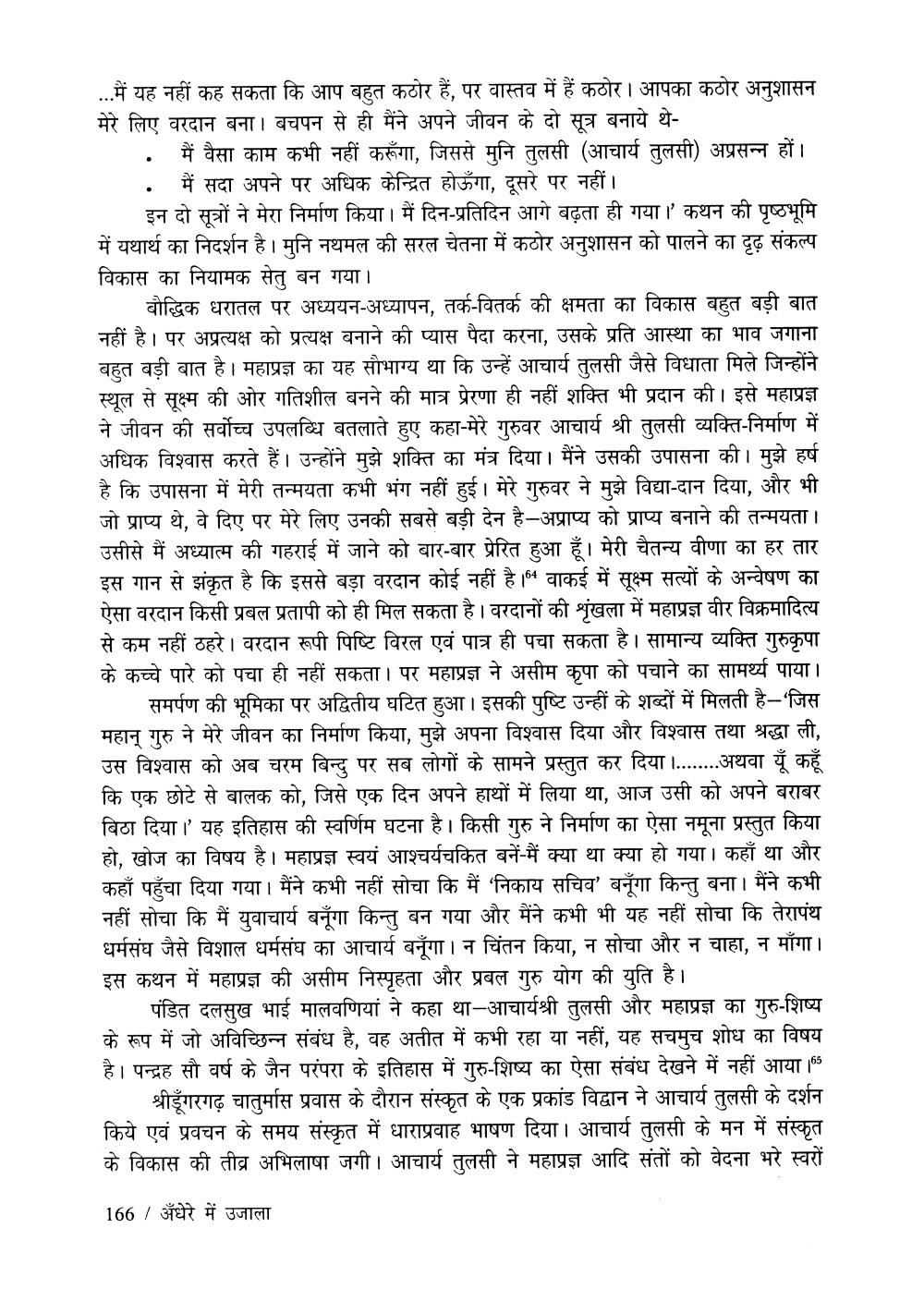________________
...मैं यह नहीं कह सकता कि आप बहुत कठोर हैं, पर वास्तव में हैं कठोर । आपका कठोर अनुशासन मेरे लिए वरदान बना। बचपन से ही मैंने अपने जीवन के दो सूत्र बनाये थे
. मैं वैसा काम कभी नहीं करूँगा, जिससे मुनि तुलसी (आचार्य तुलसी) अप्रसन्न हों। . मैं सदा अपने पर अधिक केन्द्रित होऊँगा, दूसरे पर नहीं।
इन दो सूत्रों ने मेरा निर्माण किया। मैं दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ता ही गया।' कथन की पृष्ठभूमि में यथार्थ का निदर्शन है। मुनि नथमल की सरल चेतना में कठोर अनुशासन को पालने का दृढ़ संकल्प विकास का नियामक सेतु बन गया।
बौद्धिक धरातल पर अध्ययन-अध्यापन, तर्क-वितर्क की क्षमता का विकास बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष बनाने की प्यास पैदा करना, उसके प्रति आस्था का भाव जगाना बहुत बड़ी बात है। महाप्रज्ञ का यह सौभाग्य था कि उन्हें आचार्य तुलसी जैसे विधाता मिले जिन्होंने स्थूल से सूक्ष्म की ओर गतिशील बनने की मात्र प्रेरणा ही नहीं शक्ति भी प्रदान की। इसे महाप्रज्ञ ने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि बतलाते हुए कहा-मेरे गुरुवर आचार्य श्री तुलसी व्यक्ति-निर्माण में अधिक विश्वास करते हैं। उन्होंने मुझे शक्ति का मंत्र दिया। मैंने उसकी उपासना की। मुझे हर्ष है कि उपासना में मेरी तन्मयता कभी भंग नहीं हुई। मेरे गुरुवर ने मुझे विद्या-दान दिया, और भी जो प्राप्य थे, वे दिए पर मेरे लिए उनकी सबसे बड़ी देन है-अप्राप्य को प्राप्य बनाने की तन्मयता। उसीसे मैं अध्यात्म की गहराई में जाने को बार-बार प्रेरित हुआ हूँ। मेरी चैतन्य वीणा का हर तार इस गान से झंकृत है कि इससे बड़ा वरदान कोई नहीं है। वाकई में सक्ष्म सत्यों के अन्वेषण का ऐसा वरदान किसी प्रबल प्रतापी को ही मिल सकता है। वरदानों की श्रृंखला में महाप्रज्ञ वीर विक्रमादित्य से कम नहीं ठहरे। वरदान रूपी पिष्टि विरल एवं पात्र ही पचा सकता है। सामान्य व्यक्ति गुरुकृपा के कच्चे पारे को पचा ही नहीं सकता। पर महाप्रज्ञ ने असीम कपा को पचाने का सामर्थ्य पाया।
समर्पण की भूमिका पर अद्वितीय घटित हुआ। इसकी पुष्टि उन्हीं के शब्दों में मिलती है-'जिस महान् गुरु ने मेरे जीवन का निर्माण किया, मुझे अपना विश्वास दिया और विश्वास तथा श्रद्धा ली, उस विश्वास को अब चरम बिन्दु पर सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया।........अथवा यूँ कहूँ कि एक छोटे से बालक को, जिसे एक दिन अपने हाथों में लिया था, आज उसी को अपने बराबर बिठा दिया।' यह इतिहास की स्वर्णिम घटना है। किसी गुरु ने निर्माण का ऐसा नमूना प्रस्तुत किया हो, खोज का विषय है। महाप्रज्ञ स्वयं आश्चर्यचकित बनें-मैं क्या था क्या हो गया। कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं 'निकाय सचिव' बनूँगा किन्तु बना। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं युवाचार्य बनूँगा किन्तु बन गया और मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि तेरापंथ धर्मसंघ जैसे विशाल धर्मसंघ का आचार्य बनूँगा। न चिंतन किया, न सोचा और न चाहा, न माँगा। इस कथन में महाप्रज्ञ की असीम निस्पृहता और प्रबल गुरु योग की युति है।
पंडित दलसुख भाई मालवणियां ने कहा था-आचार्यश्री तुलसी और महाप्रज्ञ का गुरु-शिष्य के रूप में जो अविच्छिन्न संबंध है, वह अतीत में कभी रहा या नहीं, यह सचमुच शोध का विषय है। पन्द्रह सौ वर्ष के जैन परंपरा के इतिहास में गुरु-शिष्य का ऐसा संबंध देखने में नहीं आया।
श्रीडूंगरगढ़ चातुर्मास प्रवास के दौरान संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान ने आचार्य तुलसी के दर्शन किये एवं प्रवचन के समय संस्कृत में धाराप्रवाह भाषण दिया। आचार्य तुलसी के मन में संस्कृत के विकास की तीव्र अभिलाषा जगी। आचार्य तुलसी ने महाप्रज्ञ आदि संतों को वेदना भरे स्वरों
166 / अँधेरे में उजाला