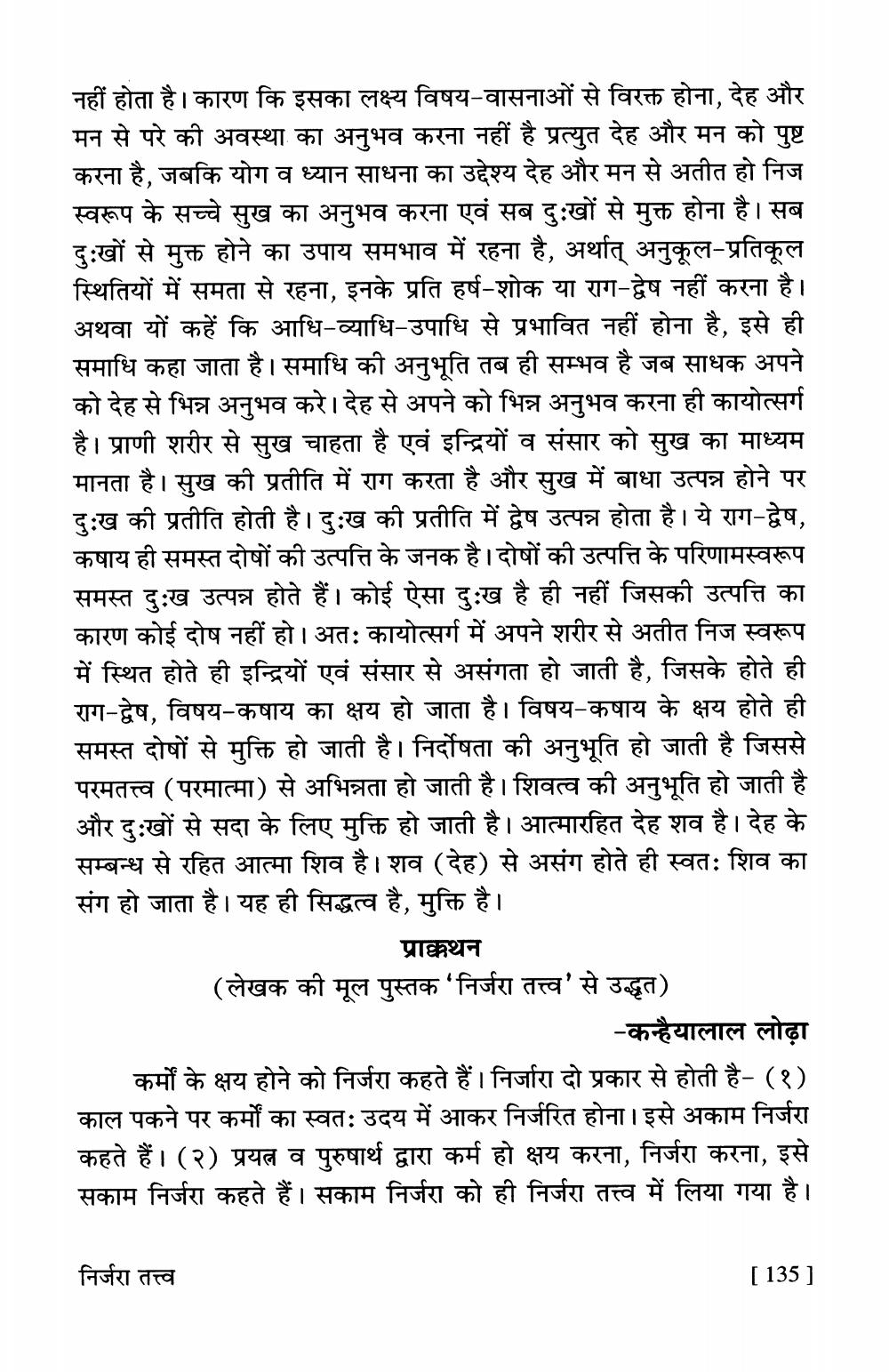________________
नहीं होता है। कारण कि इसका लक्ष्य विषय-वासनाओं से विरक्त होना, देह और मन से परे की अवस्था का अनुभव करना नहीं है प्रत्युत देह और मन को पुष्ट करना है, जबकि योग व ध्यान साधना का उद्देश्य देह और मन से अतीत हो निज स्वरूप के सच्चे सुख का अनुभव करना एवं सब दु:खों से मुक्त होना है। सब दुःखों से मुक्त होने का उपाय समभाव में रहना है, अर्थात् अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों में समता से रहना, इनके प्रति हर्ष-शोक या राग-द्वेष नहीं करना है। अथवा यों कहें कि आधि-व्याधि-उपाधि से प्रभावित नहीं होना है, इसे ही समाधि कहा जाता है। समाधि की अनुभूति तब ही सम्भव है जब साधक अपने को देह से भिन्न अनुभव करे। देह से अपने को भिन्न अनुभव करना ही कायोत्सर्ग है। प्राणी शरीर से सुख चाहता है एवं इन्द्रियों व संसार को सुख का माध्यम मानता है। सुख की प्रतीति में राग करता है और सुख में बाधा उत्पन्न होने पर दु:ख की प्रतीति होती है। दुःख की प्रतीति में द्वेष उत्पन्न होता है। ये राग-द्वेष, कषाय ही समस्त दोषों की उत्पत्ति के जनक है। दोषों की उत्पत्ति के परिणामस्वरूप समस्त दु:ख उत्पन्न होते हैं। कोई ऐसा दुःख है ही नहीं जिसकी उत्पत्ति का कारण कोई दोष नहीं हो। अतः कायोत्सर्ग में अपने शरीर से अतीत निज स्वरूप में स्थित होते ही इन्द्रियों एवं संसार से असंगता हो जाती है, जिसके होते ही राग-द्वेष, विषय-कषाय का क्षय हो जाता है। विषय-कषाय के क्षय होते ही समस्त दोषों से मुक्ति हो जाती है। निर्दोषता की अनुभूति हो जाती है जिससे परमतत्त्व (परमात्मा) से अभिन्नता हो जाती है। शिवत्व की अनुभूति हो जाती है और दु:खों से सदा के लिए मुक्ति हो जाती है। आत्मारहित देह शव है। देह के सम्बन्ध से रहित आत्मा शिव है। शव (देह) से असंग होते ही स्वतः शिव का संग हो जाता है। यह ही सिद्धत्व है, मुक्ति है।
प्राक्कथन (लेखक की मूल पुस्तक 'निर्जरा तत्त्व' से उद्धृत)
-कन्हैयालाल लोढ़ा कर्मों के क्षय होने को निर्जरा कहते हैं। निर्जारा दो प्रकार से होती है- (१) काल पकने पर कर्मों का स्वतः उदय में आकर निर्जरित होना। इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। (२) प्रयत्न व पुरुषार्थ द्वारा कर्म हो क्षय करना, निर्जरा करना, इसे सकाम निर्जरा कहते हैं। सकाम निर्जरा को ही निर्जरा तत्त्व में लिया गया है।
निर्जरा तत्त्व
[135]