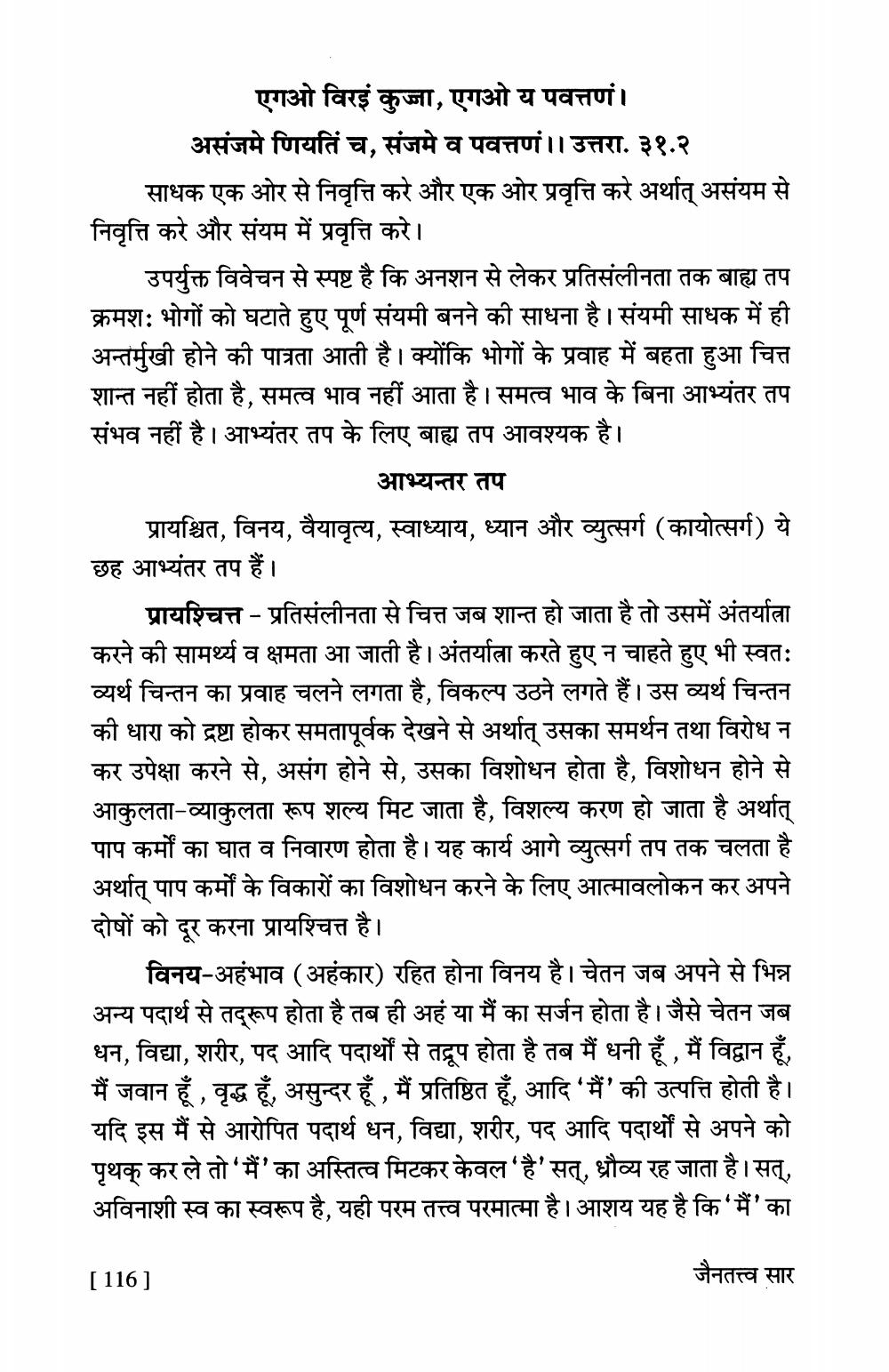________________
एगओ विरई कुजा, एगओ य पवत्तणं। असंजमे णियतिं च, संजमे व पवत्तणं। उत्तरा. ३१.२ साधक एक ओर से निवृत्ति करे और एक ओर प्रवृत्ति करे अर्थात् असंयम से निवृत्ति करे और संयम में प्रवृत्ति करे।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनशन से लेकर प्रतिसंलीनता तक बाह्य तप क्रमशः भोगों को घटाते हुए पूर्ण संयमी बनने की साधना है। संयमी साधक में ही अन्तर्मुखी होने की पात्रता आती है। क्योंकि भोगों के प्रवाह में बहता हुआ चित्त शान्त नहीं होता है, समत्व भाव नहीं आता है। समत्व भाव के बिना आभ्यंतर तप संभव नहीं है। आभ्यंतर तप के लिए बाह्य तप आवश्यक है।
आभ्यन्तर तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग (कायोत्सर्ग) ये छह आभ्यंतर तप हैं।
प्रायश्चित्त - प्रतिसंलीनता से चित्त जब शान्त हो जाता है तो उसमें अंतर्यात्रा करने की सामर्थ्य व क्षमता आ जाती है। अंतर्यात्रा करते हुए न चाहते हुए भी स्वतः व्यर्थ चिन्तन का प्रवाह चलने लगता है, विकल्प उठने लगते हैं। उस व्यर्थ चिन्तन की धारा को द्रष्टा होकर समतापूर्वक देखने से अर्थात् उसका समर्थन तथा विरोध न कर उपेक्षा करने से, असंग होने से, उसका विशोधन होता है, विशोधन होने से आकुलता-व्याकुलता रूप शल्य मिट जाता है, विशल्य करण हो जाता है अर्थात् पाप कर्मों का घात व निवारण होता है। यह कार्य आगे व्युत्सर्ग तप तक चलता है अर्थात् पाप कर्मों के विकारों का विशोधन करने के लिए आत्मावलोकन कर अपने दोषों को दूर करना प्रायश्चित्त है।
विनय-अहंभाव (अहंकार) रहित होना विनय है। चेतन जब अपने से भिन्न अन्य पदार्थ से तद्प होता है तब ही अहं या मैं का सर्जन होता है। जैसे चेतन जब धन, विद्या, शरीर, पद आदि पदार्थों से तद्रूप होता है तब मैं धनी हूँ , मैं विद्वान हूँ, मैं जवान हूँ , वृद्ध हूँ, असुन्दर हूँ , मैं प्रतिष्ठित हूँ, आदि 'मैं' की उत्पत्ति होती है। यदि इस मैं से आरोपित पदार्थ धन, विद्या, शरीर, पद आदि पदार्थों से अपने को पृथक् कर ले तो 'मैं' का अस्तित्व मिटकर केवल 'है' सत्, ध्रौव्य रह जाता है। सत्, अविनाशी स्व का स्वरूप है, यही परम तत्त्व परमात्मा है। आशय यह है कि 'मैं' का
[116]
जैनतत्त्व सार