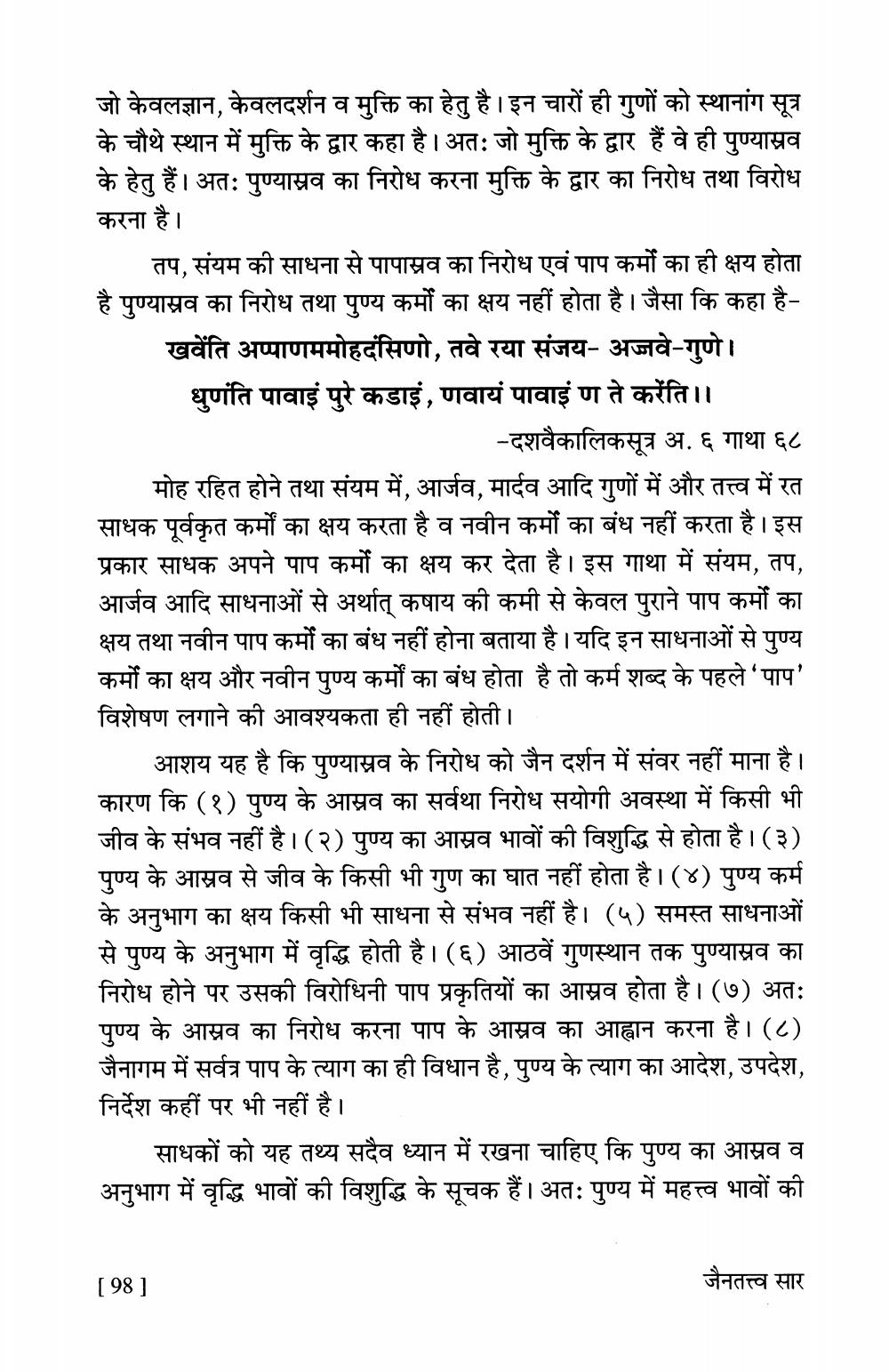________________
जो केवलज्ञान, केवलदर्शन व मुक्ति का हेतु है। इन चारों ही गुणों को स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान में मुक्ति के द्वार कहा है। अतः जो मुक्ति के द्वार हैं वे ही पुण्यासव के हेतु हैं। अतः पुण्यास्रव का निरोध करना मुक्ति के द्वार का निरोध तथा विरोध करना है।
तप, संयम की साधना से पापास्रव का निरोध एवं पाप कर्मों का ही क्षय होता है पुण्यास्रव का निरोध तथा पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता है। जैसा कि कहा है
खवेंति अप्पाणममोहदंसिणो, तवे रया संजय- अजवे-गुणे। धुणंति पावाइं पुरे कडाई, णवायं पावाई ण ते करेंति॥
-दशवैकालिकसूत्र अ. ६ गाथा ६८ मोह रहित होने तथा संयम में, आर्जव, मार्दव आदि गुणों में और तत्त्व में रत साधक पूर्वकृत कर्मों का क्षय करता है व नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है। इस प्रकार साधक अपने पाप कर्मो का क्षय कर देता है। इस गाथा में संयम, तप, आर्जव आदि साधनाओं से अर्थात् कषाय की कमी से केवल पुराने पाप कर्मों का क्षय तथा नवीन पाप कर्मों का बंध नहीं होना बताया है। यदि इन साधनाओं से पुण्य कर्मों का क्षय और नवीन पुण्य कर्मों का बंध होता है तो कर्म शब्द के पहले 'पाप' विशेषण लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती।
आशय यह है कि पुण्यास्रव के निरोध को जैन दर्शन में संवर नहीं माना है। कारण कि (१) पुण्य के आस्रव का सर्वथा निरोध सयोगी अवस्था में किसी भी जीव के संभव नहीं है। (२) पुण्य का आस्रव भावों की विशुद्धि से होता है। (३) पुण्य के आस्रव से जीव के किसी भी गुण का घात नहीं होता है। (४) पुण्य कर्म के अनुभाग का क्षय किसी भी साधना से संभव नहीं है। (५) समस्त साधनाओं से पुण्य के अनुभाग में वृद्धि होती है। (६) आठवें गुणस्थान तक पुण्यास्रव का निरोध होने पर उसकी विरोधिनी पाप प्रकृतियों का आस्रव होता है। (७) अतः पुण्य के आस्रव का निरोध करना पाप के आस्रव का आह्वान करना है। (८) जैनागम में सर्वत्र पाप के त्याग का ही विधान है, पुण्य के त्याग का आदेश, उपदेश, निर्देश कहीं पर भी नहीं है।
साधकों को यह तथ्य सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि पुण्य का आस्रव व अनुभाग में वृद्धि भावों की विशुद्धि के सूचक हैं। अतः पुण्य में महत्त्व भावों की
[98]
जैनतत्त्व सार