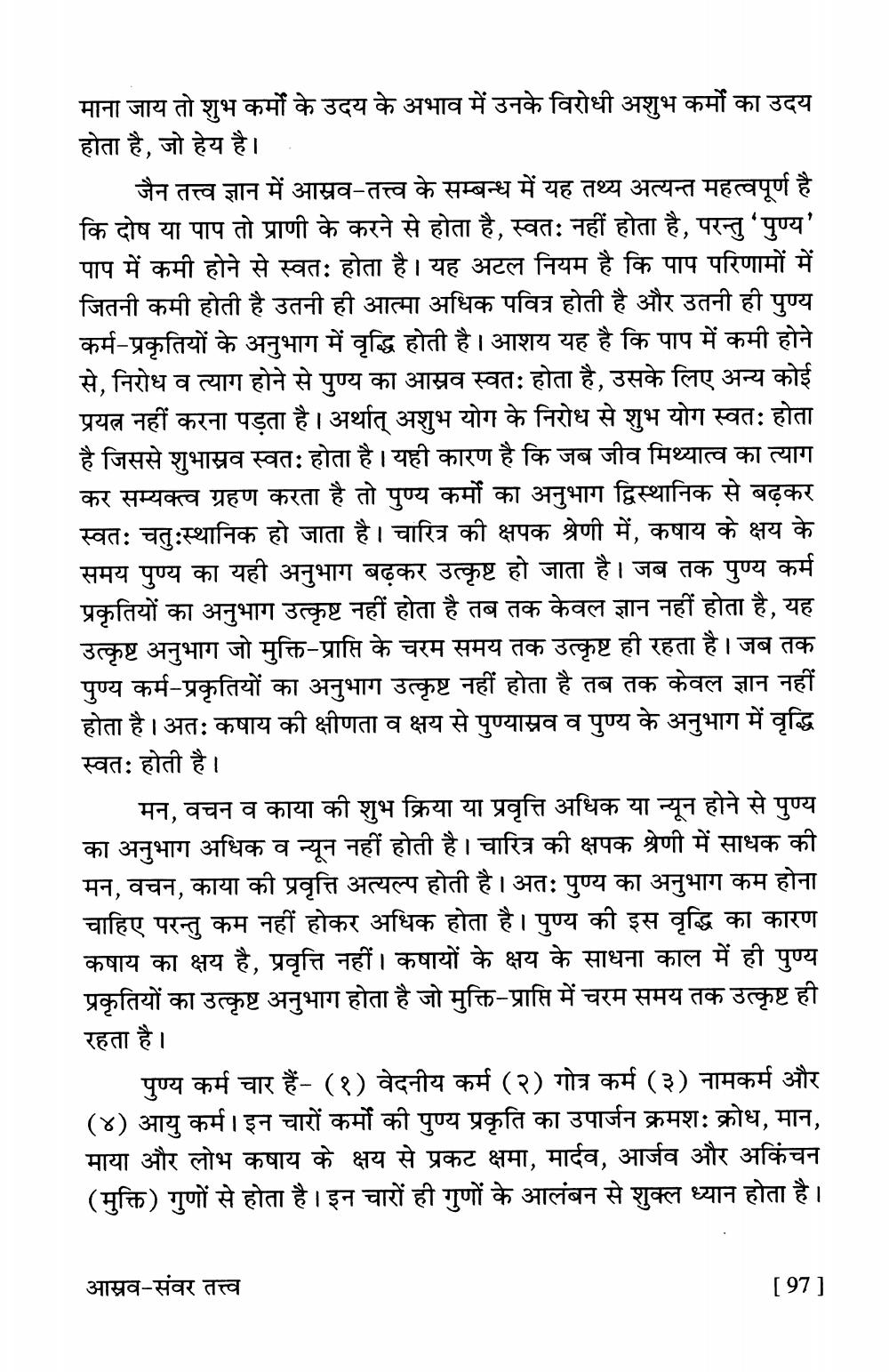________________
माना जाय तो शुभ कर्मों के उदय के अभाव में उनके विरोधी अशुभ कर्मों का उदय होता है, जो हेय है।
जैन तत्त्व ज्ञान में आस्रव-तत्त्व के सम्बन्ध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि दोष या पाप तो प्राणी के करने से होता है, स्वतः नहीं होता है, परन्तु 'पुण्य' पाप में कमी होने से स्वतः होता है। यह अटल नियम है कि पाप परिणामों में जितनी कमी होती है उतनी ही आत्मा अधिक पवित्र होती है और उतनी ही पुण्य कर्म-प्रकृतियों के अनुभाग में वृद्धि होती है। आशय यह है कि पाप में कमी होने से, निरोध व त्याग होने से पुण्य का आस्रव स्वतः होता है, उसके लिए अन्य कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अर्थात् अशुभ योग के निरोध से शुभ योग स्वतः होता है जिससे शुभास्रव स्वतः होता है। यही कारण है कि जब जीव मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक्त्व ग्रहण करता है तो पुण्य कर्मों का अनुभाग द्विस्थानिक से बढ़कर स्वतः चतु:स्थानिक हो जाता है। चारित्र की क्षपक श्रेणी में, कषाय के क्षय के समय पुण्य का यही अनुभाग बढ़कर उत्कृष्ट हो जाता है। जब तक पुण्य कर्म प्रकृतियों का अनुभाग उत्कृष्ट नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, यह उत्कृष्ट अनुभाग जो मुक्ति-प्राप्ति के चरम समय तक उत्कृष्ट ही रहता है। जब तक पुण्य कर्म-प्रकृतियों का अनुभाग उत्कृष्ट नहीं होता है तब तक केवल ज्ञान नहीं होता है। अतः कषाय की क्षीणता व क्षय से पुण्यास्रव व पुण्य के अनुभाग में वृद्धि स्वतः होती है।
मन, वचन व काया की शुभ क्रिया या प्रवृत्ति अधिक या न्यून होने से पुण्य का अनुभाग अधिक व न्यून नहीं होती है। चारित्र की क्षपक श्रेणी में साधक की मन, वचन, काया की प्रवृत्ति अत्यल्प होती है। अतः पुण्य का अनुभाग कम होना चाहिए परन्तु कम नहीं होकर अधिक होता है। पुण्य की इस वृद्धि का कारण कषाय का क्षय है, प्रवृत्ति नहीं। कषायों के क्षय के साधना काल में ही पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग होता है जो मुक्ति-प्राप्ति में चरम समय तक उत्कृष्ट ही रहता है।
पुण्य कर्म चार हैं- (१) वेदनीय कर्म (२) गोत्र कर्म (३) नामकर्म और (४) आयु कर्म। इन चारों कर्मों की पुण्य प्रकृति का उपार्जन क्रमशः क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय के क्षय से प्रकट क्षमा, मार्दव, आर्जव और अकिंचन (मुक्ति) गुणों से होता है। इन चारों ही गुणों के आलंबन से शुक्ल ध्यान होता है।
आस्रव-संवर तत्त्व
[97]