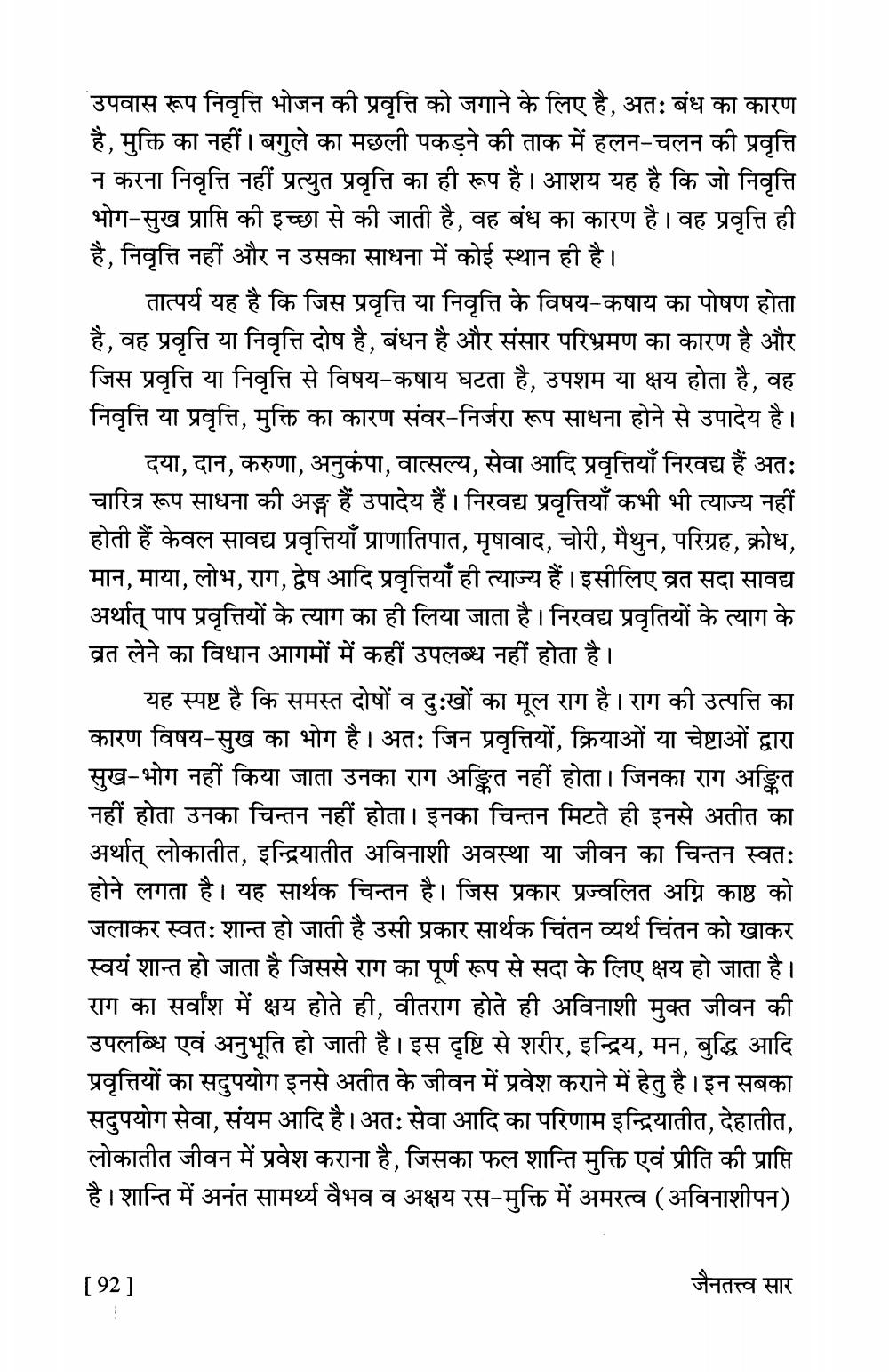________________
उपवास रूप निवृत्ति भोजन की प्रवृत्ति को जगाने के लिए है, अत: बंध का कारण है, मुक्ति का नहीं। बगुले का मछली पकड़ने की ताक में हलन-चलन की प्रवृत्ति न करना निवृत्ति नहीं प्रत्युत प्रवृत्ति का ही रूप है। आशय यह है कि जो निवृत्ति भोग-सुख प्राप्ति की इच्छा से की जाती है, वह बंध का कारण है। वह प्रवृत्ति ही है, निवृत्ति नहीं और न उसका साधना में कोई स्थान ही है।
तात्पर्य यह है कि जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति के विषय-कषाय का पोषण होता है, वह प्रवृत्ति या निवृत्ति दोष है, बंधन है और संसार परिभ्रमण का कारण है और जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति से विषय-कषाय घटता है, उपशम या क्षय होता है, वह निवृत्ति या प्रवृत्ति, मुक्ति का कारण संवर-निर्जरा रूप साधना होने से उपादेय है।
दया, दान, करुणा, अनुकंपा, वात्सल्य, सेवा आदि प्रवृत्तियाँ निरवद्य हैं अतः चारित्र रूप साधना की अङ्ग हैं उपादेय हैं। निरवद्य प्रवृत्तियाँ कभी भी त्याज्य नहीं होती हैं केवल सावद्य प्रवृत्तियाँ प्राणातिपात, मृषावाद, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियाँ ही त्याज्य हैं। इसीलिए व्रत सदा सावध अर्थात् पाप प्रवृत्तियों के त्याग का ही लिया जाता है। निरवद्य प्रवृतियों के त्याग के व्रत लेने का विधान आगमों में कहीं उपलब्ध नहीं होता है।
यह स्पष्ट है कि समस्त दोषों व दु:खों का मूल राग है। राग की उत्पत्ति का कारण विषय-सुख का भोग है। अतः जिन प्रवृत्तियों, क्रियाओं या चेष्टाओं द्वारा सुख-भोग नहीं किया जाता उनका राग अङ्कित नहीं होता। जिनका राग अङ्कित नहीं होता उनका चिन्तन नहीं होता। इनका चिन्तन मिटते ही इनसे अतीत का अर्थात् लोकातीत, इन्द्रियातीत अविनाशी अवस्था या जीवन का चिन्तन स्वतः होने लगता है। यह सार्थक चिन्तन है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को जलाकर स्वतः शान्त हो जाती है उसी प्रकार सार्थक चिंतन व्यर्थ चिंतन को खाकर स्वयं शान्त हो जाता है जिससे राग का पूर्ण रूप से सदा के लिए क्षय हो जाता है। राग का सर्वांश में क्षय होते ही, वीतराग होते ही अविनाशी मुक्त जीवन की उपलब्धि एवं अनुभूति हो जाती है। इस दृष्टि से शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि प्रवृत्तियों का सदुपयोग इनसे अतीत के जीवन में प्रवेश कराने में हेतु है। इन सबका सदुपयोग सेवा, संयम आदि है। अतः सेवा आदि का परिणाम इन्द्रियातीत, देहातीत, लोकातीत जीवन में प्रवेश कराना है, जिसका फल शान्ति मुक्ति एवं प्रीति की प्राप्ति है। शान्ति में अनंत सामर्थ्य वैभव व अक्षय रस-मुक्ति में अमरत्व (अविनाशीपन)
[92]
जैनतत्त्व सार