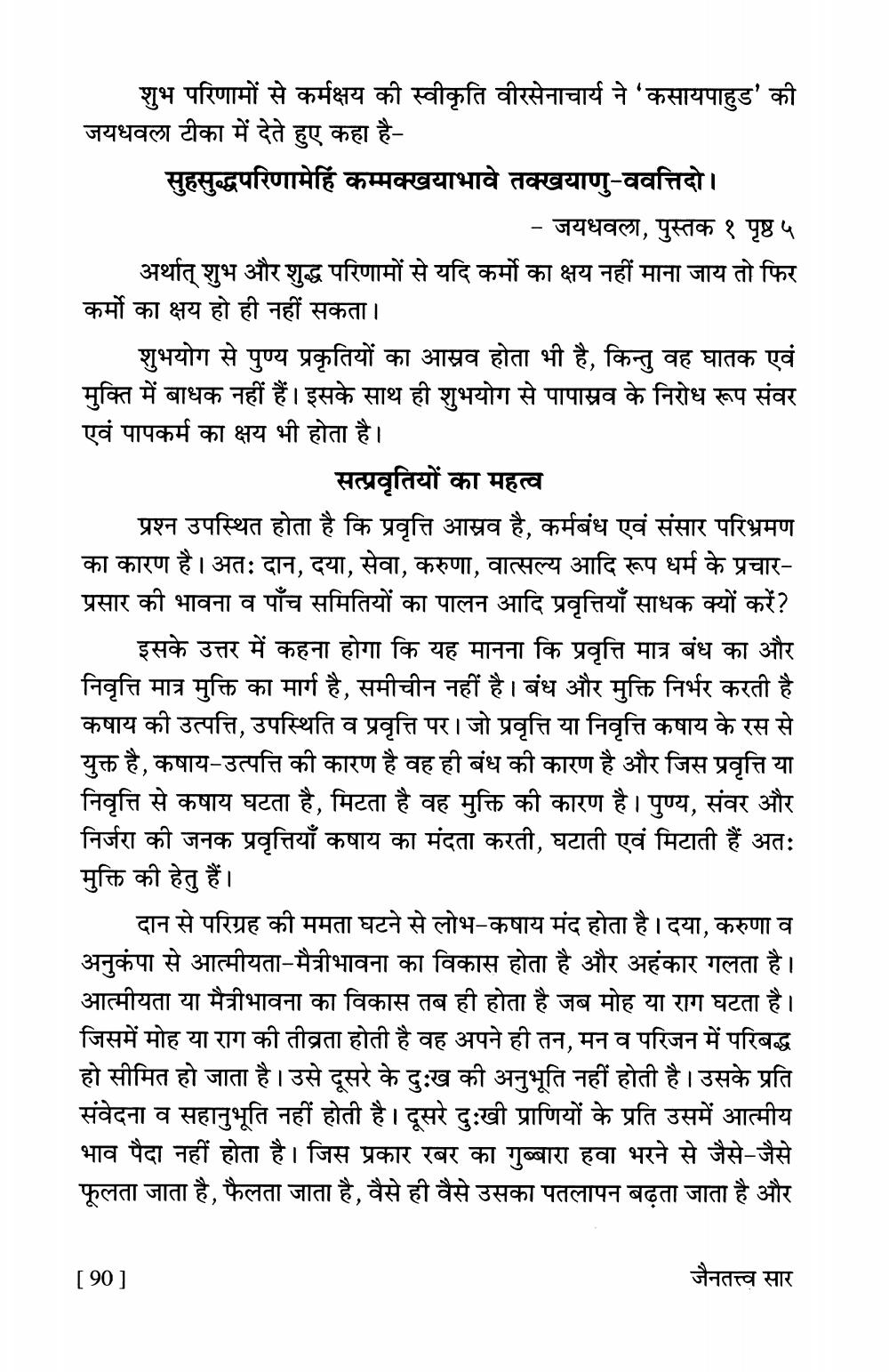________________
शुभ परिणामों से कर्मक्षय की स्वीकृति वीरसेनाचार्य ने 'कसायपाहुड' की जयधवला टीका में देते हुए कहा हैसुहसुद्धपरिणामेहिं कम्मक्खयाभावे तक्खयाणु-ववत्तिदो।
_ - जयधवला, पुस्तक १ पृष्ठ ५ अर्थात् शुभ और शुद्ध परिणामों से यदि कर्मो का क्षय नहीं माना जाय तो फिर कर्मो का क्षय हो ही नहीं सकता।
शभयोग से पुण्य प्रकृतियों का आस्रव होता भी है, किन्तु वह घातक एवं मुक्ति में बाधक नहीं हैं। इसके साथ ही शुभयोग से पापास्रव के निरोध रूप संवर एवं पापकर्म का क्षय भी होता है।
सत्प्रवृतियों का महत्व प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रवृत्ति आस्रव है, कर्मबंध एवं संसार परिभ्रमण का कारण है। अतः दान, दया, सेवा, करुणा, वात्सल्य आदि रूप धर्म के प्रचारप्रसार की भावना व पाँच समितियों का पालन आदि प्रवृत्तियाँ साधक क्यों करें?
इसके उत्तर में कहना होगा कि यह मानना कि प्रवृत्ति मात्र बंध का और निवृत्ति मात्र मुक्ति का मार्ग है, समीचीन नहीं है। बंध और मुक्ति निर्भर करती है कषाय की उत्पत्ति, उपस्थिति व प्रवृत्ति पर। जो प्रवृत्ति या निवृत्ति कषाय के रस से युक्त है, कषाय-उत्पत्ति की कारण है वह ही बंध की कारण है और जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति से कषाय घटता है, मिटता है वह मुक्ति की कारण है। पुण्य, संवर और निर्जरा की जनक प्रवृत्तियाँ कषाय का मंदता करती, घटाती एवं मिटाती हैं अतः मुक्ति की हेतु हैं।
दान से परिग्रह की ममता घटने से लोभ-कषाय मंद होता है। दया, करुणा व अनुकंपा से आत्मीयता-मैत्रीभावना का विकास होता है और अहंकार गलता है। आत्मीयता या मैत्रीभावना का विकास तब ही होता है जब मोह या राग घटता है। जिसमें मोह या राग की तीव्रता होती है वह अपने ही तन, मन व परिजन में परिबद्ध हो सीमित हो जाता है। उसे दूसरे के दुःख की अनुभूति नहीं होती है। उसके प्रति संवेदना व सहानुभूति नहीं होती है। दूसरे दुःखी प्राणियों के प्रति उसमें आत्मीय भाव पैदा नहीं होता है। जिस प्रकार रबर का गुब्बारा हवा भरने से जैसे-जैसे फूलता जाता है, फैलता जाता है, वैसे ही वैसे उसका पतलापन बढ़ता जाता है और
[90]
जैनतत्त्व सार