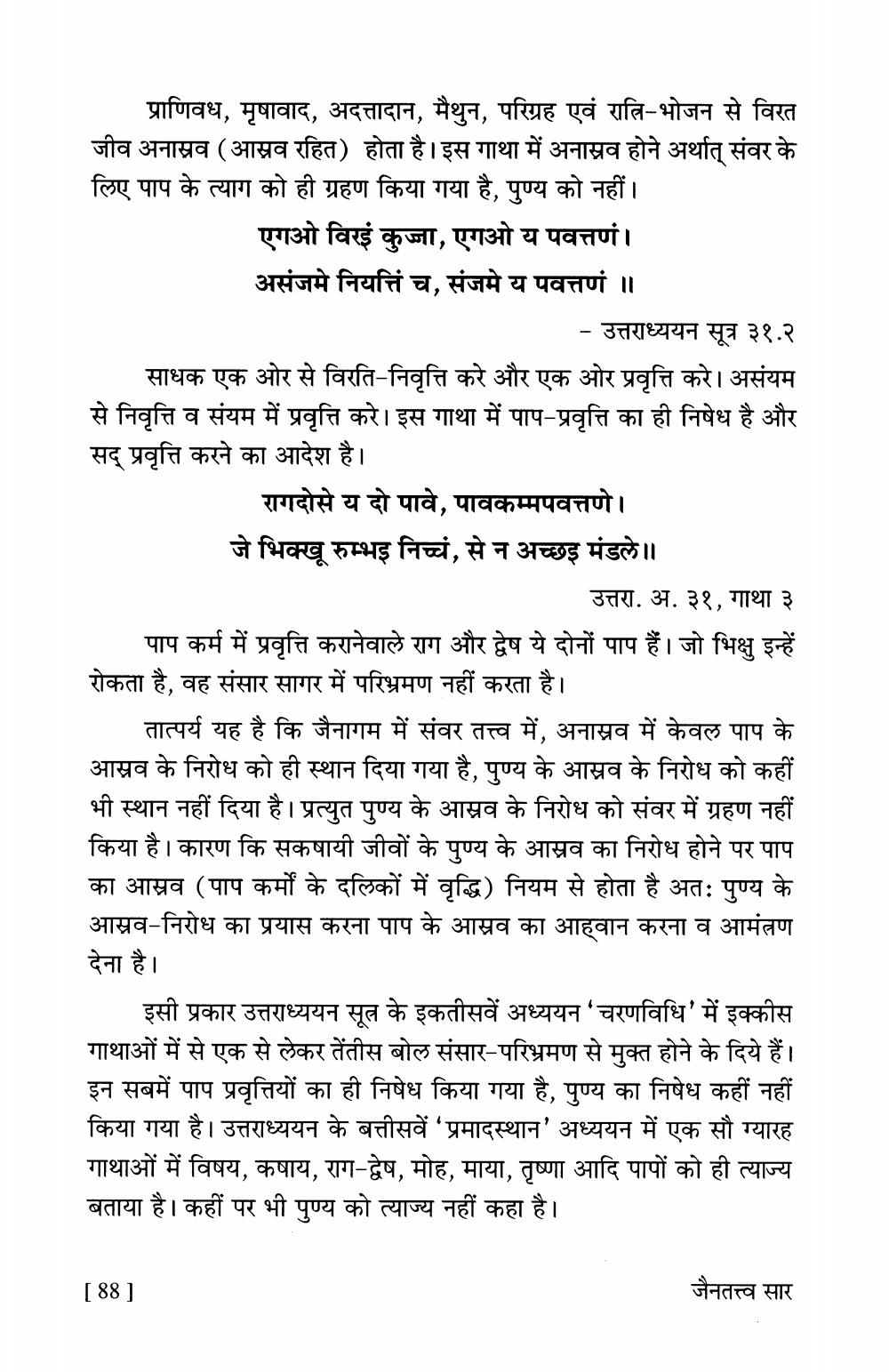________________
प्राणिवध, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह एवं रात्रि-भोजन से विरत जीव अनास्रव (आस्रव रहित) होता है। इस गाथा में अनास्रव होने अर्थात् संवर के लिए पाप के त्याग को ही ग्रहण किया गया है, पुण्य को नहीं।
एगओ विरई कुजा, एगओ य पवत्तणं। असंजमे नियत्तिं च, संजमे य पवत्तणं ॥
- उत्तराध्ययन सूत्र ३१.२ साधक एक ओर से विरति-निवृत्ति करे और एक ओर प्रवृत्ति करे। असंयम से निवृत्ति व संयम में प्रवृत्ति करे। इस गाथा में पाप-प्रवृत्ति का ही निषेध है और सद् प्रवृत्ति करने का आदेश है।
रागदोसे य दो पावे, पावकम्मपवत्तणे। जे भिक्खू रुम्भइ निच्चं, से न अच्छइ मंडले॥
उत्तरा. अ. ३१, गाथा ३ पाप कर्म में प्रवृत्ति करानेवाले राग और द्वेष ये दोनों पाप हैं। जो भिक्ष इन्हें रोकता है, वह संसार सागर में परिभ्रमण नहीं करता है।
तात्पर्य यह है कि जैनागम में संवर तत्त्व में, अनास्रव में केवल पाप के आस्रव के निरोध को ही स्थान दिया गया है, पुण्य के आस्रव के निरोध को कहीं भी स्थान नहीं दिया है। प्रत्युत पुण्य के आस्रव के निरोध को संवर में ग्रहण नहीं किया है। कारण कि सकषायी जीवों के पुण्य के आस्रव का निरोध होने पर पाप का आस्रव (पाप कर्मों के दलिकों में वृद्धि) नियम से होता है अतः पुण्य के आस्रव-निरोध का प्रयास करना पाप के आस्रव का आह्वान करना व आमंत्रण देना है।
इसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र के इकतीसवें अध्ययन 'चरणविधि' में इक्कीस गाथाओं में से एक से लेकर तेंतीस बोल संसार-परिभ्रमण से मुक्त होने के दिये हैं। इन सबमें पाप प्रवृत्तियों का ही निषेध किया गया है, पुण्य का निषेध कहीं नहीं किया गया है। उत्तराध्ययन के बत्तीसवें 'प्रमादस्थान' अध्ययन में एक सौ ग्यारह गाथाओं में विषय, कषाय, राग-द्वेष, मोह, माया, तृष्णा आदि पापों को ही त्याज्य बताया है। कहीं पर भी पुण्य को त्याज्य नहीं कहा है।
[88]
जैनतत्त्व सार