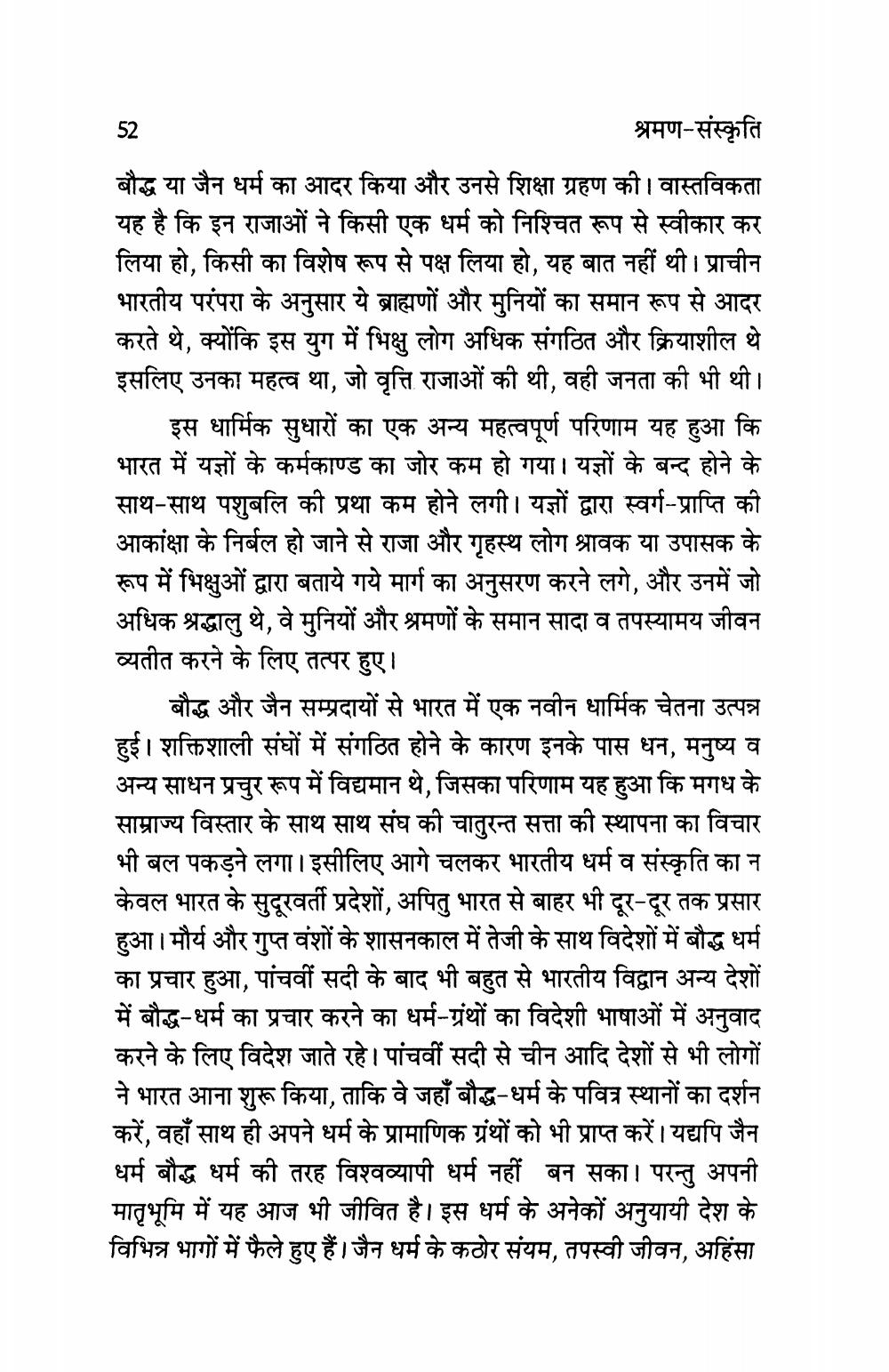________________
श्रमण-संस्कृति बौद्ध या जैन धर्म का आदर किया और उनसे शिक्षा ग्रहण की। वास्तविकता यह है कि इन राजाओं ने किसी एक धर्म को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेष रूप से पक्ष लिया हो, यह बात नहीं थी। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ये ब्राह्मणों और मुनियों का समान रूप से आदर करते थे, क्योंकि इस युग में भिक्षु लोग अधिक संगठित और क्रियाशील थे इसलिए उनका महत्व था, जो वृत्ति राजाओं की थी, वही जनता की भी थी।
इस धार्मिक सुधारों का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि भारत में यज्ञों के कर्मकाण्ड का जोर कम हो गया। यज्ञों के बन्द होने के साथ-साथ पशुबलि की प्रथा कम होने लगी। यज्ञों द्वारा स्वर्ग-प्राप्ति की आकांक्षा के निर्बल हो जाने से राजा और गृहस्थ लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिक्षुओं द्वारा बताये गये मार्ग का अनुसरण करने लगे, और उनमें जो अधिक श्रद्धालु थे, वे मुनियों और श्रमणों के समान सादा व तपस्यामय जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर हुए।
बौद्ध और जैन सम्प्रदायों से भारत में एक नवीन धार्मिक चेतना उत्पन्न हुई। शक्तिशाली संघों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर रूप में विद्यमान थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि मगध के साम्राज्य विस्तार के साथ साथ संघ की चातुरन्त सत्ता की स्थापना का विचार भी बल पकड़ने लगा। इसीलिए आगे चलकर भारतीय धर्म व संस्कृति का न केवल भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों, अपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक प्रसार हुआ। मौर्य और गुप्त वंशों के शासनकाल में तेजी के साथ विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, पांचवीं सदी के बाद भी बहुत से भारतीय विद्वान अन्य देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने का धर्म-ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विदेश जाते रहे। पांचवीं सदी से चीन आदि देशों से भी लोगों ने भारत आना शुरू किया, ताकि वे जहाँ बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों का दर्शन करें, वहाँ साथ ही अपने धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों को भी प्राप्त करें। यद्यपि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तरह विश्वव्यापी धर्म नहीं बन सका। परन्तु अपनी मातृभूमि में यह आज भी जीवित है। इस धर्म के अनेकों अनुयायी देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। जैन धर्म के कठोर संयम, तपस्वी जीवन, अहिंसा