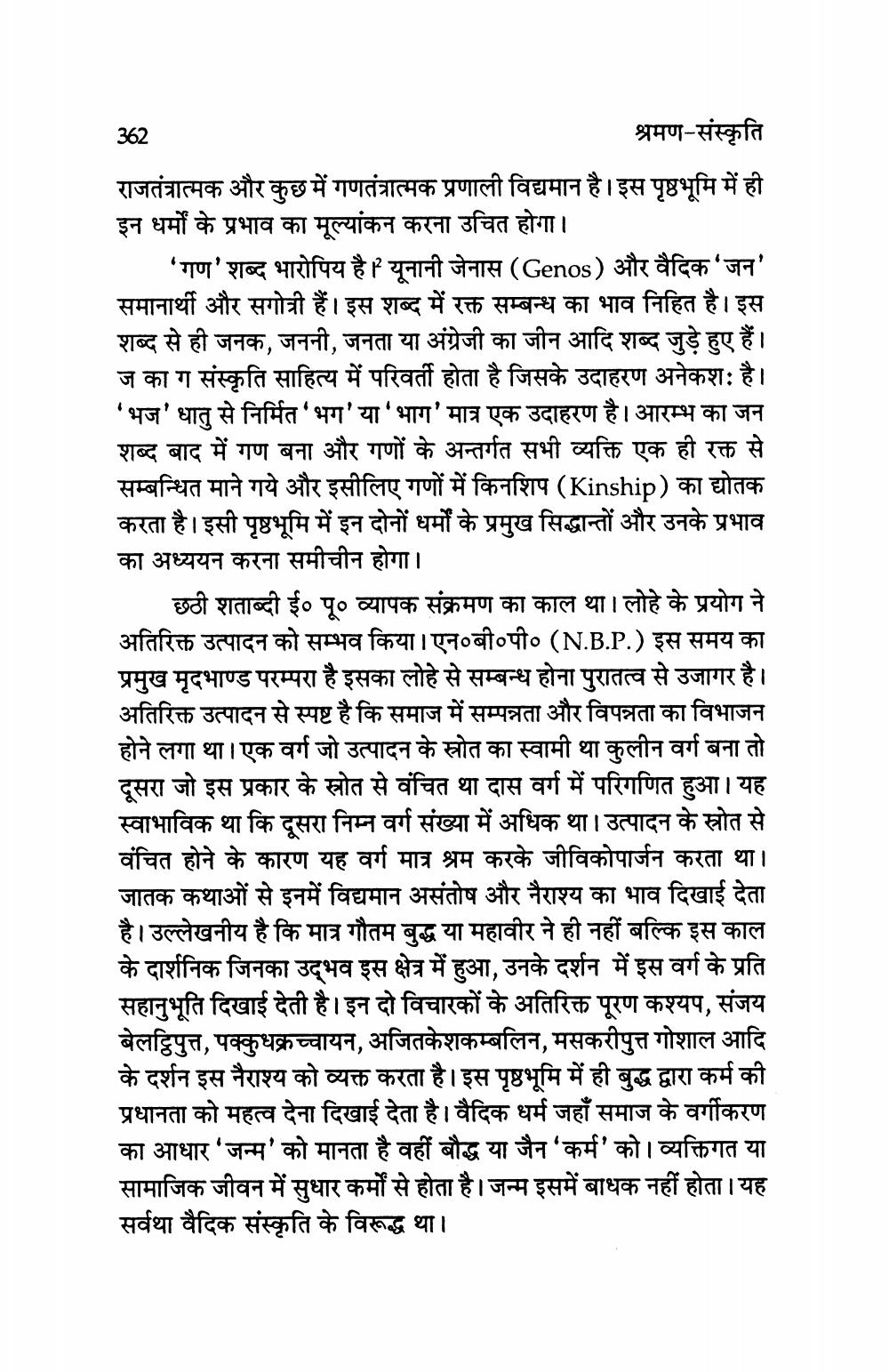________________
श्रमण-संस्कृति
राजतंत्रात्मक और कुछ में गणतंत्रात्मक प्रणाली विद्यमान है। इस पृष्ठभूमि में ही इन धर्मों के प्रभाव का मूल्यांकन करना उचित होगा ।
362
'गण' शब्द भारोपिय है। यूनानी जेनास (Genos ) और वैदिक 'जन' समानार्थी और सगोत्री हैं । इस शब्द में रक्त सम्बन्ध का भाव निहित है । इस शब्द से ही जनक, जननी, जनता या अंग्रेजी का जीन आदि शब्द जुड़े हुए हैं।
का ग संस्कृति साहित्य में परिवर्ती होता है जिसके उदाहरण अनेकश: है । 'भज' धातु से निर्मित ' भग' या 'भाग' मात्र एक उदाहरण है। आरम्भ का जन शब्द बाद में गण बना और गणों के अन्तर्गत सभी व्यक्ति एक ही रक्त से सम्बन्धित माने गये और इसीलिए गणों में किनशिप ( Kinship) का द्योतक करता है। इसी पृष्ठभूमि में इन दोनों धर्मों के प्रमुख सिद्धान्तों और उनके प्रभाव का अध्ययन करना समीचीन होगा।
छठी शताब्दी ई० पू० व्यापक संक्रमण का काल था । लोहे के प्रयोग ने अतिरिक्त उत्पादन को सम्भव किया। एन० बी० पी० (N.B.P.) इस समय का प्रमुख मृदभाण्ड परम्परा है इसका लोहे से सम्बन्ध होना पुरातत्व से उजागर है। अतिरिक्त उत्पादन से स्पष्ट है कि समाज में सम्पन्नता और विपन्नता का विभाजन होने लगा था। एक वर्ग जो उत्पादन के स्रोत का स्वामी था कुलीन वर्ग बना तो दूसरा जो इस प्रकार के स्रोत से वंचित था दास वर्ग में परिगणित हुआ । यह स्वाभाविक था कि दूसरा निम्न वर्ग संख्या में अधिक था । उत्पादन के स्रोत से वंचित होने के कारण यह वर्ग मात्र श्रम करके जीविकोपार्जन करता था । जातक कथाओं से इनमें विद्यमान असंतोष और नैराश्य का भाव दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि मात्र गौतम बुद्ध या महावीर ने ही नहीं बल्कि इस काल के दार्शनिक जिनका उद्भव इस क्षेत्र में हुआ, उनके दर्शन में इस वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। इन दो विचारकों के अतिरिक्त पूरण कश्यप, संजय बेलट्ठिपुत्त, पक्कुधक्रच्चायन, अजितकेशकम्बलिन, मसकरीपुत्त गोशाल आदि के दर्शन इस नैराश्य को व्यक्त करता है । इस पृष्ठभूमि में ही बुद्ध द्वारा कर्म की प्रधानता को महत्व देना दिखाई देता है। वैदिक धर्म जहाँ समाज के वर्गीकरण का आधार 'जन्म' को मानता है वहीं बौद्ध या जैन 'कर्म' को । व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में सुधार कर्मों से होता है। जन्म इसमें बाधक नहीं होता। यह सर्वथा वैदिक संस्कृति के विरूद्ध था ।