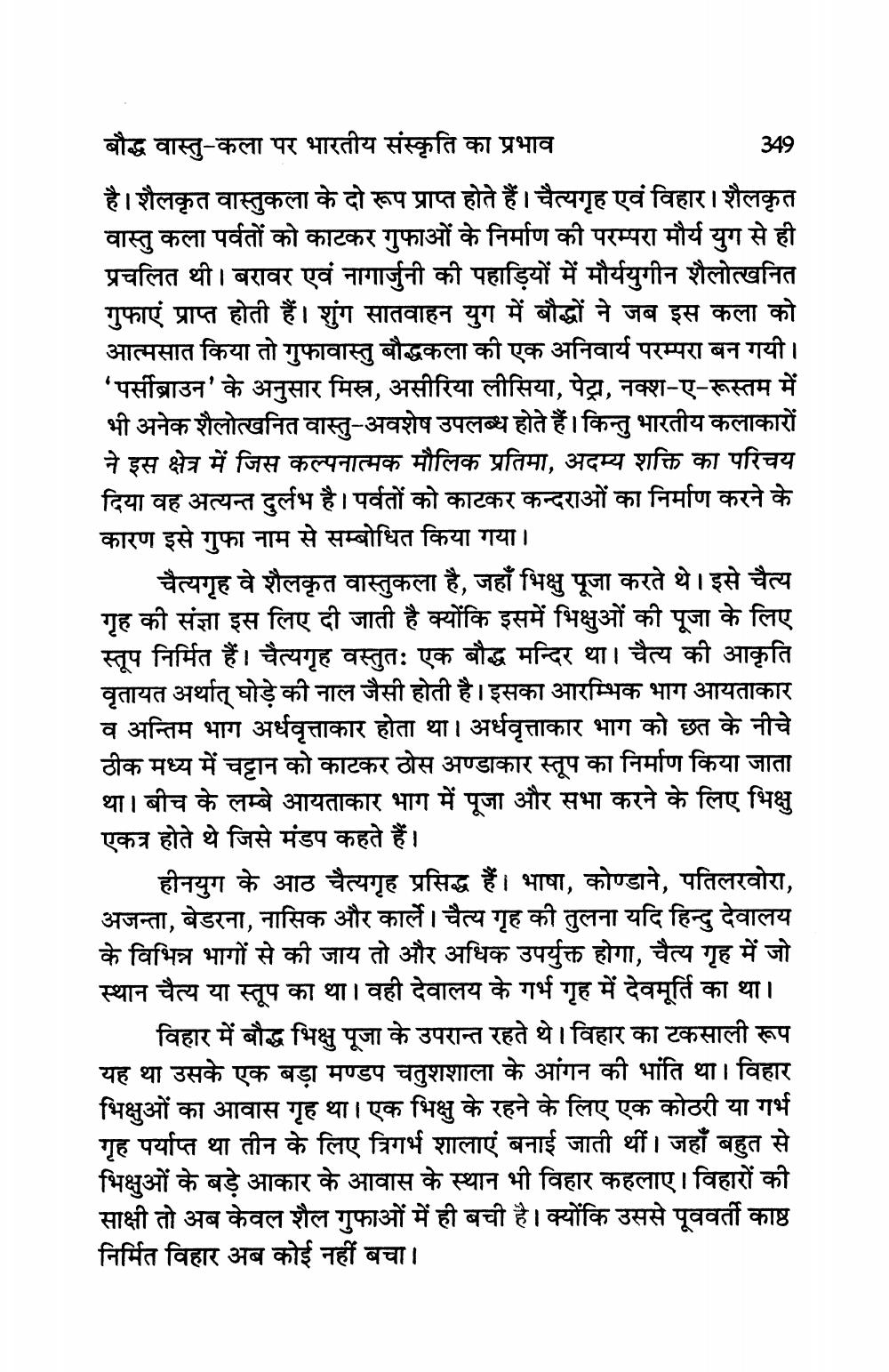________________
बौद्ध वास्तु-कला पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव
349 है। शैलकृत वास्तुकला के दो रूप प्राप्त होते हैं। चैत्यगृह एवं विहार । शैलकृत वास्तु कला पर्वतों को काटकर गुफाओं के निर्माण की परम्परा मौर्य युग से ही प्रचलित थी। बरावर एवं नागार्जुनी की पहाड़ियों में मौर्ययुगीन शैलोत्खनित गुफाएं प्राप्त होती हैं। शुंग सातवाहन युग में बौद्धों ने जब इस कला को आत्मसात किया तो गुफावास्तु बौद्धकला की एक अनिवार्य परम्परा बन गयी। 'पर्सीब्राउन' के अनुसार मिस्त्र, असीरिया लीसिया, पेट्रा, नक्श-ए-रूस्तम में भी अनेक शैलोत्खनित वास्तु-अवशेष उपलब्ध होते हैं। किन्तु भारतीय कलाकारों ने इस क्षेत्र में जिस कल्पनात्मक मौलिक प्रतिमा, अदम्य शक्ति का परिचय दिया वह अत्यन्त दुर्लभ है। पर्वतों को काटकर कन्दराओं का निर्माण करने के कारण इसे गुफा नाम से सम्बोधित किया गया।
चैत्यगृह वे शैलकृत वास्तुकला है, जहाँ भिक्षु पूजा करते थे। इसे चैत्य गृह की संज्ञा इस लिए दी जाती है क्योंकि इसमें भिक्षुओं की पूजा के लिए स्तूप निर्मित हैं। चैत्यगृह वस्तुतः एक बौद्ध मन्दिर था। चैत्य की आकृति वृतायत अर्थात् घोड़े की नाल जैसी होती है। इसका आरम्भिक भाग आयताकार व अन्तिम भाग अर्धवृत्ताकार होता था। अर्धवृत्ताकार भाग को छत के नीचे ठीक मध्य में चट्टान को काटकर ठोस अण्डाकार स्तूप का निर्माण किया जाता था। बीच के लम्बे आयताकार भाग में पूजा और सभा करने के लिए भिक्षु एकत्र होते थे जिसे मंडप कहते हैं।
__ हीनयुग के आठ चैत्यगृह प्रसिद्ध हैं। भाषा, कोण्डाने, पतिलरवोरा, अजन्ता, बेडरना, नासिक और कार्ले । चैत्य गृह की तुलना यदि हिन्दु देवालय के विभिन्न भागों से की जाय तो और अधिक उपर्युक्त होगा, चैत्य गृह में जो स्थान चैत्य या स्तूप का था। वही देवालय के गर्भ गृह में देवमूर्ति का था।
विहार में बौद्ध भिक्षु पूजा के उपरान्त रहते थे। विहार का टकसाली रूप यह था उसके एक बड़ा मण्डप चतुशशाला के आंगन की भांति था। विहार भिक्षुओं का आवास गृह था। एक भिक्षु के रहने के लिए एक कोठरी या गर्भ गृह पर्याप्त था तीन के लिए त्रिगर्भ शालाएं बनाई जाती थीं। जहाँ बहुत से भिक्षुओं के बड़े आकार के आवास के स्थान भी विहार कहलाए। विहारों की साक्षी तो अब केवल शैल गुफाओं में ही बची है। क्योंकि उससे पूर्ववर्ती काष्ठ निर्मित विहार अब कोई नहीं बचा।