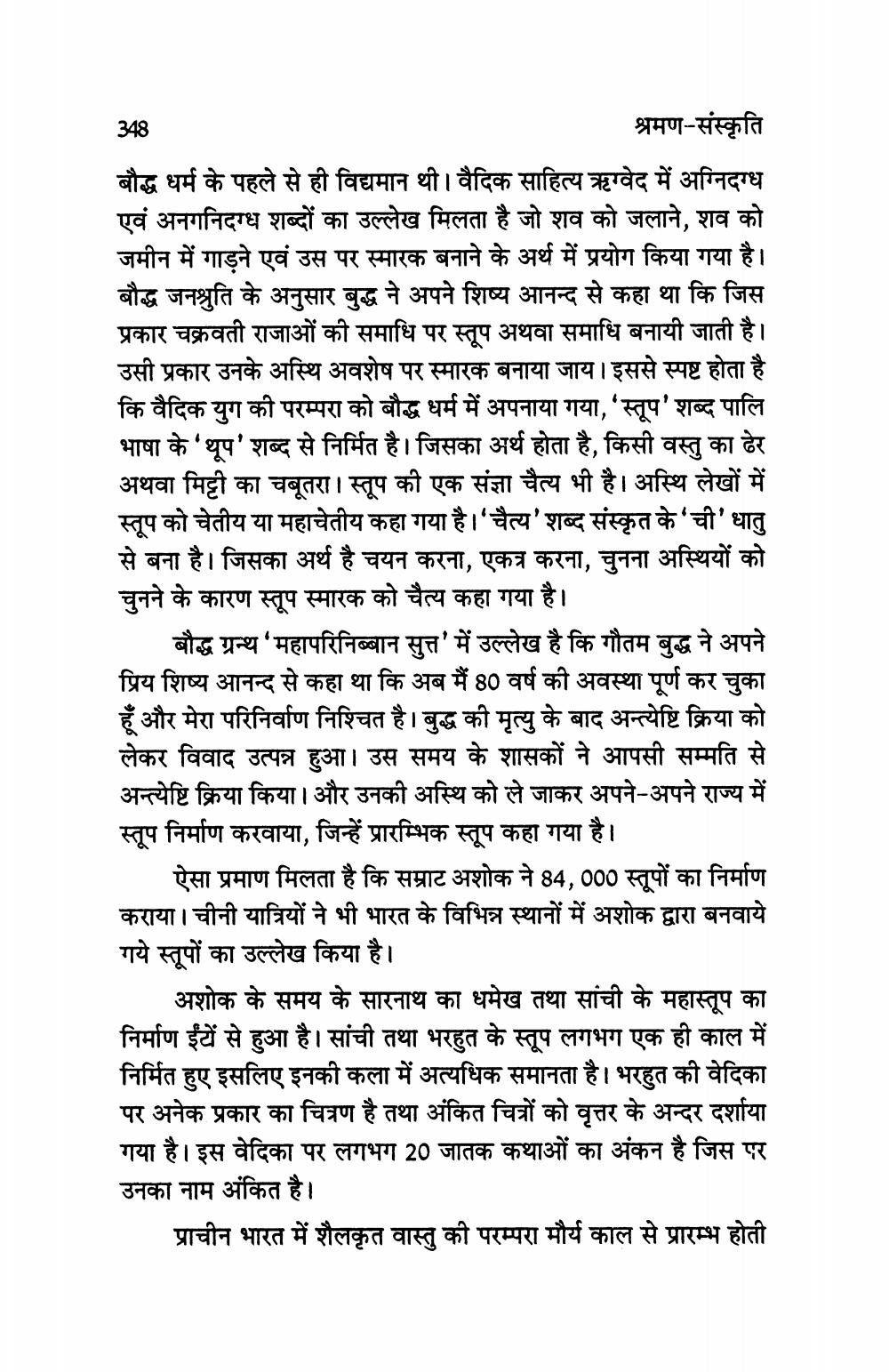________________
348
श्रमण-संस्कृति बौद्ध धर्म के पहले से ही विद्यमान थी। वैदिक साहित्य ऋग्वेद में अग्निदग्ध एवं अनगनिदग्ध शब्दों का उल्लेख मिलता है जो शव को जलाने, शव को जमीन में गाड़ने एवं उस पर स्मारक बनाने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। बौद्ध जनश्रुति के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द से कहा था कि जिस प्रकार चक्रवती राजाओं की समाधि पर स्तूप अथवा समाधि बनायी जाती है। उसी प्रकार उनके अस्थि अवशेष पर स्मारक बनाया जाय। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक युग की परम्परा को बौद्ध धर्म में अपनाया गया, 'स्तूप' शब्द पालि भाषा के 'थूप' शब्द से निर्मित है। जिसका अर्थ होता है, किसी वस्तु का ढेर अथवा मिट्टी का चबूतरा । स्तूप की एक संज्ञा चैत्य भी है। अस्थि लेखों में स्तूप को चेतीय या महाचेतीय कहा गया है। 'चैत्य' शब्द संस्कृत के 'ची' धातु से बना है। जिसका अर्थ है चयन करना, एकत्र करना, चुनना अस्थियों को चुनने के कारण स्तूप स्मारक को चैत्य कहा गया है।
बौद्ध ग्रन्थ 'महापरिनिब्बान सुत्त' में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा था कि अब मैं 80 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर चुका हँ और मेरा परिनिर्वाण निश्चित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद अन्त्येष्टि क्रिया को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उस समय के शासकों ने आपसी सम्मति से अन्त्येष्टि क्रिया किया। और उनकी अस्थि को ले जाकर अपने-अपने राज्य में स्तूप निर्माण करवाया, जिन्हें प्रारम्भिक स्तूप कहा गया है।
ऐसा प्रमाण मिलता है कि सम्राट अशोक ने 84, 000 स्तूपों का निर्माण कराया। चीनी यात्रियों ने भी भारत के विभिन्न स्थानों में अशोक द्वारा बनवाये गये स्तूपों का उल्लेख किया है। ___अशोक के समय के सारनाथ का धमेख तथा सांची के महास्तूप का निर्माण ईंटों से हुआ है। सांची तथा भरहुत के स्तूप लगभग एक ही काल में निर्मित हुए इसलिए इनकी कला में अत्यधिक समानता है। भरहुत की वेदिका पर अनेक प्रकार का चित्रण है तथा अंकित चित्रों को वृत्तर के अन्दर दर्शाया गया है। इस वेदिका पर लगभग 20 जातक कथाओं का अंकन है जिस पर उनका नाम अंकित है।
प्राचीन भारत में शैलकृत वास्तु की परम्परा मौर्य काल से प्रारम्भ होती