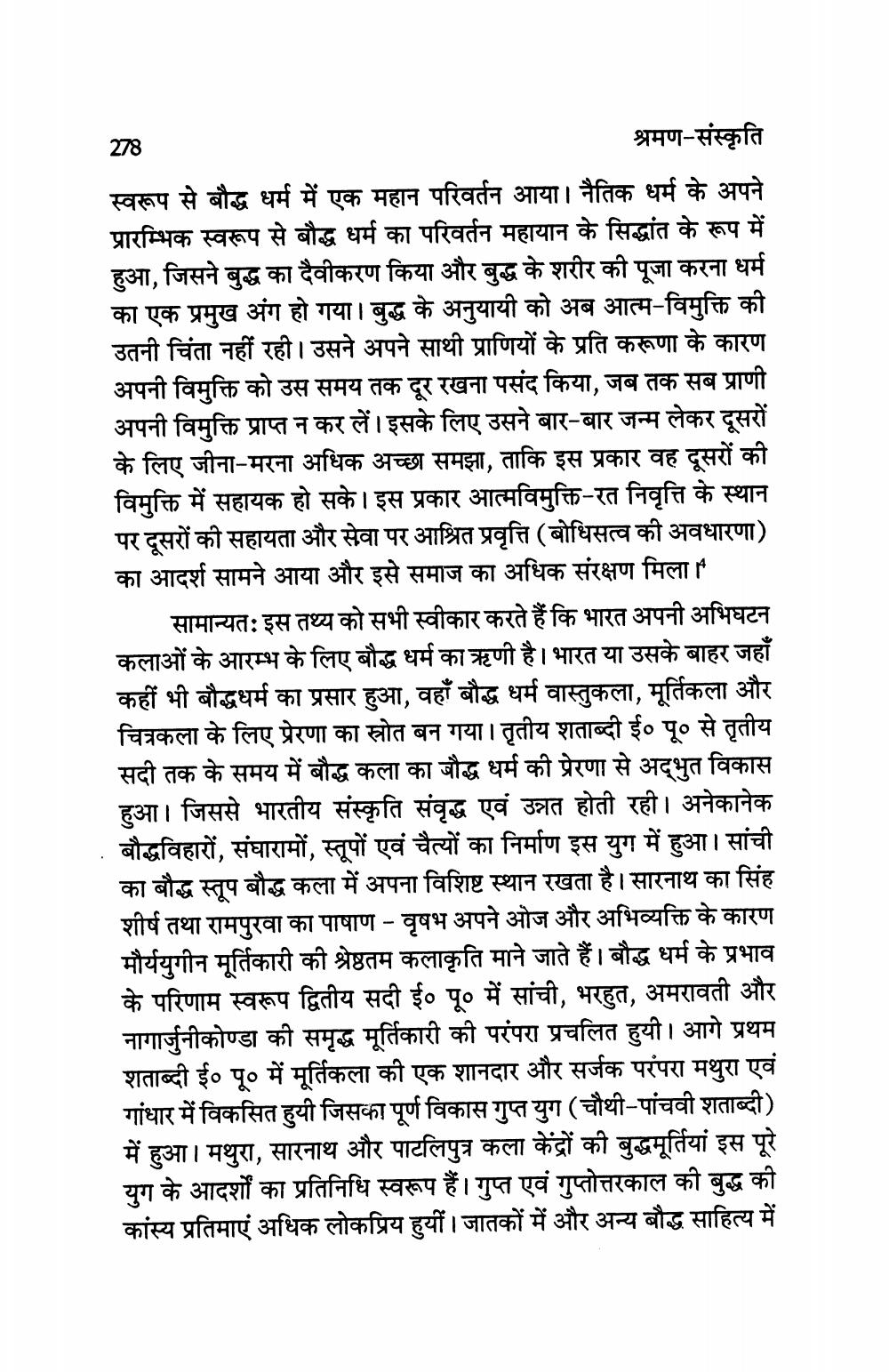________________
श्रमण-संस्कृति
स्वरूप से बौद्ध धर्म में एक महान परिवर्तन आया। नैतिक धर्म के अपने प्रारम्भिक स्वरूप से बौद्ध धर्म का परिवर्तन महायान के सिद्धांत के रूप में हुआ, जिसने बुद्ध का दैवीकरण किया और बुद्ध के शरीर की पूजा करना धर्म का एक प्रमुख अंग हो गया। बुद्ध के अनुयायी को अब आत्म - 1 - विमुक्ति की उतनी चिंता नहीं रही । उसने अपने साथी प्राणियों के प्रति करुणा के कारण अपनी विमुक्ति को उस समय तक दूर रखना पसंद किया, जब तक सब प्राणी अपनी विमुक्ति प्राप्त न कर लें। इसके लिए उसने बार-बार जन्म लेकर दूसरों के लिए जीना मरना अधिक अच्छा समझा, ताकि इस प्रकार वह दूसरों की विमुक्ति में सहायक हो सके। इस प्रकार आत्मविमुक्ति-रत निवृत्ति के स्थान पर दूसरों की सहायता और सेवा पर आश्रित प्रवृत्ति (बोधिसत्व की अवधारणा) का आदर्श सामने आया और इसे समाज का अधिक संरक्षण मिला ।'
278
-
सामान्यतः इस तथ्य को सभी स्वीकार करते हैं कि भारत अपनी अभिघटन कलाओं के आरम्भ के लिए बौद्ध धर्म का ऋणी है। भारत या उसके बाहर जहाँ कहीं भी बौद्धधर्म का प्रसार हुआ, वहाँ बौद्ध धर्म वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया । तृतीय शताब्दी ई० पू० से तृतीय सदी तक के समय में बौद्ध कला का बौद्ध धर्म की प्रेरणा से अद्भुत विकास हुआ। जिससे भारतीय संस्कृति संवृद्ध एवं उन्नत होती रही । अनेकानेक बौद्धविहारों, संघारामों, स्तूपों एवं चैत्यों का निर्माण इस युग में हुआ । सांची
1
बौद्ध स्तूप बौद्ध कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सारनाथ का सिंह शीर्ष तथा रामपुरवा का पाषाण - वृषभ अपने ओज और अभिव्यक्ति के कारण मौर्ययुगीन मूर्तिकारी की श्रेष्ठतम कलाकृति माने जाते हैं । बौद्ध धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप द्वितीय सदी ई० पू० में सांची, भरहुत, अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा की समृद्ध मूर्तिकारी की परंपरा प्रचलित हुयी। आगे प्रथम शताब्दी ई० पू० में मूर्तिकला की एक शानदार और सर्जक परंपरा मथुरा एवं गांधार में विकसित हुयी जिसका पूर्ण विकास गुप्त युग (चौथी - पांचवी शताब्दी) में हुआ। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र कला केंद्रों की बुद्धमूर्तियां इस पूरे युग के आदर्शों का प्रतिनिधि स्वरूप हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तरकाल की बुद्ध की कांस्य प्रतिमाएं अधिक लोकप्रिय हुयीं । जातकों में और अन्य बौद्ध साहित्य में