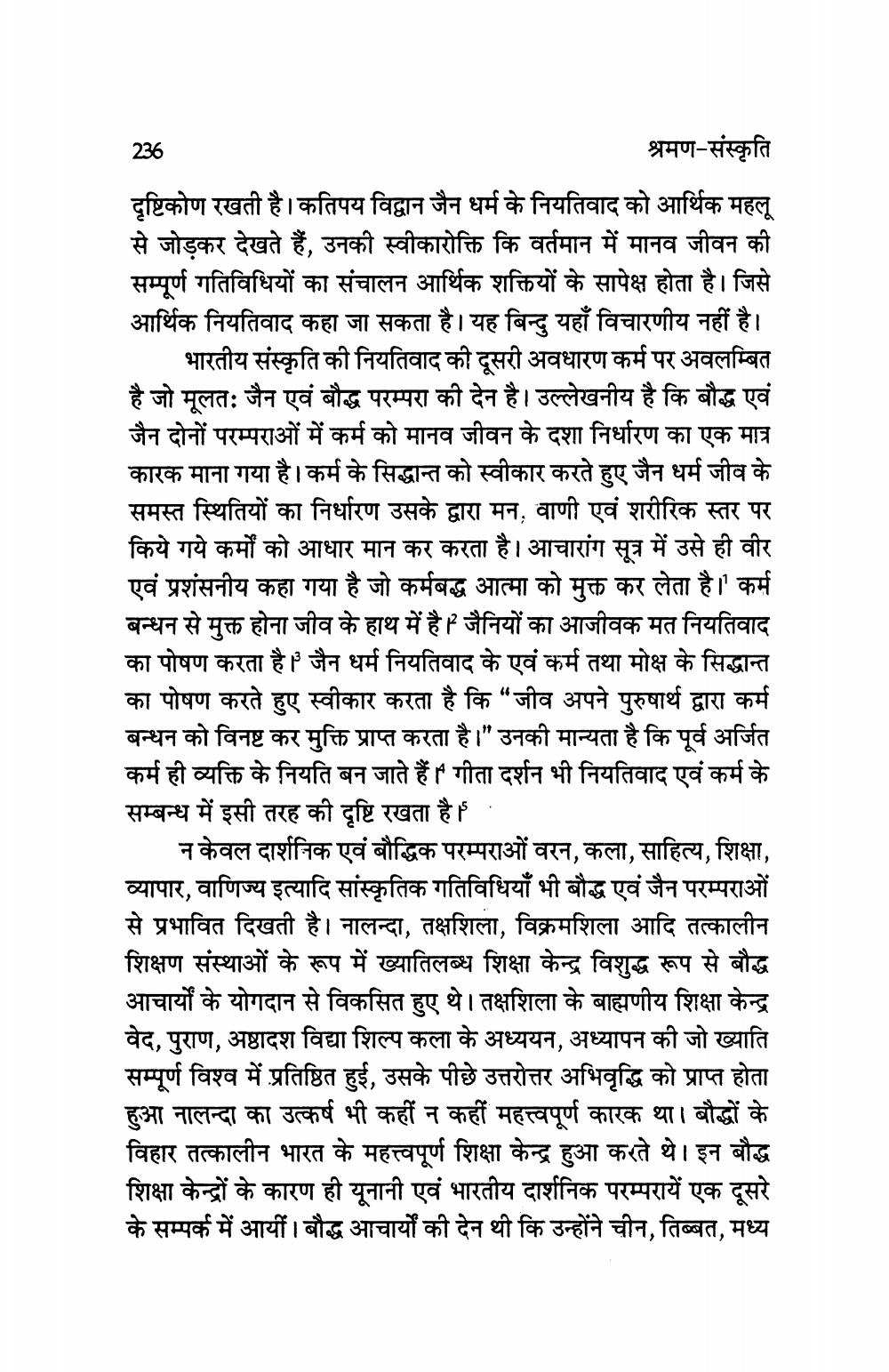________________
236
श्रमण-संस्कृति दृष्टिकोण रखती है। कतिपय विद्वान जैन धर्म के नियतिवाद को आर्थिक महलू से जोड़कर देखते हैं, उनकी स्वीकारोक्ति कि वर्तमान में मानव जीवन की सम्पूर्ण गतिविधियों का संचालन आर्थिक शक्तियों के सापेक्ष होता है। जिसे आर्थिक नियतिवाद कहा जा सकता है। यह बिन्दु यहाँ विचारणीय नहीं है।
भारतीय संस्कृति की नियतिवाद की दूसरी अवधारण कर्म पर अवलम्बित है जो मूलतः जैन एवं बौद्ध परम्परा की देन है। उल्लेखनीय है कि बौद्ध एवं जैन दोनों परम्पराओं में कर्म को मानव जीवन के दशा निर्धारण का एक मात्र कारक माना गया है। कर्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए जैन धर्म जीव के समस्त स्थितियों का निर्धारण उसके द्वारा मन, वाणी एवं शरीरिक स्तर पर किये गये कर्मों को आधार मान कर करता है। आचारांग सूत्र में उसे ही वीर एवं प्रशंसनीय कहा गया है जो कर्मबद्ध आत्मा को मुक्त कर लेता है। कर्म बन्धन से मुक्त होना जीव के हाथ में है। जैनियों का आजीवक मत नियतिवाद का पोषण करता है। जैन धर्म नियतिवाद के एवं कर्म तथा मोक्ष के सिद्धान्त का पोषण करते हुए स्वीकार करता है कि “जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा कर्म बन्धन को विनष्ट कर मुक्ति प्राप्त करता है।" उनकी मान्यता है कि पूर्व अर्जित कर्म ही व्यक्ति के नियति बन जाते हैं। गीता दर्शन भी नियतिवाद एवं कर्म के सम्बन्ध में इसी तरह की दृष्टि रखता है।
न केवल दार्शनिक एवं बौद्धिक परम्पराओं वरन, कला, साहित्य, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी बौद्ध एवं जैन परम्पराओं से प्रभावित दिखती है। नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि तत्कालीन शिक्षण संस्थाओं के रूप में ख्यातिलब्ध शिक्षा केन्द्र विशुद्ध रूप से बौद्ध आचार्यों के योगदान से विकसित हुए थे। तक्षशिला के बाह्मणीय शिक्षा केन्द्र वेद, पुराण, अष्ठादश विद्या शिल्प कला के अध्ययन, अध्यापन की जो ख्याति सम्पूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित हुई, उसके पीछे उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त होता हुआ नालन्दा का उत्कर्ष भी कहीं न कहीं महत्त्वपूर्ण कारक था। बौद्धों के विहार तत्कालीन भारत के महत्त्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र हुआ करते थे। इन बौद्ध शिक्षा केन्द्रों के कारण ही यूनानी एवं भारतीय दार्शनिक परम्परायें एक दूसरे के सम्पर्क में आयीं। बौद्ध आचार्यों की देन थी कि उन्होंने चीन, तिब्बत, मध्य