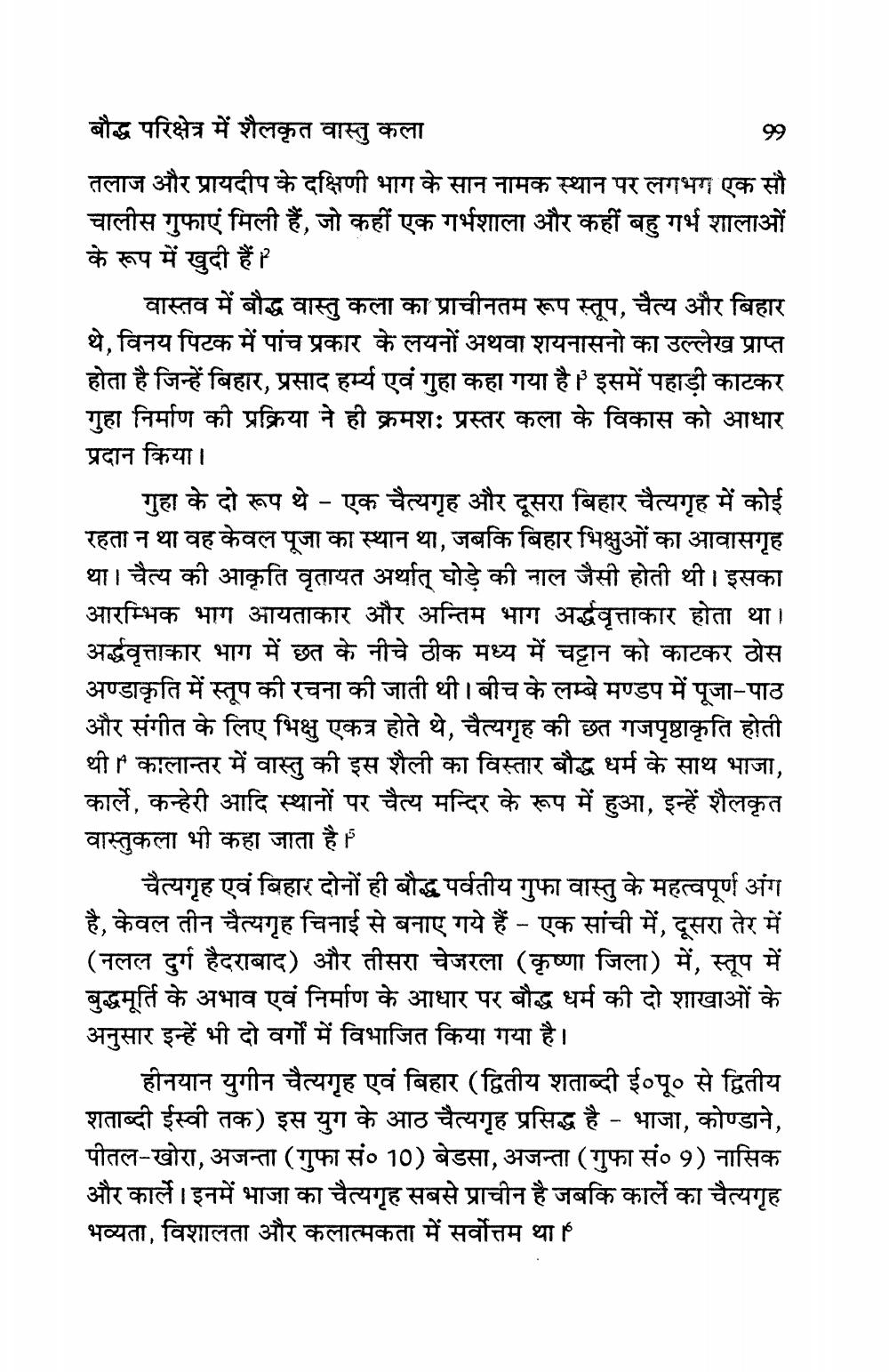________________
बौद्ध परिक्षेत्र में शैलकृत वास्तु कला तलाज और प्रायदीप के दक्षिणी भाग के सान नामक स्थान पर लगभग एक सौ चालीस गुफाएं मिली हैं, जो कहीं एक गर्भशाला और कहीं बहु गर्भ शालाओं के रूप में खुदी हैं।
वास्तव में बौद्ध वास्तु कला का प्राचीनतम रूप स्तूप, चैत्य और बिहार थे, विनय पिटक में पांच प्रकार के लयनों अथवा शयनासनो का उल्लेख प्राप्त होता है जिन्हें बिहार, प्रसाद हर्म्य एवं गुहा कहा गया है। इसमें पहाड़ी काटकर गुहा निर्माण की प्रक्रिया ने ही क्रमशः प्रस्तर कला के विकास को आधार प्रदान किया।
गुहा के दो रूप थे - एक चैत्यगृह और दूसरा बिहार चैत्यगृह में कोई रहता न था वह केवल पूजा का स्थान था, जबकि बिहार भिक्षुओं का आवासगृह था। चैत्य की आकृति वृतायत अर्थात् घोड़े की नाल जैसी होती थी। इसका आरम्भिक भाग आयताकार और अन्तिम भाग अर्द्धवृत्ताकार होता था। अर्द्धवृत्ताकार भाग में छत के नीचे ठीक मध्य में चट्टान को काटकर ठोस अण्डाकृति में स्तूप की रचना की जाती थी। बीच के लम्बे मण्डप में पूजा-पाठ और संगीत के लिए भिक्षु एकत्र होते थे, चैत्यगृह की छत गजपृष्ठाकृति होती थी। कालान्तर में वास्तु की इस शैली का विस्तार बौद्ध धर्म के साथ भाजा, कार्ले, कन्हेरी आदि स्थानों पर चैत्य मन्दिर के रूप में हुआ, इन्हें शैलकृत वास्तुकला भी कहा जाता है।
चैत्यगृह एवं बिहार दोनों ही बौद्ध पर्वतीय गुफा वास्तु के महत्वपूर्ण अंग है, केवल तीन चैत्यगृह चिनाई से बनाए गये हैं - एक सांची में, दूसरा तेर में (नलल दुर्ग हैदराबाद) और तीसरा चेजरला (कृष्णा जिला) में, स्तूप में बुद्धमूर्ति के अभाव एवं निर्माण के आधार पर बौद्ध धर्म की दो शाखाओं के अनुसार इन्हें भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है।
हीनयान युगीन चैत्यगृह एवं बिहार (द्वितीय शताब्दी ई०पू० से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक) इस युग के आठ चैत्यगृह प्रसिद्ध है - भाजा, कोण्डाने, पीतल-खोरा, अजन्ता (गुफा सं० 10) बेडसा, अजन्ता (गुफा सं0 9) नासिक
और कालें । इनमें भाजा का चैत्यगृह सबसे प्राचीन है जबकि काले का चैत्यगृह भव्यता, विशालता और कलात्मकता में सर्वोत्तम था।