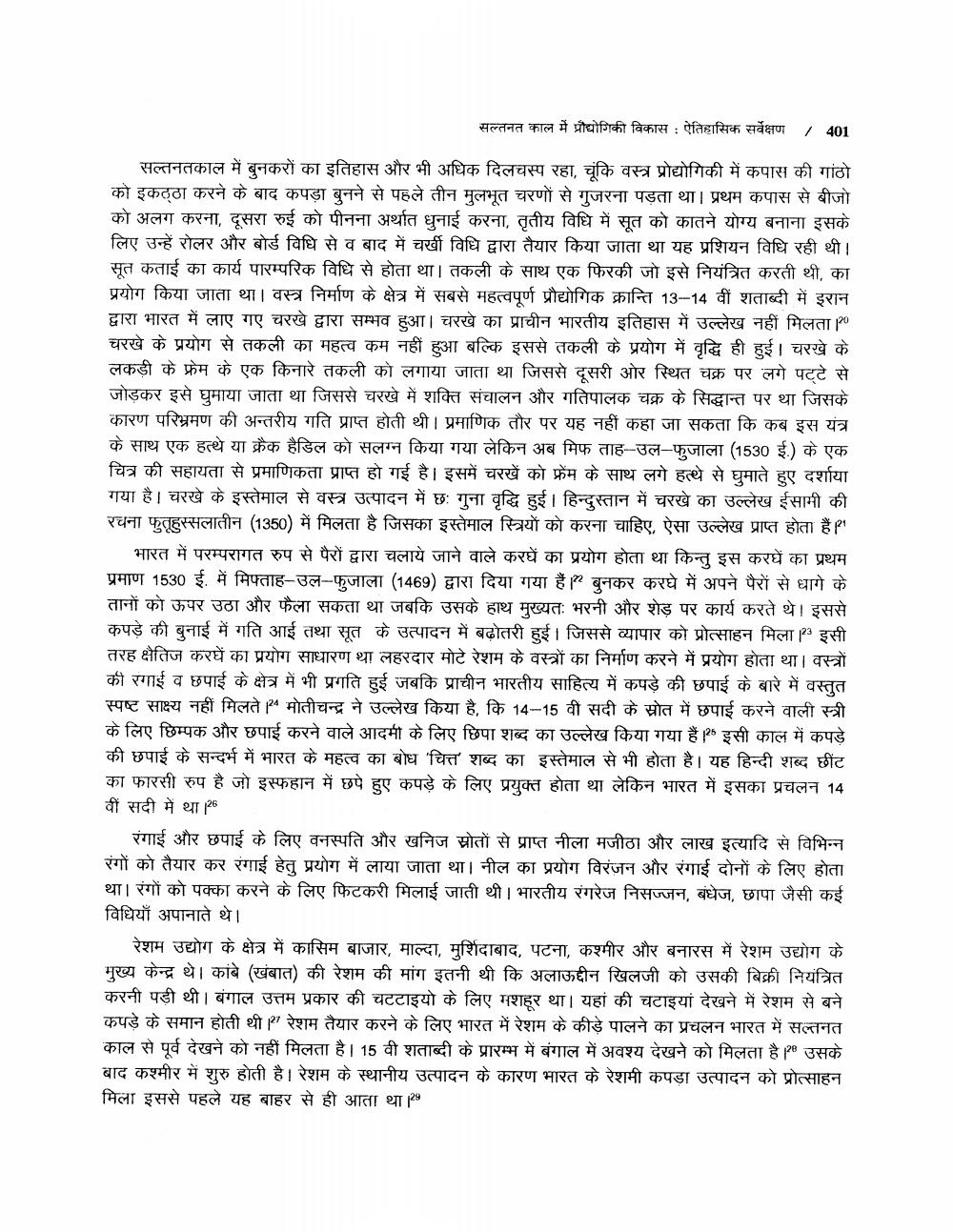________________
सल्तनत काल में प्रौद्योगिकी विकास : ऐतिहासिक सर्वेक्षण / 401
सल्तनतकाल में बुनकरों का इतिहास और भी अधिक दिलचस्प रहा, चूंकि वस्त्र प्रोद्योगिकी में कपास की गांठो को इकट्ठा करने के बाद कपड़ा बुनने से पहले तीन मुलभूत चरणों से गुजरना पड़ता था। प्रथम कपास से बीजो को अलग करना, दूसरा रुई को पीनना अर्थात धुनाई करना, तृतीय विधि में सूत को कातने योग्य बनाना इसके लिए उन्हें रोलर और बोर्ड विधि से व बाद में ची विधि द्वारा तैयार किया जाता था यह प्रशियन विधि रही थी। सूत कताई का कार्य पारम्परिक विधि से होता था। तकली के साथ एक फिरकी जो इसे नियंत्रित करती थी, का प्रयोग किया जाता था। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक क्रान्ति 13-14 वीं शताब्दी में इरान द्वारा भारत में लाए गए चरखे द्वारा सम्भव हुआ। चरखे का प्राचीन भारतीय इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता। चरखे के प्रयोग से तकली का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि इससे तकली के प्रयोग में वृद्धि ही हुई। चरखे के लकड़ी के फ्रेम के एक किनारे तकली को लगाया जाता था जिससे दूसरी ओर स्थित चक्र पर लगे पट्टे से जोड़कर इसे घुमाया जाता था जिससे चरखे में शक्ति संचालन और गतिपालक चक्र के सिद्धान्त पर था जिसके कारण परिभ्रमण की अन्तरीय गति प्राप्त होती थी। प्रमाणिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कब इस यंत्र के साथ एक हत्थे या क्रैक हैडिल को सलग्न किया गया लेकिन अब मिफ ताह-उल-फुजाला (1530 ई.) के एक चित्र की सहायता से प्रमाणिकता प्राप्त हो गई है। इसमें चरखें को फ्रेम के साथ लगे हत्थे से घुमाते हुए दर्शाया गया है। चरखे के इस्तेमाल से वस्त्र उत्पादन में छ: गुना वृद्धि हुई। हिन्दुस्तान में चरखे का उल्लेख ईसामी की रचना फुतूहुस्सलातीन (1350) में मिलता है जिसका इस्तेमाल स्त्रियों को करना चाहिए, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता हैं।
भारत में परम्परागत रुप से पैरों द्वारा चलाये जाने वाले करघे का प्रयोग होता था किन्तु इस करघे का प्रथम प्रमाण 1530 ई. में मिफ्ताह-उल-फुजाला (1469) द्वारा दिया गया हैं। बुनकर करघे में अपने पैरों से धागे के तानों को ऊपर उठा और फैला सकता था जबकि उसके हाथ मुख्यतः भरनी और शेड़ पर कार्य करते थे। इससे कपड़े की बुनाई में गति आई तथा सूत के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इसी तरह क्षैतिज करघे का प्रयोग साधारण था लहरदार मोटे रेशम के वस्त्रों का निर्माण करने में प्रयोग होता था। वस्त्रों की रंगाई व छपाई के क्षेत्र में भी प्रगति हुई जबकि प्राचीन भारतीय साहित्य में कपड़े की छपाई के बारे में वस्तुत स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। मोतीचन्द्र ने उल्लेख किया है, कि 14-15 वीं सदी के स्रोत में छपाई करने वाली स्त्री के लिए छिम्पक और छपाई करने वाले आदमी के लिए छिपा शब्द का उल्लेख किया गया हैं। इसी काल में कपड़े की छपाई के सन्दर्भ में भारत के महत्व का बोध 'चित्त' शब्द का इस्तेमाल से भी होता है। यह हिन्दी शब्द छींट का फारसी रुप है जो इस्फहान में छपे हुए कपड़े के लिए प्रयुक्त होता था लेकिन भारत में इसका प्रचलन 14 वीं सदी में था
रंगाई और छपाई के लिए वनस्पति और खनिज स्रोतों से प्राप्त नीला मजीठा और लाख इत्यादि से विभिन्न रंगों को तैयार कर रंगाई हेतु प्रयोग में लाया जाता था। नील का प्रयोग विरंजन और रंगाई दोनों के लिए होता था। रंगों को पक्का करने के लिए फिटकरी मिलाई जाती थी। भारतीय रंगरेज निसज्जन, बंधेज, छापा जैसी कई विधियाँ अपानाते थे।
रेशम उद्योग के क्षेत्र में कासिम बाजार, माल्दा, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर और बनारस में रेशम उद्योग के मुख्य केन्द्र थे। कांबे (खंबात) की रेशम की मांग इतनी थी कि अलाऊद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी थी। बंगाल उत्तम प्रकार की चटटाइयो के लिए मशहूर था। यहां की चटाइयां देखने में रेशम से बने कपड़े के समान होती थी।" रेशम तैयार करने के लिए भारत में रेशम के कीड़े पालने का प्रचलन भारत में सल्तनत काल से पूर्व देखने को नहीं मिलता है। 15 वी शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल में अवश्य देखने को मिलता है। उसके बाद कश्मीर में शुरु होती है। रेशम के स्थानीय उत्पादन के कारण भारत के रेशमी कपड़ा उत्पादन को प्रोत्साहन मिला इससे पहले यह बाहर से ही आता था।