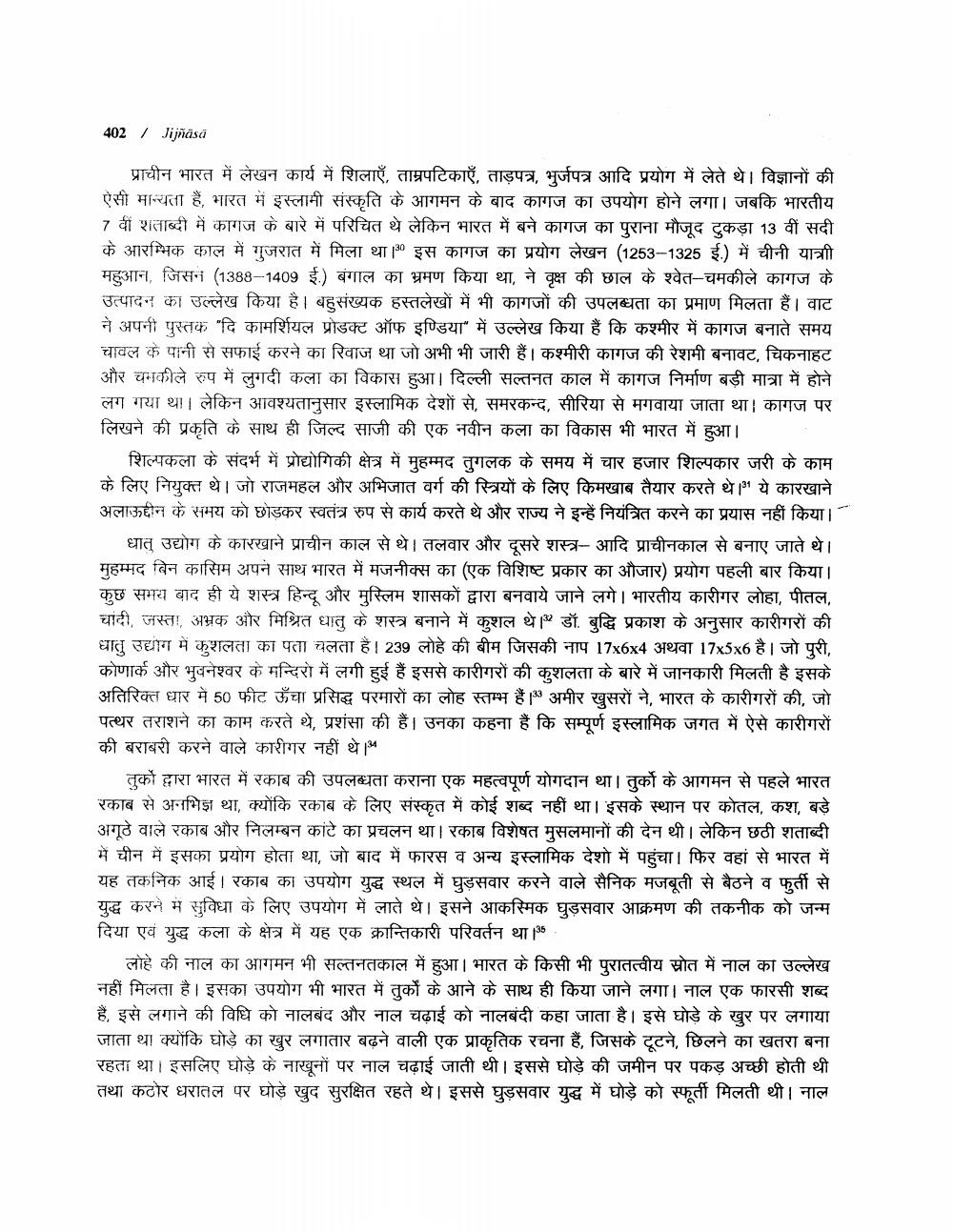________________
402
Jijñäsä
प्राचीन भारत में लेखन कार्य में शिलाएँ, ताम्रपटिकाएँ, ताड़पत्र, भुर्जपत्र आदि प्रयोग में लेते थे। विज्ञानों की ऐसी मान्यता हैं, भारत में इस्लामी संस्कृति के आगमन के बाद कागज का उपयोग होने लगा। जबकि भारतीय 7 वीं शताब्दी में कागज के बारे में परिचित थे लेकिन भारत में बने कागज का पुराना मौजूद टुकड़ा 13 वीं सदी के आरम्भिक काल में गुजरात में मिला था। इस कागज का प्रयोग लेखन (1253-1325 ई.) में चीनी यात्री महुआन, जिसने (1388-1409 ई.) बंगाल का भ्रमण किया था, ने वृक्ष की छाल के श्वेत-चमकीले कागज के उत्पादन का उल्लेख किया है। बहुसंख्यक हस्तलेखों में भी कागजों की उपलब्धता का प्रमाण मिलता हैं। वाट ने अपनी पुस्तक "दि कामर्शियल प्रोडक्ट ऑफ इण्डिया' में उल्लेख किया हैं कि कश्मीर में कागज बनाते समय चावल के पानी से सफाई करने का रिवाज था जो अभी भी जारी हैं। कश्मीरी कागज की रेशमी बनावट, चिकनाहट और चमकीले रुप में लुगदी कला का विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत काल में कागज निर्माण बड़ी मात्रा में होने लग गया था। लेकिन आवश्यतानुसार इस्लामिक देशों से, समरकन्द, सीरिया से मगवाया जाता था। कागज पर लिखने की प्रकृति के साथ ही जिल्द साजी की एक नवीन कला का विकास भी भारत में हुआ।
शिल्पकला के संदर्भ में प्रोद्योगिकी क्षेत्र में मुहम्मद तुगलक के समय में चार हजार शिल्पकार जरी के काम के लिए नियुक्त थे। जो राजमहल और अभिजात वर्ग की स्त्रियों के लिए किमखाब तैयार करते थे। ये कारखाने अलाऊद्दीन के समय को छोड़कर स्वतंत्र रुप से कार्य करते थे और राज्य ने इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया।
धातु उद्योग के कारखाने प्राचीन काल से थे। तलवार और दूसरे शस्त्र-आदि प्राचीनकाल से बनाए जाते थे। मुहम्मद बिन कासिम अपने साथ भारत में मजनीक्स का (एक विशिष्ट प्रकार का औजार) प्रयोग पहली बार किया। कुछ समय बाद ही ये शस्त्र हिन्दू और मुस्लिम शासकों द्वारा बनवाये जाने लगे। भारतीय कारीगर लोहा, पीतल, चांदी, जस्ता, अभ्रक और मिश्रित धातु के शस्त्र बनाने में कुशल थे। डॉ. बुद्धि प्रकाश के अनुसार कारीगरों की धातु उद्योग में कुशलता का पता चलता है। 239 लोहे की बीम जिसकी नाप 17x6x4 अथवा 17x5x6 है। जो पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर के मन्दिरो में लगी हुई हैं इससे कारीगरों की कुशलता के बारे में जानकारी मिलती है इसके अतिरिक्त धार में 50 फीट ऊँचा प्रसिद्ध परमारों का लोह स्तम्भ हैं। अमीर खुसरों ने, भारत के कारीगरों की, जो पत्थर तराशने का काम करते थे, प्रशंसा की हैं। उनका कहना हैं कि सम्पूर्ण इस्लामिक जगत में ऐसे कारीगरों की बराबरी करने वाले कारीगर नहीं थे।
तुर्को द्वारा भारत में रकाब की उपलब्धता कराना एक महत्वपूर्ण योगदान था। तुर्को के आगमन से पहले भारत रकाब से अनभिज्ञ था, क्योंकि रकाब के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं था। इसके स्थान पर कोतल, कश, बड़े अगूठे वाले रकाब और निलम्बन कांटे का प्रचलन था। रकाब विशेषत मुसलमानों की देन थी। लेकिन छठी शताब्दी में चीन में इसका प्रयोग होता था, जो बाद में फारस व अन्य इस्लामिक देशो में पहुंचा। फिर वहां से भारत में यह तकनिक आई। रकाब का उपयोग युद्ध स्थल में घुड़सवार करने वाले सैनिक मजबूती से बैठने व फुर्ती से युद्ध करने में सुविधा के लिए उपयोग में लाते थे। इसने आकस्मिक घुड़सवार आक्रमण की तकनीक को जन्म दिया एवं युद्ध कला के क्षेत्र में यह एक क्रान्तिकारी परिवर्तन था।3.
लोहे की नाल का आगमन भी सल्तनतकाल में हुआ। भारत के किसी भी पुरातत्वीय स्रोत में नाल का उल्लेख नहीं मिलता है। इसका उपयोग भी भारत में तुर्कों के आने के साथ ही किया जाने लगा। नाल एक फारसी शब्द हैं, इसे लगाने की विधि को नालबंद और नाल चढ़ाई को नालबंदी कहा जाता है। इसे घोड़े के खुर पर लगाया जाता था क्योंकि घोड़े का खुर लगातार बढ़ने वाली एक प्राकृतिक रचना हैं, जिसके टूटने, छिलने का खतरा बना रहता था। इसलिए घोड़े के नाखूनों पर नाल चढ़ाई जाती थी। इससे घोड़े की जमीन पर पकड़ अच्छी होती थी तथा कटोर धरातल पर घोड़े खुद सुरक्षित रहते थे। इससे घुड़सवार युद्ध में घोड़े को स्फूर्ती मिलती थी। नाल