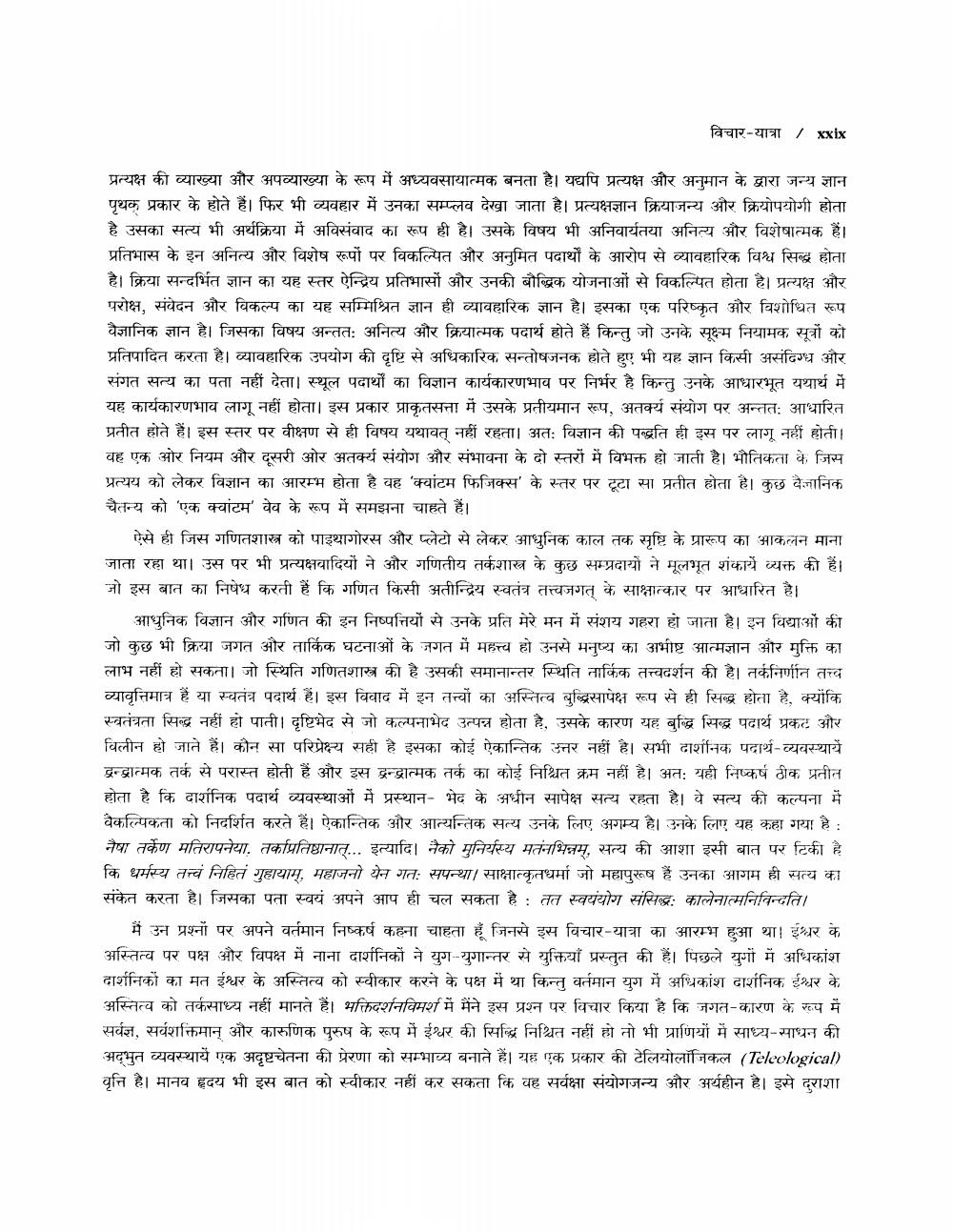________________
विचार-यात्रा / xxix
प्रत्यक्ष की व्याख्या और अपव्याख्या के रूप में अध्यवसायात्मक बनता है। यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जन्य ज्ञान पृथक प्रकार के होते हैं। फिर भी व्यवहार में उनका सम्प्लव देखा जाता है। प्रत्यक्षज्ञान क्रियाजन्य और क्रियोपयोगी होता है उसका सत्य भी अर्थक्रिया में अविसंवाद का रूप ही है। उसके विषय भी अनिवार्यतया अनित्य और विशेषात्मक हैं। प्रतिभास के इन अनित्य और विशेष रूपों पर विकल्पित और अनुमित पदार्थों के आरोप से व्यावहारिक विश्व सिद्ध होता है। क्रिया सन्दर्भित ज्ञान का यह स्तर ऐन्द्रिय प्रतिभासों और उनकी बौद्धिक योजनाओं से विकल्पित होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, संवेदन और विकल्प का यह सम्मिश्रित ज्ञान ही व्यावहारिक ज्ञान है। इसका एक परिष्कृत और विशोधित रूप वैज्ञानिक ज्ञान है। जिसका विषय अन्ततः अनित्य और क्रियात्मक पदार्थ होते हैं किन्तु जो उनके सूक्ष्म नियामक सूत्रों को प्रतिपादित करता है। व्यावहारिक उपयोग की दृष्टि से अधिकारिक सन्तोषजनक होते हुए भी यह ज्ञान किसी असंदिग्ध और संगत सत्य का पता नहीं देता। स्थूल पदार्थों का विज्ञान कार्यकारणभाव पर निर्भर है किन्तु उनके आधारभूत यथार्थ में यह कार्यकारणभाव लागू नहीं होता। इस प्रकार प्राकृतसत्ता में उसके प्रतीयमान रूप, अतयं संयोग पर अन्तत: आधारित प्रतीत होते हैं। इस स्तर पर वीक्षण से ही विषय यथावत् नहीं रहता। अत: विज्ञान की पद्धति ही इस पर लागू नहीं होती। वह एक ओर नियम और दूसरी ओर अतयं संयोग और संभावना के दो स्तरों में विभक्त हो जाती है। भौतिकता के जिस प्रत्यय को लेकर विज्ञान का आरम्भ होता है वह 'क्वांटम फिजिक्स' के स्तर पर टूटा सा प्रतीत होता है। कुछ वैज्ञानिक चैतन्य को 'एक क्वांटम' वेव के रूप में समझना चाहते हैं।
ऐसे ही जिस गणितशास्त्र को पाइथागोरस और प्लेटो से लेकर आधुनिक काल तक सृष्टि के प्रारूप का आकलन माना जाता रहा था। उस पर भी प्रत्यक्षवादियों ने और गणितीय तर्कशास्त्र के कुछ सम्प्रदायों ने मूलभूत शंकायें व्यक्त की है। जो इस बात का निषेध करती हैं कि गणित किसी अतीन्द्रिय स्वतंत्र तत्त्वजगत् के साक्षात्कार पर आधारित है।
आधुनिक विज्ञान और गणित की इन निष्पत्तियों से उनके प्रति मेरे मन में संशय गहरा हो जाता है। इन विद्याओं की जो कुछ भी क्रिया जगत और तार्किक घटनाओं के जगत में महत्त्व हो उनसे मनुष्य का अभीष्ट आत्मज्ञान और मुक्ति का लाभ नहीं हो सकता। जो स्थिति गणितशास्त्र की है उसकी समानान्तर स्थिति तार्किक तत्त्वदर्शन की है। तर्कनिर्णीत तत्त्व व्यावृत्तिमात्र हैं या स्वतंत्र पदार्थ हैं। इस विवाद में इन तत्त्वों का अस्तित्व बुद्धिसापेक्ष रूप से ही सिद्ध होता है, क्योंकि स्वतंत्रता सिद्ध नहीं हो पाती। दृष्टिभेद से जो कल्पनाभेद उत्पन्न होता है, उसके कारण यह बुद्धि सिद्ध पदार्थ प्रकट और विलीन हो जाते हैं। कौन सा परिप्रेक्ष्य सही है इसका कोई ऐकान्तिक उत्तर नहीं है। सभी दार्शनिक पदार्थ-व्यवस्थायें द्वन्द्वात्मक तर्क से परास्त होती हैं और इस द्वन्द्वात्मक तर्क का कोई निश्चित क्रम नहीं है। अत: यही निष्कर्ष ठीक प्रतीत होता है कि दार्शनिक पदार्थ व्यवस्थाओं में प्रस्थान- भेद के अधीन सापेक्ष सत्य रहता है। वे सत्य की कल्पना में वैकल्पिकता को निदर्शित करते हैं। ऐकान्तिक और आत्यन्तिक सत्य उनके लिए अगम्य है। उनके लिए यह कहा गया है : नैषा तर्केण मतिरापनेया. तर्काप्रतिष्ठानात्... इत्यादि। नैको मुनिर्यस्य मतंन भिन्नम्, सत्य की आशा इसी बात पर टिकी है कि धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्, महाजनो येन गतः सपन्था। साक्षात्कृतधर्मा जो महापुरूष हैं उनका आगम ही सत्य का संकेत करता है। जिसका पता स्वयं अपने आप ही चल सकता है : तत स्वयंयोग संसिद्ध: कालेनात्मनिविन्दति।
मैं उन प्रश्नों पर अपने वर्तमान निष्कर्ष कहना चाहता हूँ जिनसे इस विचार-यात्रा का आरम्भ हुआ था। ईश्वर के अस्तित्व पर पक्ष और विपक्ष में नाना दार्शनिकों ने युग-युगान्तर से युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। पिछले युगों में अधिकांश दार्शनिकों का मत ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने के पक्ष में था किन्तु वर्तमान युग में अधिकांश दार्शनिक ईश्वर के अस्तित्व को तर्कसाध्य नहीं मानते हैं। भक्तिदर्शनविमर्श में मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है कि जगत-कारण के रूप में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और कारुणिक पुरुष के रूप में ईश्वर की सिद्धि निश्चित नहीं हो तो भी प्राणियों में साध्य-साधन की अद्भुत व्यवस्थायें एक अदृष्टचेतना की प्रेरणा को सम्भाव्य बनाते हैं। यह एक प्रकार की टेलियोलॉजिकल (Teleological) वृत्ति है। मानव हृदय भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि वह सर्वक्षा संयोगजन्य और अर्थहीन है। इसे दुराशा