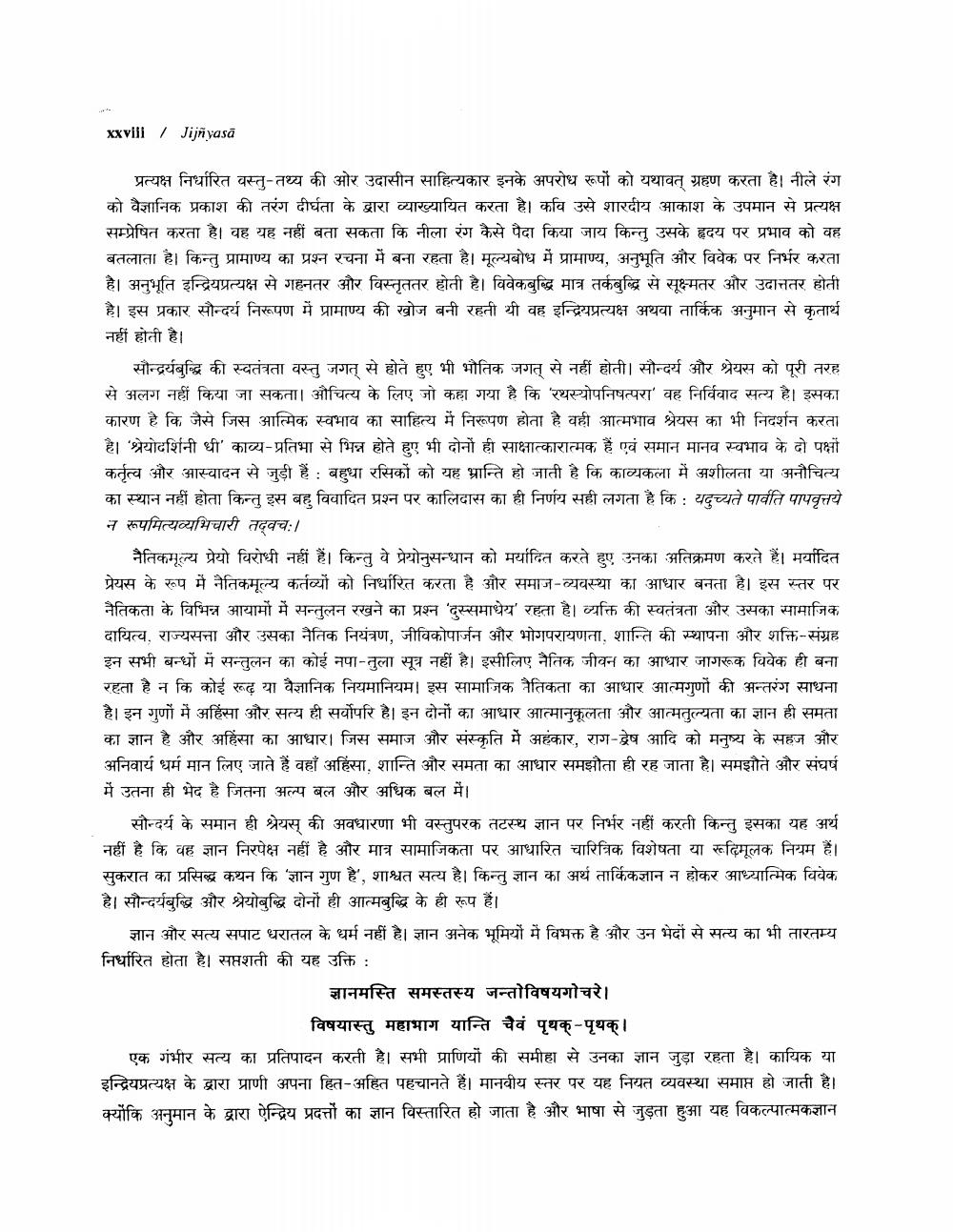________________
xxvili /
Jijnyasa
प्रत्यक्ष निर्धारित वस्तु-तथ्य की ओर उदासीन साहित्यकार इनके अपरोध रूपों को यथावत् ग्रहण करता है। नीले रंग को वैज्ञानिक प्रकाश की तरंग दीर्घता के द्वारा व्याख्यायित करता है। कवि उसे शारदीय आकाश के उपमान से प्रत्यक्ष सम्प्रेषित करता है। वह यह नहीं बता सकता कि नीला रंग कैसे पैदा किया जाय किन्तु उसके हृदय पर प्रभाव को वह बतलाता है। किन्तु प्रामाण्य का प्रश्न रचना में बना रहता है। मूल्यबोध में प्रामाण्य, अनुभूति और विवेक पर निर्भर करता है। अनुभूति इन्द्रियप्रत्यक्ष से गहनतर और विस्तृततर होती है। विवेकबुद्धि मात्र तर्कबुद्धि से सूक्ष्मतर और उदात्ततर होती है। इस प्रकार सौन्दर्य निरूपण में प्रामाण्य की खोज बनी रहती थी वह इन्द्रियप्रत्यक्ष अथवा तार्किक अनुमान से कृतार्थ नहीं होती है।
सौन्द्रर्यबुद्धि की स्वतंत्रता वस्तु जगत् से होते हुए भी भौतिक जगत् से नहीं होती। सौन्दर्य और श्रेयस को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। औचित्य के लिए जो कहा गया है कि 'रथस्योपनिषत्परा' वह निर्विवाद सत्य है। इसका कारण है कि जैसे जिस आत्मिक स्वभाव का साहित्य में निरूपण होता है वही आत्मभाव श्रेयस का भी निदर्शन करता है। 'श्रेयोदर्शिनी धी' काव्य-प्रतिभा से भिन्न होते हुए भी दोनों ही साक्षात्कारात्मक हैं एवं समान मानव स्वभाव के दो पक्षों कर्तृत्व और आस्वादन से जुड़ी हैं : बहुधा रसिकों को यह भ्रान्ति हो जाती है कि काव्यकला में अशीलता या अनौचित्य का स्थान नहीं होता किन्तु इस बहु विवादित प्रश्न पर कालिदास का ही निर्णय सही लगता है कि : यदुच्यते पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारी तद्वचः।
नैतिकमूल्य प्रेयो विरोधी नहीं हैं। किन्तु वे प्रेयोनुसन्धान को मर्यादित करते हुए उनका अतिक्रमण करते हैं। मर्यादित प्रेयस के रूप में नैतिकमूल्य कर्तव्यों को निर्धारित करता है और समाज-व्यवस्था का आधार बनता है। इस स्तर पर नैतिकता के विभिन्न आयामों में सन्तुलन रखने का प्रश्न 'दुस्समाधेय' रहता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका सामाजिक दायित्व, राज्यसत्ता और उसका नैतिक नियंत्रण, जीविकोपार्जन और भोगपरायणता, शान्ति की स्थापना और शक्ति-संग्रह इन सभी बन्धों में सन्तुलन का कोई नपा-तुला सूत्र नहीं है। इसीलिए नैतिक जीवन का आधार जागरूक विवेक ही बना रहता है न कि कोई रूढ़ या वैज्ञानिक नियमानियम। इस सामाजिक नैतिकता का आधार आत्मगुणों की अन्तरंग साधना है। इन गुणों में अहिंसा और सत्य ही सर्वोपरि है। इन दोनों का आधार आत्मानुकूलता और आत्मतुल्यता का ज्ञान ही समता का ज्ञान है और अहिंसा का आधार। जिस समाज और संस्कृति में अहंकार, राग-द्वेष आदि को मनुष्य के सहज और अनिवार्य धर्म मान लिए जाते हैं वहाँ अहिंसा, शान्ति और समता का आधार समझौता ही रह जाता है। समझौते और संघर्ष में उतना ही भेद है जितना अल्प बल और अधिक बल में। __ सौन्दर्य के समान ही श्रेयस् की अवधारणा भी वस्तुपरक तटस्थ ज्ञान पर निर्भर नहीं करती किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह ज्ञान निरपेक्ष नहीं है और मात्र सामाजिकता पर आधारित चारित्रिक विशेषता या रूदिमूलक नियम हैं। सुकरात का प्रसिद्ध कथन कि 'ज्ञान गुण है', शाश्वत सत्य है। किन्तु ज्ञान का अर्थ तार्किकज्ञान न होकर आध्यात्मिक विवेक है। सौन्दर्यबुद्धि और श्रेयोबुद्धि दोनों ही आत्मबुद्धि के ही रूप हैं। ___ ज्ञान और सत्य सपाट धरातल के धर्म नहीं है। ज्ञान अनेक भूमियों में विभक्त है और उन भेदों से सत्य का भी तारतम्य निर्धारित होता है। सप्तशती की यह उक्ति :
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचरे।
विषयास्तु महाभाग यान्ति चैवं पृथक्-पृथक्। एक गंभीर सत्य का प्रतिपादन करती है। सभी प्राणियों की समीहा से उनका ज्ञान जुड़ा रहता है। कायिक या इन्द्रियप्रत्यक्ष के द्वारा प्राणी अपना हित-अहित पहचानते हैं। मानवीय स्तर पर यह नियत व्यवस्था समाप्त हो जाती है। क्योंकि अनुमान के द्वारा ऐन्द्रिय प्रदत्तों का ज्ञान विस्तारित हो जाता है और भाषा से जुड़ता हुआ यह विकल्पात्मकज्ञान