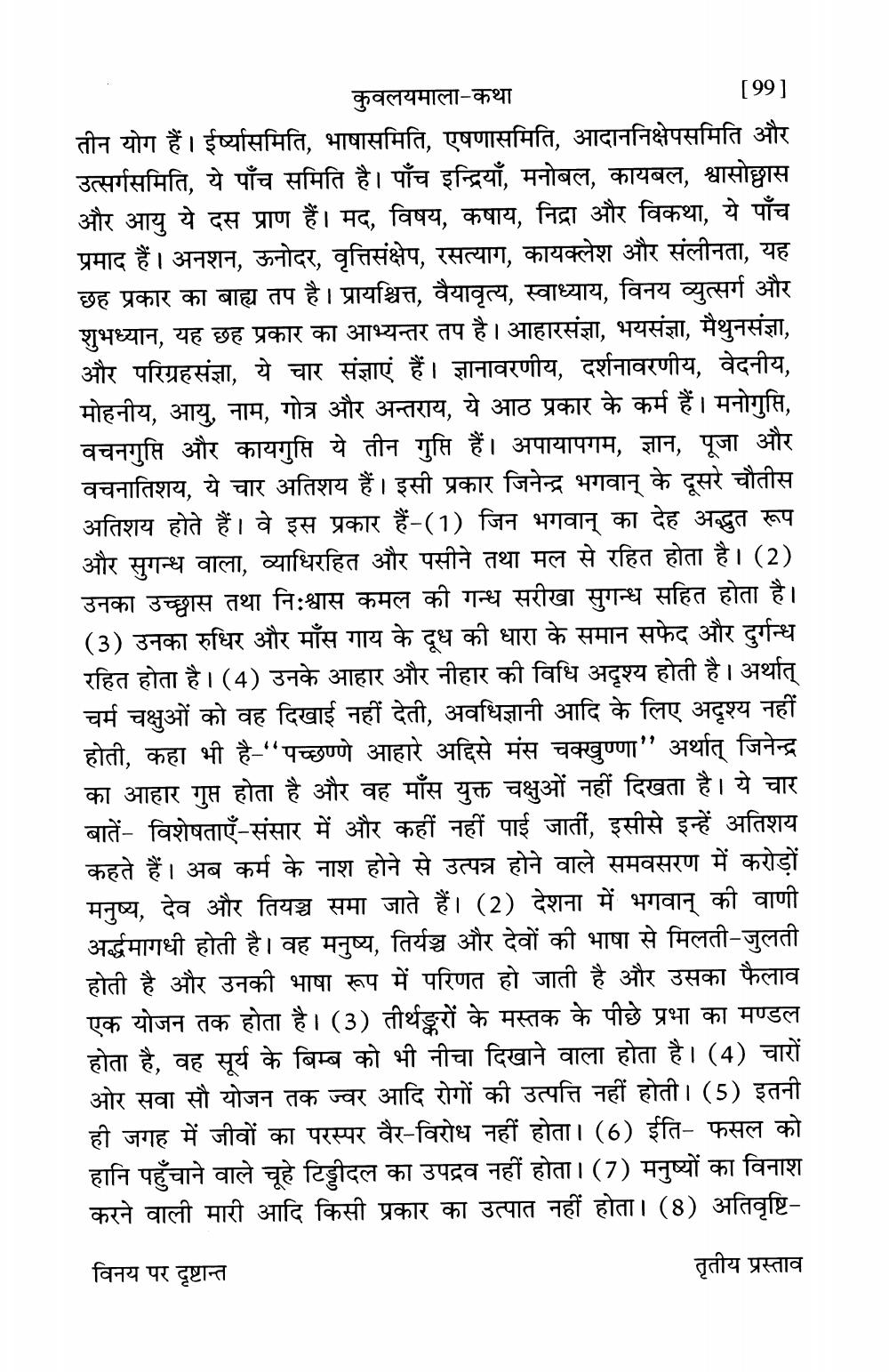________________
कुवलयमाला-कथा
[99] तीन योग हैं। ईर्ष्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति और उत्सर्गसमिति, ये पाँच समिति है। पाँच इन्द्रियाँ, मनोबल, कायबल, श्वासोवास
और आयु ये दस प्राण हैं। मद, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा, ये पाँच प्रमाद हैं। अनशन, ऊनोदर, वृत्तिसंक्षेप, रसत्याग, कायक्लेश और संलीनता, यह छह प्रकार का बाह्य तप है। प्रायश्चित्त, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विनय व्युत्सर्ग और शुभध्यान, यह छह प्रकार का आभ्यन्तर तप है। आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा,
और परिग्रहसंज्ञा, ये चार संज्ञाएं हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, ये आठ प्रकार के कर्म हैं। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्ति हैं। अपायापगम, ज्ञान, पूजा और वचनातिशय, ये चार अतिशय हैं। इसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान् के दूसरे चौतीस अतिशय होते हैं। वे इस प्रकार हैं-(1) जिन भगवान् का देह अद्भुत रूप और सुगन्ध वाला, व्याधिरहित और पसीने तथा मल से रहित होता है। (2) उनका उच्छ्वास तथा निःश्वास कमल की गन्ध सरीखा सुगन्ध सहित होता है। (3) उनका रुधिर और माँस गाय के दूध की धारा के समान सफेद और दुर्गन्ध रहित होता है। (4) उनके आहार और नीहार की विधि अदृश्य होती है। अर्थात् चर्म चक्षुओं को वह दिखाई नहीं देती, अवधिज्ञानी आदि के लिए अदृश्य नहीं होती, कहा भी है-"पच्छण्णे आहारे अद्दिसे मंस चक्खुण्णा" अर्थात् जिनेन्द्र का आहार गुप्त होता है और वह माँस युक्त चक्षुओं नहीं दिखता है। ये चार बातें- विशेषताएँ-संसार में और कहीं नहीं पाई जातीं, इसीसे इन्हें अतिशय कहते हैं। अब कर्म के नाश होने से उत्पन्न होने वाले समवसरण में करोड़ों मनुष्य, देव और तियञ्च समा जाते हैं। (2) देशना में भगवान् की वाणी अर्द्धमागधी होती है। वह मनुष्य, तिर्यञ्च और देवों की भाषा से मिलती-जुलती होती है और उनकी भाषा रूप में परिणत हो जाती है और उसका फैलाव एक योजन तक होता है। (3) तीर्थङ्करों के मस्तक के पीछे प्रभा का मण्डल होता है, वह सूर्य के बिम्ब को भी नीचा दिखाने वाला होता है। (4) चारों
ओर सवा सौ योजन तक ज्वर आदि रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। (5) इतनी ही जगह में जीवों का परस्पर वैर-विरोध नहीं होता। (6) ईति- फसल को हानि पहुँचाने वाले चूहे टिड्डीदल का उपद्रव नहीं होता। (7) मनुष्यों का विनाश करने वाली मारी आदि किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता। (8) अतिवृष्टि
विनय पर दृष्टान्त
तृतीय प्रस्ताव