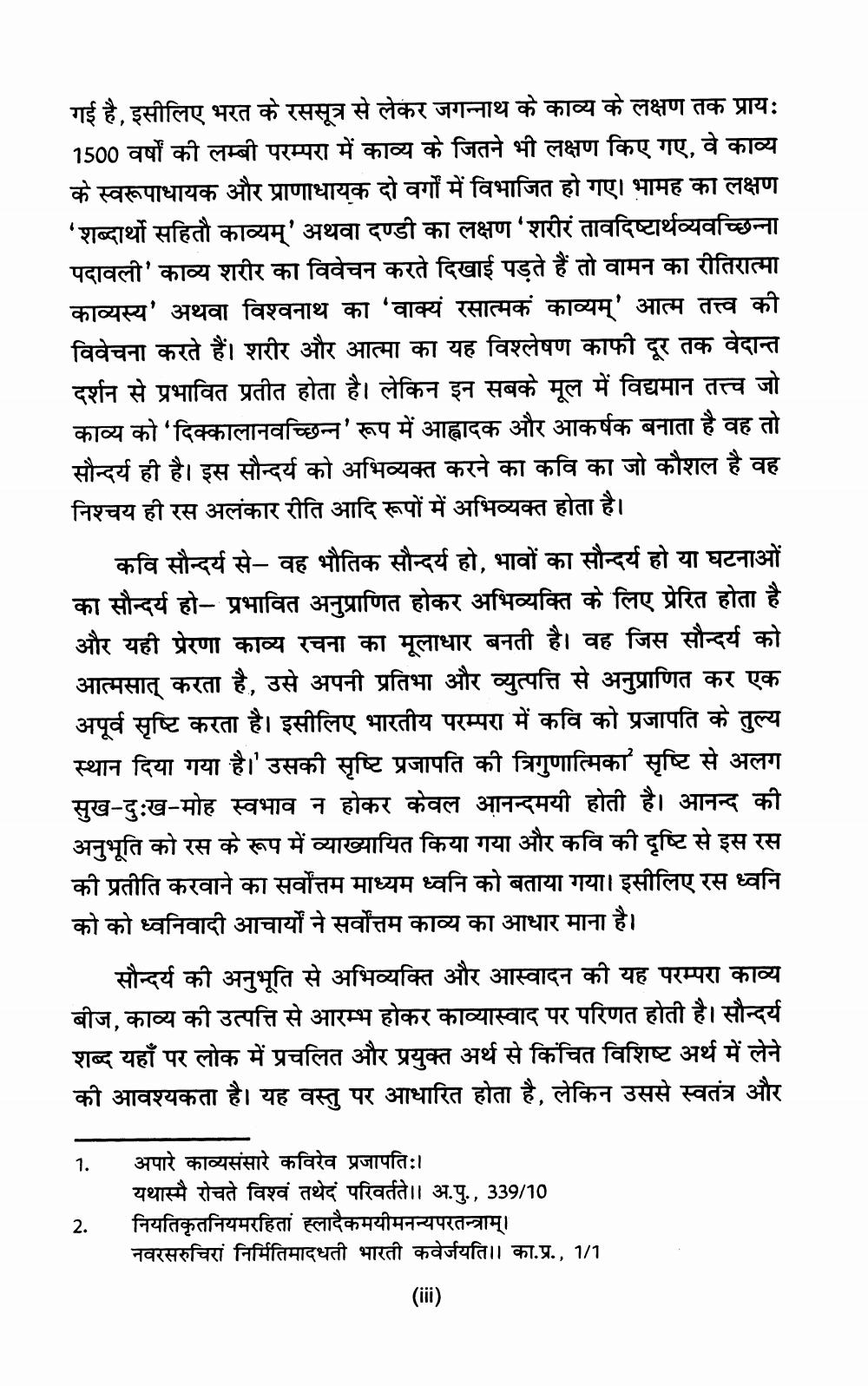________________
गई है, इसीलिए भरत के रससूत्र से लेकर जगन्नाथ के काव्य के लक्षण तक प्रायः 1500 वर्षों की लम्बी परम्परा में काव्य के जितने भी लक्षण किए गए, वे काव्य के स्वरूपाधायक और प्राणाधायक दो वर्गों में विभाजित हो गए। भामह का लक्षण ‘शब्दार्थो सहितौ काव्यम्' अथवा दण्डी का लक्षण 'शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली' काव्य शरीर का विवेचन करते दिखाई पड़ते हैं तो वामन का रीतिरात्मा काव्यस्य' अथवा विश्वनाथ का 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' आत्म तत्त्व की विवेचना करते हैं। शरीर और आत्मा का यह विश्लेषण काफी दूर तक वेदान्त दर्शन से प्रभावित प्रतीत होता है। लेकिन इन सबके मूल में विद्यमान तत्त्व जो काव्य को 'दिक्कालानवच्छिन्न' रूप में आह्वादक और आकर्षक बनाता है वह तो सौन्दर्य ही है। इस सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने का कवि का जो कौशल है वह निश्चय ही रस अलंकार रीति आदि रूपों में अभिव्यक्त होता है।
कवि सौन्दर्य से - वह भौतिक सौन्दर्य हो, भावों का सौन्दर्य हो या घटनाओं का सौन्दर्य हो - प्रभावित अनुप्राणित होकर अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित होता है और यही प्रेरणा काव्य रचना का मूलाधार बनती है। वह जिस सौन्दर्य को आत्मसात् करता है, उसे अपनी प्रतिभा और व्युत्पत्ति से अनुप्राणित कर एक अपूर्व सृष्टि करता है । इसीलिए भारतीय परम्परा में कवि को प्रजापति के तुल्य स्थान दिया गया है।' उसकी सृष्टि प्रजापति की त्रिगुणात्मिका सृष्टि से अलग सुख - दुःख - मोह स्वभाव न होकर केवल आनन्दमयी होती है। आनन्द की अनुभूतिको रस के रूप में व्याख्यायित किया गया और कवि की दृष्टि से इस रस की प्रतीति करवाने का सर्वोत्तम माध्यम ध्वनि को बताया गया । इसीलिए रस ध्वनि को को ध्वनिवादी आचार्यों ने सर्वोत्तम काव्य का आधार माना है।
सौन्दर्य की अनुभूति से अभिव्यक्ति और आस्वादन की यह परम्परा काव्य बीज, काव्य की उत्पत्ति से आरम्भ होकर काव्यास्वाद पर परिणत होती है। सौन्दर्य शब्द यहाँ पर लोक में प्रचलित और प्रयुक्त अर्थ से किंचित विशिष्ट अर्थ में लेने की आवश्यकता है। यह वस्तु पर आधारित होता है, लेकिन उससे स्वतंत्र और
1. अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः ।
2.
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ।। अ.पु., 339/10
नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्। नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति ।। का. प्र., 1/1
(iii)